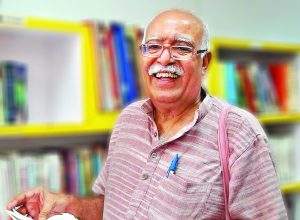मुझे याद है, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा, तभी से यह सवाल सुनता आया हूँ। दारा शिकोह के बसाए शहर शिकोहाबाद के मीराँ कटरा मुहल्ले में जहाँ हमारा घर था, वहाँ आसपास बहुत से विस्थापित परिवार थे। वे सभी हमारी ही तरह उजड़कर उस मुल्क से आए थे, जो रातोंरात पराया बन गया था। एकाएक हृदय को झिंझोड़ देने वाले विचित्र से भावावेदगी धक्के की तरह सबको पता चल गया था कि अब हमारी जन्मभूमि—हमारी मातृभूमि पराई हो चुकी है, और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, हमें निकल जाना चाहिए। वरना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी…! अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत, बहू-बेटियों की अस्मत और पीढ़ियों से कमाई घर-परिवार की साख सब एक क्षण में जा सकती है। सिर्फ एक क्षण में। हवा के बगूले की तरह!
कौन अपना है, कौन पराया? किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं, सारे फर्क और फासले गायब हो चुके थे। और दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। देखते ही देखते काँटेदार बाड़ की तरह कुछ नई और बेहद कठोर हदबंदियाँ बन गई थीं। भीतर भी, बाहर भी। और रह-रहकर हवा में गूँजते उन्मादी नारे दिलों में खौफ और दहशत पैदा करते थे। खूनी खंजर की तरह।
हवाओं में रक्त की बू आने लगी थी।
एक सूनापन। भीतर भी, बाहर भी।…तमाम शोर-शराबे, आवाजों और चीख-चिल्लाहट के वावजूद कुछ था जो एकदम सुन्न हो गया था। और हर जगह संदेह की नागफनियाँ उग आई थीं। हर शख्स उन्हीं में घिरा हुआ, लहूलुहान।
एक विश्वास जो लुट-पिट गया था। वह कैसे वापस आए, यह कोई नहीं जानता था। पता नहीं किसने अदृश्य हाथों से हजारों दिलों पर बरछी चलाई थी, जिसका घाव अब किसी भी तरह भर नहीं सकता था। जिंदगी भर उसकी पीड़ा और दंश के साथ जीना था और मरना था। मरना और जीना था।

इतिहास नटी ने देखते ही देखते कालपटल पर एक रक्तरंजित महा नाटक रच दिया था, जिसका सूत्रधार कौन है, यह कोई नहीं जानता था।
तब सरगोधा शहर बसाने वाले सर गोधाराम सरीखे बहुत सारे भले, उपकारी और प्रभावशाली लोगों ने जगह-जगह विशाल कैंप लगाकर, रातोंरात शरणार्थी बन गए हजारों लोगों के ठहरने, खाने-पीने और सुरक्षा का इंतजाम किया था। सब लोग अपने-अपने घरों, गलियों, मुहल्लों से निकलकर छिपते-छिपाते वहाँ आ रहे थे, आश्रय पाने के लिए। कल तक जिन गली-मुहल्लों में सिर उठाकर चलते थे, वहाँ से अब चोरों की तरह छिपकर डरते हुए निकलना पड़ रहा था। सिरों पर सामान की छोटी-बड़ी पोटलियाँ। गोदी में बच्चे, और हर पल आशंकित स्त्रियाँ, रातोंरात जिनके चेहरों की रंगत उड़ गई थी। दिलों में विचित्र कँपकँपी और थरथराहट सी। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा… !
ऐसे में कैंप में आकर लगता, जैसे भगवान के घर आ गए हों। जीते-जी। सही-सलामत। काँपते हाथ ऊपर आसमान की ओर उठ जाते—हे राम जी! और आँखों से गंगा-जमुना की धाराएँ बह उठतीं।
कैंप सचमुच ऐसे सारे बेसहारों के लिए भगवान का घर ही था। खाने-पीने को वहाँ मिल जाता। और भी छोटी-मोटी सुविधाएँ। फिर सबके साथ होने का अहसास। दूसरों के सुख-दुख की करुण गाथाएँ सुनते-सुनते अपने दुख हलके लगने लगते।
रात होने पर किसी तरह टाँगें सिकोड़कर लेट रहो। मगर मन तो उन्हीं घरों में मँडराता रहता, जो कल तक अपने थे। मगर अब पता नहीं, जिंदगी में कभी उसकी एक झलक भी देख पाएँगे या नहीं।
“हे राम जी! किसी तरह बलवाइयों से बचकर हम इस कैंप में आ गए, यही क्या कम है।”
किसी बूढ़ी स्त्री की कँपकँपाती आवाज देखते ही देखते दूर तक फैल जाती और सैकड़ों आँखें नम हो जातीं।
“तूने बहुत दिया मेरे राम जी! बहुत दिया।…आगे भी उम्मीद है, जरूर देगा। हमारे हाथ-पैर सलामत रहे तो कोई कमी नहीं। फिर सब कुछ हो जाएगा। वही इज्जत, वही रोटी। सब कुछ।…बस, किसी तरह बचकर अपने वतन पहुँच जाएँ।” कँपकँपाते होंठों पर एक उम्मीद।
रात भर वहाँ पहरा रहता। सतर्क वालंटियर। किसी फौजी छावनी की तरह। बीच-बीच में छोटे-बड़े नेताओं का आना-जाना। वादे और वादे। आश्वासन…और हवा में फड़फड़ाते अखबारी टुकड़ों की तरह आधे-अधूरे समाचार भी।
गाँधी…नेहरू…पटेल…!
नेहरू…पटेल…गाँधी…!!
यह रातोंरात पराए और हिंसक बन गए मुल्क की कहानी है। बेहद करुण और सच्ची, मगर अविश्वसनीय भी!…दादी-नानी की पुरानी कहानियों की तरह।
फिर रेलगाड़ियों में बैठाकर किसी विशाल टोली को अंबाला, किसी को अमृतसर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत या दिल्ली रवाना कर दिया जाता। और पूरे रास्ते में हवा में छन-छनकर कर आती यहाँ-वहाँ मारकाट और बलात्कार की खबरें…! उन सबके बीच ही रुक-रुककर, थम-थमकर, और बलवाइयों के आतंक से थर-थर काँपते हुए, भयभीय स्त्री और बच्चों के साथ सबको यह लंबी काल-यात्रा पूरी करनी होती, ताकि सुरक्षित अपने वतन पहुँच जाएँ।…
अलबत्ता, शिकोहाबाद में जब आसपास के घरों से कोई शख्स पिता जी से मिलने आता, तो पहला वाक्य जो आपसी परिचय में पूछा जाता था, वह यह कि “तुस्सी पिच्छों किथाँ दे हो?” यानी आप सरगोधे के हैं या लाहौर के? या कराची, बन्नू, मियाँवाली, लायलपुर, पेशावर या सरहद के? और इस सवाल का जवाब मिलते ही आपस में परिचय इतना गहरा हो जाता था और एक के बाद एक दास्तानें कुछ इस कदर चल पड़ती थीं कि न पिता जी को समय का कुछ होश रहता और न आगंतुक को। फिर चाय, लस्सी या खाने का इंतजाम होता और चलते-चलते वह शख्स हमारे लिए हमेशा-हमेशा के लिए चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी या ऐसा ही कुछ और हो चुका होता। एक ऐसा संबंध जो बरसोंबरस चलना था। जीवन और मौत के पार भी।…
और यह सारी की सारी महागाथा जिस छोटे से सवाल से पैदा हुई थी, उसे फिर से दोहरा देना होगा, “तुस्सीं पिच्छों किथाँ दे हो…?”
उन दिनों मैं छोटा था। बहुत छोटा सा। मुश्किल से तीन-चार बरस का। तब मुझे ठीक से न पंजाबी समझ में आती थी और न हिंदी। अभी मुझे ठीक से क, ख, ग की भी पहचान नहीं थी। पर इस सवाल को मैं अच्छे से पहचान गया था और इसकी जादुई शक्ति और प्रभाव को भी, कि तुसीं पिच्छों किथाँ दे हो?
मुझे लगता था, एक गूँगे के आगे भी यह सवाल रख दो, तो उसके भीतर से इस तरह वाग्धारा फूट पड़ेगी, जैसे सतलुज सरीखे बड़े विशाल दरिया बहते हैं। और आप एक पत्थर से यह सवाल पूछो, तो उसके भीतर से सुख-दुख और पीड़ा का एक महाकाव्य निकलकर सामने आ जाएगा। गंगा-जमुना की धाराओं की तरह, निर्मल और पावन।
तो फिर मैं अपनी आत्मकथा की शुरुआत यहीं से क्यों न करूँ कि तुसीं पिच्छों किथाँ दे हो?
*
तो अपनी कहानी शुरू करूँ, इससे पहले शायद थोड़ा परिवार का ब्योरा देना जरूरी है। मैं अपने पिता की आठवीं संतान हूँ। पिता दादा जी की अकेली संतान थे। लेकिन आगे पिता की नौ संतानें हुईं। हम नौ भाई-बहनों में कमलेश दीदी, मैं और मुझसे छोटा सत—हम तीनों भारत में जनमे हैं। बड़ी भैन जी और मुझसे बड़े पाँच भाई पाकिस्तान में जनमे। पाकिस्तान के कुरड़ गाँव में, जो खुशाब तहसील, जिला सरगोधा में है। कुरड़ और कट्ठा गाँव साथ-साथ थे, सहोदर भाइयों की तरह, जिनका नाम भी साथ-साथ लिया जाता था। यानी कौन सा कुरड़ गाँव? पूछने पर कहा जाएगा, कुरड़-कट्ठे वाला कुरड़ गाँव।
गाँव के पास ही मीठे पानी का एक सोता था, जो आगे जाकर नदी में बदल गया था। पंजाबी में मीठे पानी के सोते को कट्ठा कहते हैं, और जहाँ वह सोता हो, उस स्थान का नाम भी कट्ठा पड़ जाता है। संभव है, इसीलिए साथ के गाँव का नाम कट्ठा पड़ गया हो।
हमारा परिवार जब भारत आया तो श्याम भैया छोटे से थे, माँ की गोद में। जगन भाईसाहब पहली-दूसरी में और मैं अभी प्रतीक्षा में था। मुझे अभी तीन बरस बाद पैदा होना था! तीन बरस बाद, ताकि ‘आजादी’ अपनी फौरी चमक-दमक से निजात पाकर एक तरह की आत्मालोचना की राह पर बढ़ आए! और मैं सच में आजादी के बाद की पीढ़ी का खरा प्रतिनिधित्व कर पाऊँ।
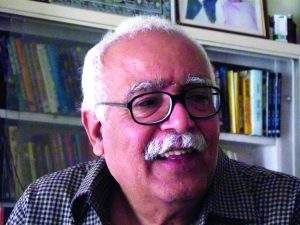
उस समय परिवार को किन कठिनाइयों और करुण हालात से होकर गुजरना पड़ा, कैसे कठोर संघर्ष भरे वे दिन थे, इसके बारे में माँ, बड़ी भैन जी और कश्मीरी भाईसाहब से काफी कुछ सुना है। मैंने वह सब देखा तो नहीं, पर अपनी सहज संवेदना से महसूस तो किया ही है। जब मैं उन अभागे दिनों और मुश्किल हालात के बारे में सोचता हूँ तो अकसर मुझे विस्थापन की असह्य तकलीफों के बीच कंधे पर कपड़ों की भारी सी गठरी टाँगे गाँव-गाँव घूमते पिता दिखाई देते हैं। यहाँ आने के बाद जब सारे सहारे छिन गए तो उन्हें फेरीवाला बनकर अपना और परिवार का गुजर-बसर करना पड़ा।
पिता जी अमृतसर से पगड़ियाँ खरीदकर लाते थे और अंबाला में गाँव-गाँव जाकर बेचते थे। और यह काम अकेले पिता को ही नहीं, मेरे दादा देशराज जी और दोनों बड़े भाइयों बलराज जी और कश्मीरी भाईसाहब को भी करना पड़ता था। एक दिशा में पिता पगड़ियाँ बेचने निकलते, तो दूसरी दिशा में दादा जी और तीसरी दिशा में मेरे दोनों बड़े भाई बलराज जी और कश्मीरीलाल। तब कहीं घर का गुजारा चल पाता था। खुशाब तहसील के जिस कुरड़ गाँव से पिता विस्थापित होकर आए थे, वहाँ एक संपन्न और सम्मानित व्यापारी के रूप में उनकी साख थी और दूर-दूर तक उनका नाम था। पर वह देखते ही देखते पराया देश बन गया—पाकिस्तान। और फिर रातोंरात वहाँ से पलायन की तैयारियाँ हो गईं।
शुरू में लग ही नहीं रहा था, कि अपनी जमीन और घरबार सब कुछ छोड़कर कभी विस्थापित होना पड़ेगा और दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। आर्थिक विषमताओं के थपेड़ों के बीच जिंदगी की एक बिल्कुल नई शुरुआत करनी होगी। एकदम ककहरा से, और एकाएक सम्मानित व्यक्ति से शरणार्थी बन जाना होगा। पर इतिहास के जिस क्रूर पहिए ने हजारों लोगों को बेघरबार किया और खून की नदियाँ बहा दीं, उससे किसी का भी बच पाना मुश्किल था। जाहिर है, हमारा परिवार भी उसकी लपेट में आया और पिता को रातोंरात अपना सब कुछ समेटकर चल देना पड़ा।
वे सोच रहे थे, कुछ समय बाद जब यह हिंसा और उपद्रव शांत हो जाएँगे, तो फिर यहाँ लौट आएँगे, और जीवन फिर अपनी पुरानी गति पकड़ लेगा। इसलिए बहुत कुछ उन्होंने वहीं छोड़ देना ठीक समझा। पर उनकी आशा बस दुराशा ही साबित हुई, और फिर जो कुछ छूटा, वह हमेशा-हमेशा के लिए ही छूट गया। भारत आने के बाद पिछला सब कुछ भूलकर, उन्हें जीवन की फिर एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी।
कुछ समय वे परिवार के साथ अंबाला छावनी रहे, पर अंततः उन्हें आगरा-कानपुर के मुख्य राजमार्ग पर स्थित उस शिकोहाबाद शहर में आकर टिकना था, जिसकी नींव शाहजहाँ के उदारहृदय बेटे दारा शिकोह ने रखी थी। दारा शिकोह तो जुल्मी औरंगजेब की क्रूरता की बलि चढ़ गया, जिसने हाथी के पैरों के नीचे उसे कुचलवा दिया, पर उस नरमदिल दारा ने आगरा से कोई चालीस मील दूर जिस शिकोहाबाद शहर की नींव रखी थी, वह बहुत कुछ उसके आदर्शों का शहर था, जिसमें हिंदू-मुसलिम दोनों समुदाय आपस में प्रेम से रहते थे। फिर आगरा-कानपुर के मुख्य राजमार्ग पर स्थित होने के बावजूद शिकोहाबाद ऐसा शहर था, जिसमें शहरातीपन कम, कसबाईपन ज्यादा था, जिसमें लोग जल्दी ही एक-दूसरे से परच जाते हैं और और फिर बहुत समय तक उस प्रेम और आत्मीयता के संबंध को निभाते हैं।
शिकोहाबाद तब मैनपुरी जिले में आता था, पर वह तब भी मैनपुरी से कहीं ज्यादा विकसित था। बाद में तो उसने और भी तेजी से तरक्की की और फिरोजाबाद जिले का हिस्सा बन गया। वही फिरोजाबाद जिसमें घर-घर चूड़ियाँ और दूसरा काँच का सामान बनता है, और जिसे ‘सुहागनगरी’ के नाम से भी जाना जाता है।
अलबत्ता पिता ने शिकोहाबाद को अपनी शेष जीवन-यात्रा के लिए चुना और कुरड़ की तरह ही स्थायी ठिकाना बनाया, तो शिकोहाबाद ने भी कोई कोर-कसर नहीं रखी। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर बड़े प्यार से उन्हें अपना लिया। फिर तो हमारा परिवार हमेशा के लिए शिकोहाबाद का होकर ही रह गया। पिता के लिए बहुत कड़े संघर्ष के दिन थे ये। ताप से ताए हुए। पर पिता बड़े दिलेर, बड़े हिम्मती थे। वे थके नहीं। बड़े बेटों ने आगे बढ़कर उन्हें पूरा साथ दिया। घर में माँ, पिता, भाई-बहन सब इस दुख की भट्ठी से निकले, पर किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं। कोई मलिनता नहीं। सब एक मुट्ठी की तरह एक। बस, एक ही धुन कि इस दुख की घड़ी में हारना नहीं है और एक-दूसरे को सहारा देना है।
फिर धीरे-धीरे दिन बहुरे। पिता ने थोड़े ही समय में अपने इस नए काम में साख हासिल कर ली, और फिर कपड़ों की एक दुकान खोल ली, जो खासी चल निकली। क्लेम के कागजों के आधार पर अपना घर भी हो गया। फिर पिता ने आटा चक्की और तेल का एक्सपेलर सँभाला और दोनों बड़े भाइयों बलराज जी और कश्मीरी भाईसाहब के पास अपनी-अपनी कपड़े की दुकानें हो गईं। कृष्ण भाईसाहब ने पिता का साथ देने के लिए पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया, और हम छोटे भाई-बहन निश्चिंत होकर पढ़ने-लिखने में लग गए। कुछ ही वर्षों में जिंदगी फिर से अपनी सम लय-गति में चलने लगी। जीवन के कठोर संघर्ष ने पिता, माँ और भाई-बहनों को हराया नहीं, बल्कि तपाकर और उजला कर दिया। जब भी पारिवारिक इतिहास के ये पन्ने फड़फड़ाते हुए मेरी आँखों के आगे आते हैं, तो मन में सचमुच एक गर्व का अहसास होता है।
*
हमारा परिवार एक पारंपरिक व्यवसायी परिवार था, और किसी व्यवसायी परिवार का एक अलग तरह का चरित्र होता है। नए विचारों की रोशनी वहाँ कुछ देर से आती है। पर फिर जल्दी ही इसमें नई-नई धाराएँ फूट पड़ीं और इससे परिवार का रहन-सहन, सोच और पारिवारिक संस्कृति भी बदली। एक नई कर्म संस्कृति और विचार संस्कृति आई। जगन भाईसाहब ने इंजीनियरिंग की लाइन चुनी तो वे जाने-अनजाने अपने ढंग से घर के माहौल और पारिवारिक वातावरण को कुछ बदल भी रहे थे।
कृष्ण भाईसाहब रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर हो गए तो उनका ही नहीं, घर में औरों का भी रंग-ढंग बदला। फिर मैं साहित्य की धारा में बह निकला और अंततः पत्रकारिता में आया, तो यह एक नई ही राह थी। छोटे भाई सत ने पारंपरिक व्यवसाय को अलविदा करके बड़ी कंपनियों की खाद एजेंसी ली, तो एक नई ही राह निकल आई। परिवार का मूल ढाँचा वही रहा, पर हर बार वह कुछ बदलता भी गया। शायद हर विकास की यति-गति ऐसी ही होती है।…
पर इस बीच जिंदगी के थपेड़े भी कम नहीं रहे। हम भाई-बहनों में बलराज भाईसाहब जो हमारे सबसे बड़े भाई थे, कोई बत्तीस वर्ष की अवस्था में ही चले गए। वे आकस्मिक हृदयाघात से गए। अभी कुछ अरसा पहले ही हम भाइयों में जो सबसे सरल, शांत और बुद्धिमान थे, और जिन्हें हमेशा मुसकराते हुए ही देखा, वे कृष्ण भाईसाहब भी नहीं रहे। मुझसे कोई तीन बरस बड़े श्याम भाईसाहब तो बरसों पहले ही चले गए। वे असमय ही गए। श्याम भैया की मृत्यु का घाव मन में अब भी इतना ताजा है कि उनकी मृत्यु कल की बात लगती है। लेकिन अभी-अभी हिसाब लगाने बैठा तो मैं चौंका। श्याम भैया को गुजरे कोई इकतीस साल बीत चुके हैं।
सन् 1990 के सितंबर महीने में श्याम भैया गुजरे और बड़े भाईसाहब तो तब गुजरे, जब मैं सातवीं या शायद आठवीं कक्षा में पढ़ता था। सन् 63 की यह बात होनी चाहिए। सर्दियों की। आगे कुछ अरसे बाद 27 मई,1964 को नेहरू जी नहीं रहे। उस दिन की अच्छी तरह याद है कि खबर सुनते ही हर चेहरे पर दुख के बादल उमड़ पड़े। कुछ तो बिलख-बिलखकर रो भी रहे थे। भाईसाहब का निधन उनसे कुछ महीने पहले ही हुआ था। और हमारे लिए यह एक पारिवारिक शोक के बाद आया दूसरा बड़ा शोक था। एक राष्ट्रीय शोक…!
मुझे अच्छी तरह याद है कि सन् 62 में चीनी हमले के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए हमारे मोहल्ले में एक बड़ी सभा हुई थी। उसमें सभी ने अपनी सेना और सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ अंशदान देने का फैसला किया था। जितने भी लोग उस सभा में मौजूद थे, उन सभी के चेहरे पर एक गुस्से से भरी तमतमाहट मुझे नजर आई थी, और कुछ करने का निश्चय भी। उस सभा के बारे में सोचता हूँ, तो बहुत कुछ यादों की खिड़की से झरता नजर आता है।
मुझे याद है कि मैं अभी छोटा ही था, मगर मेरे भीतर जोश का सैलाब सा उमड़ आया था। चीन के आक्रमण के साथ ही अचानक मुझे अपने भीतर बहुत कुछ जागता और अँगड़ाई लेता महसूस हुआ था। उस सभा में बड़े भाईसाहब बलराज जी मौजूद थे या नहीं, यह अब याद नहीं आ रहा। उस समय वे एटा रोड पर बने क्वार्टर में आ गए थे। हमारे घर से वह कुछ दूर था, इसलिए संभव है कि उस सभा में आ न सके हों। या उन्हें सूचना ही न गई हो।
उस सभा में पिता जी और जगन भाई साहब की उपस्थिति की बड़ी अच्छी तरह याद है। साथ ही बिरादरी के लोग भी काफी संख्या में आए थे। किशोर, नौजवान और बूढ़े भी। जहाँ तक मुझे याद है, जगन भाई साहब और बतरा जी उस सभा के कर्ता-धर्ता थे। उन्होंने उस समय सामाजिक जागृति लाने के लिए एक संस्था भी बनाई थी, पंजाब और सिंध सेवा दल। साथ ही एक पुस्तकालय भी शुरू करने का फैसला हुआ, जो हमारे घर की बाहर वाली बैठक में खुला था।
बड़े भाईसाहब बलराज जी की मृत्यु बहुत कम अवस्था में हुई थी। शायद तब वे कुल बत्तीस बरस के रहे होंगे। हमारे घर में यह हरहराती आँधी का पहला धक्का था जिससे पूरा घर तितर-बितर हो गया। जैसे किसी चिड़िया का सुंदर घोंसला तिनका-तिनका होकर बिखर जाए। पंजाब से उजड़कर आने के बाद, जैसे जल्दी ही फिर उजड़ना लिखा हो भाग्य में। बलराज भाई साहब ऐसे ही श्रवणकुमार पुत्तर थे, जिनमें माँ और पिता जी दोनों के प्राण बसते थे। ऐसे में उनका जाना, और इस तरह जवानी में ही चले जाना…! यह किसी हरे-भरे पेड़ पर बिजली गिरने सरीखा था।
याद पड़ता है, हमारे पड़ोसी और ठेठ देसी अंदाज के कवि, हकीम चंद्रभान फंडा का वह दर्दभरा गीत जिसे सुनकर माँ और पिता ही नहीं, पूरी खलकत आँसुओं में डूब गई थी। उस दर्दभरे शोकगीत की शुरुआती पंक्तियाँ अब भी कानों में गूँज रही हैं—
दस्साँ की हाल मैं त्वानूँ बलराज जी दा,
उसनूँ जाणदा सी सकल जहान यारो!…
आँधी का दूसरा धक्का था रामकली भाभी की मृत्यु और आँधी का तीसरा धक्का था श्याम भाईसाहब की मृत्यु। श्याम भाईसाहब गुजरे तो चवालीस-पैंतालीस से अधिक के न थे। एक हरे पेड़ के कटने का-सा चीत्कार उस समय आप पूरे घर की दीवारों से सुन सकते थे।
*
तो यह थी उस घर की दास्तान, जिसमें कुक्कू का जन्म हुआ। वह पला और बड़ा हुआ।
वह बेशक सबसे अलग था, पर कहीं न कहीं सबसे जुड़ा हुआ भी। किसी का छोटे से छोटा दुख भी उसे उदास कर देता और वह घंटों उसके बारे में सोचता रहता था। और इसी तरह, किसी के मुख से कोई खुशी की, या अचरज भरी बात सुनता तो एकदम उल्लसित हो उठता और ‘ओल्लै’ कहकर तालियाँ बजाता हुआ नाच उठता। जल्दी ही वह खुश हो जाता और जल्दी ही आँखों से आँसुओं की बरसात। छल-छल, छल-छल…!
कुक्कू को कहानियाँ पसंद थीं। उसे लगता, कोई उसे दिन-रात कहानियाँ सुनाता रहे और वह सुनता रहे। कहानियाँ सुनते हुए वह जरा भी थकता न था। कुक्कू को कविताएँ पसंद थीं। जब भी वह कोई कविता सुनता, तो उसकी बढ़िया और मर्मस्पर्शी पंक्तियाँ उसके भीतर उतर जातीं। फिर न जाने कितनी बार वह अंदर ही अंदर उन्हें दोहराता और उनका आनंद लेता। कुक्कू को कल्पना की दुनिया पसंद थी। कल्पना की दुनिया में पंख पसारकर वह एक बार उड़ना शुरू करता, तो उसे बिल्कुल याद न रहता कि वह कहाँ बैठा है और उसके आसपास क्या है। वह असलियत से ज्यादा कल्पना की दुनिया में ही रहता था। बल्कि असलियत की दुनिया में उसे कभी ठेस लगती या कोई चीज बुरी लगती, तो वह उसी समय कल्पना की दुनिया में जाकर उसे दुरुस्त कर लेता और अपनी चोट भूल जाता। तब उसे लगता कि उसने दुनिया को कुछ सुधार दिया है, उसे पहले से कहीं अधिक अच्छा और सुंदर बना दिया है। और वह इसी बात से मगन और आनंदित हो जाता।…
तो चलिए, अब कुक्कू की कथा शुरू की जाए। इसी परिवेश में धीरे-धीरे बड़ा हो रहा और घर और आसपास की संवेदना से कुछ-कुछ सीझा-सा कुक्कू, जो असल में थोड़ा बुद्धू ही था। चलो, बुद्धू न सही, पर ज्यादा चतुर और होशियार तो वह कभी न था। हाँ, सोचता बहुत था, हर वक्त चुपचाप कुछ न कुछ सोचता ही रहता था।
पर यह भी मैं क्यों कहूँ? चलिए, आप कुक्कू से ही मिल लीजिए। शायद वह कुछ कहने और आपसे बात करने के लिए खुद ही बेताब है।
*
हाँ, तो शुरू करता हूँ।…मेरा बचपन का घर पर पुकारने का नाम था, ‘कुक्कू’। यह कुछ बुरा तो नहीं है। और जब से मुझे पता चला है कि कुक्कू माने कोयल भी होता है, तब से तो कुक्कू खासा अच्छा लगने लगा है। पर बचपन में जाने क्यों कुक्कू मुझे कुछ खास पसंद न था। अगर कोई बिगाड़कर कहता कि, “अरे ओए कुकड़ू!” तो मेरी जान सूखती थी ओर बड़ा गुस्सा आता था। याद पड़ता है कि कृष्ण भाईसाहब भी ‘कुकड़ू कूँ’ कहते थे, पर वह इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वे किसी अत्यंत लोकप्रिय लोककथा का स्मरण कराते हुए एक गीत की दो पंक्तियाँ सुनाते थे। यह गीत उस लोककथा में ही पिरोया हुआ था—
कुकडूँ-कूँ,
राजे दी धी परना दे तूँ!
(यानी, ओ रे कुकड़ूँ-कूँ बोलने वाले मुरगे, तू राजा की बेटी से मेरा विवाह करवा दे।)
आज इस कहानी के बारे में सोचता हूँ तो लगता है, जरूर यह कहानी किसी ऐसे नवयुवक हरखू की है, जिसका दोस्त एक मुरगा है। वह मुरगा ऐसा सच्चा और प्यारा दोस्त है जो हर कदम पर हरखू की मदद करता है।
और फिर अचानक कभी हरखू को पता चला होगा किसी राजा की बेटी के बारे में, जो बहुत सुंदर है। तब हरखू ने अपने उस दोस्त मुरगे से बड़े प्यार से गुजारिश की होगी कि—
कुकुड़ूँ कूँ,
राजे दी धी परना दे तूँ।
उसके बाद हो सकता है कि मुरगा राजा के पास पहुँचा हो और पंख फड़फड़ाते हुए उछल-उछलकर उसे युद्ध के लिए ललकारा हो। अकेले दम पर उसकी सारी सेनाओं का मुकाबला किया हो। फिर आखिर में उसने कैसे अपनी चतुराई से राजा को इस बात के लिए तैयार किया होगा कि वह अपनी बेटी का विवाह हरखू से ही करे, यह तो कहानी पढ़ने या सुनने से ही पता चल सकता था। पर गीत की इन दो सुंदर पंक्तियों से उसका अनुमान जरूर लग जाता है।
काश, मैंने कृष्ण भाईसाहब से कुकड़ूँ कूँ कहने वाले मुरगे की कहानी भी सुन ली होती। पर वे इतने बड़े थे और मैं उनके आगे इतना छोटा और दबा हुआ कि यह आग्रह कर ही न सका।
यों श्याम भैया को छोड़ दें तो मुझसे बड़े भाई तो सब बहुत बड़े थे और उनका मन पर कुछ-कुछ आतंक सा था, इसलिए ज्यादातर तो मैं छोटे भाई सत के साथ ही खेलता था। घर में एक बस वही मुझसे छोटा था, बाकी तो सब इतने बड़े थे कि उनसे दूर-दूर रहना ही भला लगता था। उस दौर का यह बड़ा स्वाभाविक अनुशासन था, जो आज उतना स्वाभाविक नहीं लगता। आज लगता है, बड़े अपना बड़प्पन कुछ देर भूलकर छोटों के साथ हँसें-खेलें तो भला क्या बिगड़ जाएगा? आज कुछ-कुछ यही अनौपचारिकता घरों में आ भी रही है।
तो खैर, खूब बड़े से आँगन वाला बड़ा सा घर था हमारा। उसमें बड़े मजे से लंबी कूद, ऊँची कूद और गेंदटप्पा खेला जा सकता था। छुपमछुपाई भी। फिर लूडो और साँप-सीढ़ी में तो मुश्किल ही क्या थी? और भी तमाम खेल थे। इन्हीं में कोड़ा बदामशाही वाला खेल भी था, जिसके साथ गीत की ये पंक्तियाँ भी गाई जाती थीं—
कोड़ा बदामशाही,
पीछे देखो, मार खाई।
इस खेल में एक बच्चे के हाथ में कपड़े का बना कोड़ा होता था, जिसे वह लगातार हवा में फटकारता रहता था। कभी-कभी वह किसी बच्चे की पीठ पर भी जड़ देता था। पर खेल-खेल में उससे कोड़े खाने के भी मजे थे।
कमलेश दीदी मुझसे कोई दो-ढाई साल बड़ी थीं, पर वे भी खुशी-खुशी अपने खेलों में मुझे शामिल कर लेती थीं। कमलेश दीदी और बड़ी भैन जी की बेटी राज लगभग समवयस्का थीं। उनकी प्रायः खेल में अच्छी जोड़ी बन जाती। यों सत के अलावा मैं कमलेश दीदी, राज और उनकी सहेलियों के साथ भी खेला करता था और ये खेल या तो गुड्डे-गुड़ियों के खेल होते थे या फिर गुट्टे। दोनों ही खेल जिनमें मैं दोयम या तीयम दरजे का खिलाड़ी ही साबित होता था और आँखें फाड़े भौचक्का-सा उनका कमाल, उनकी कला और उनका नाट्य देखा करता था और सोचता था—मैं तो जनम-जिंदगी तक ऐसे कमाल नहीं कर सकता!
राज, कमलेश दोनों और उनकी सहेलियाँ भी अपनी हथेलियों में पहले से ही छह-छह, आठ-आठ गुट्टे भरे होने के बावजूद नीचे पड़ा गुट्टा बड़े ही कलात्मक लाघव के साथ फिर से उठा सकती थीं, इस सावधानी के साथ कि पहले से मुट्ठी में सहेजे गए गुट्टे कतई न गिरें, वरना तो आप हारे। ओह, क्या गजब का संतुलन था, क्या गजब की कला! और मैं सोचा करता था, “हे भगवान, ऐसी दिव्य कलाएँ, तूने बस लड़कियों को ही क्यों दीं?”
इसी तरह गुड्डे-गुड़िया के ब्याह में जमाने भर की बातें जो वे कर लेती थीं और उनमें सारी सृष्टि का जो ज्ञान उँड़ेला जाता था, मेरे पास तो उसका एक कण, एक तिनका तक न था। तो फिर मैं बुद्धू इस दुनिया में कर क्या रहा था और था क्यों? “राम जी, यह तो अजब-सी बात है!” मैं अकेले में चुपचाप अपनी शिकायत दर्ज कर देता।
रस्सीकूद और लँगड़ी कबड्डी में भी उनका यही कमाल। लगता, जैसे रस्सी कूदती हुई वे हवा हो जाती हों और लँगड़ी कबड्डी की कूद ऐसी कि अगर वे चाहें तो एक पैर से ही दुनिया फतह कर लें। मैं बुद्धू तो बस आँखें फाड़े, मुँह बाए, उनकी कला, लाघव और फुर्ती देखता था और सोचता था, मैं तो भाई, जनम जिंदगी में ऐसे रस्सी टप नहीं सकता और लँगड़ी कबड्डी में एक पैर से उछलने और होशियारी से एक-एक खाने में कूदने का यह कमाल तो बिल्कुल ही नहीं दिखा सकता। रस्सीकूद में मैं बार-बार रस्सी में उलझकर गिरता और घुटने तुड़ा लेता। यों एकदम फिसड्डी साबित होता। इसलिए अक्सर मेरी बारी बड़ी देर से आती थी। रस्सी का एक छोर पकड़े, औरों के लिए रस्सी घुमाते रहो और उनके खेल का आऩंद लो, बस यही मेरे बस में था। और इसमें मैं कोई कंजूसी नहीं करता था।
इसके अलावा मेरा एक और बड़ा महत्त्वपूर्ण काम था कि जब कमलेश दीदी और उनकी सहेलियों का गुड्डे-गुड़िया के ब्याह का आयोजन हो तो दौड़कर बाजार जाऊँ। दो आने में मुन्ने खाँ बिसाती से गुड़िया के छोटे-छोटे दूधिया चमकीले रोल्डगोल्ड के गहनों का पत्ता ले लाऊँ। या फिर चवन्नी में गुड्डे-गुड़िया की शादी की दावत के लिए एल्यूमिनियम के छोटे-छोटे चमकीले बरतन ले आऊँ, जिनमें नन्हे-मुन्ने से गिलास, कटोरियाँ, थाली, भगौना सब कुछ होता था। इस कदर नया, जादुई और चमचमाता हुआ सामान कि क्या कहने! देखकर सचमुच आँखों में ठंडक पड़ती थी।
इतना ही नहीं, रस्सीकूद वाली सुंदर सी हैंडिलदार रस्सी या गेंदटप्पा के लिए बड़ी वाली लाल गेंद लाने की जिम्मेदारी भी मेरी। मगर लाने के बाद खेल शुरू होता तो मैं पीछे-पीछे, और पीछे खिसकता जाता। वहाँ तो ऐसी-ऐसी चतुराई की बातें और दाँव-पेंच थे कि मैं भला कहाँ टिकता? मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चे ऐसी चतुराई कहाँ से सीख लेते हैं! मुझे तो चतुराई सिखाने वाले ऐसे किसी स्कूल का पता तक मालूम नहीं था।
मुझे लगता, मैं तो बस बुद्धू हूँ, और जिंदगी भर बुद्धू बसंत ही रहूँगा। कभी-कभी भगवान जी से प्रार्थना भी करता कि “हे भगवान जी, मेरे पास जो कुछ भी है, सब ले लो। बस, मुझे भी ऐसी ही कला, ऐसी ही चुस्ती-फुर्ती दे दो, जैसी आपने मेरी कमलेश दीदी और उनकी सहेलियों को दी है!”
पर ना जी ना…! मेरे पास ऐसा था ही क्या कि भगवान जी इस फालतू विनिमय पर ध्यान देते? सो मेरी प्रार्थना अस्वीकार हो गई और मैं खेलों में रह गया एकदम कोरा, बुद्धू का बुद्धू!…
इस बात से मुझे बड़ी झेंप आती, जैसे मुझमें कोई बड़ी भारी कमी है। पर शायद कुछ अलग चीज भी थी मुझमें जो मेरे साथ के और बच्चों में नहीं थी। छुटपन से ही मुझे एकांत अच्छा लगने लगा था। मैं एक ही जगह बैठा देर-देर तक जाने क्या सोचता रहता। बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया खींचती थी मुझे। जो कुछ बाहर देखता, उसकी एक प्रतिछवि मन में बना लेता और उसके बारे में भीतर घंटों सोचता रहता। इसमें मुझे आनंद आता था। और खेल-कूद में कच्चड़ था तो उसकी कुछ थोड़ी सी भरपाई हुई पढ़ने-लिखने में। पढ़ने-लिखने में मुझे वाकई मजा आता था।
*
मैं छोटा, बहुत छोटा था, तभी से अक्षर मुझे खींचते थे। शब्द खींचते थे, छपे हुए पृष्ठ खींचते थे। जब क, ल और म को जोड़कर कलम पढ़ना शुरू किया, तभी से दुनिया-जहान में जहाँ भी कहीं अक्षर मिलते, चाहे दुकान पर लगे बोर्ड पर या दीवार पर लिखे विज्ञापनों में, मैं रास्ता चलते उन्हें जोड़-जोड़कर पढ़ता। अभी ठीक से पढ़ना—लिखना नहीं आता था, पर जब भी मौका मिलता, मैं मेज पर पड़ा अखबार आँखों के आगे रखकर अक्षर से अक्षर जोड़ना शुरू कर देता। एक अंतहीन खेल। मुझे इसमें बड़ा रस आता, आनंद आता। अक्षर से अक्षर मिलाने का यह खेल अकेले भी खेला जा सकता था और घंटों खेला जा सकता था। मेरा मन इससे कभी ऊबता नहीं था।
बाजार से उन दिनों चीजें अखबारी लिफाफों में आती थीं और उन पर भी तो अक्षर होते थे। मैं उन दिनों घर में चीनी, चावल-दाल वगैरह-वगैरह का कोई खाली लिफाफा देखता तो उसे खोलकर और एकदम सीधा करके पढ़ना शुरू कर देता। कभी-कभी उसमें कोई अधूरी सी कहानी छपी होती। या तो उसका आगे का हिस्सा गायब होता या पीछे का। मैं कल्पना के सहारे उसे पूरा करने की कोशिश करता। यानी अगर कहानी के शुरू का हिस्सा पता है तो बाद का खुद बनाओ, और अगर बाद का पता है तो शुरू के हिस्से की खुद कल्पना करो। और अगर बीच का हिस्सा पता है तो पहले और बाद के हिस्से जोड़कर मन ही मन कहानी पूरी करो। मेरे लिए यह निराले आनंद की बात थी। एक बिल्कुल अलग सा खेल था, जिसमें कल्पना और कौतुक का विचित्र मेल था।
तो यानी कि छुटपन से ही गाड़ी दौड़ पड़ी।…
एकाध घंटा खेल का छोड़ दो तो सुबह से शाम तक पढ़ना, पढ़ना और बस पढ़ना। कमलेश दीदी मुझसे दो दरजे ऊँची क्लास में पढ़ती थीं, पर एकाध बार वे भी मेरी मदद ले लेतीं। खासकर हिंदी की किताब ‘हमारे पूर्वज’ में। असल में ‘हमारे पूर्वज’ मेरी बड़ी ही प्रिय पुस्तक थी। पुस्तक तीन खंडों में थी और छठी से लेकर आठवीं तक पढ़ाई जाती थी। हर क्लास में ‘हमारे पूर्वज’ का एक अलग खंड पढ़ाया जाता। पर मैं यह फर्क कहाँ मानता था? मेरे लिए तो यह पुस्तक भी कहानियों की ही एक पुस्तक थी, जिसमें प्राचीन चरित्रों और महापुरुषों की कथाओं का बखान था। इसलिए जब भी समय मिलता, मैं ‘हमारे पूर्वज’ पुस्तक खोलकर पढ़ने बैठ जाता।
एक बार कमलेश दीदी को हिंदी का होमवर्क मिला। वे अपनी कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक ‘हमारे पूर्वज’ मेरे आगे रखकर बोलीं, “इस पाठ का सार लिखना है। क्या तू बता सकता है कुक्कू…?
“कौन सा पाठ…?” मैंने उत्साहित होकर पूछा।
“‘हमारे पूर्वज’ का भरत वाला पाठ है। लिखवा देगा तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उत्तर कैसे लिखूँ।”
मैं बोला, “हाँ-हाँ, यह तो बड़ा आसान है, लो लिखो।” कहानी मुझे पता ही थी। इसलिए सार मैंने झटपट लिखवा दिया।
अगले दिन दीदी स्कूल से आकर बोलीं, “वाह रे कुक्कू! मैडम ने मेरी बड़ी तारीफ की। पूरी क्लास को पढ़कर सुनाया, जो तूने कॉपी में लिखवाया था।” कहते हुए दीदी का चेहरा चमक रहा था।
सुनकर मेरा जी खुश हो गया। हाथ जोड़कर भगवान जी से कहा, “अरे भगवान जी, मुझे पता नहीं था। आपने तो मुझे बड़ा अनमोल खजाना दे दिया। सॉरी, अगर मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो। मेरे लिए तो यही खजाना बड़ा अच्छा है। अब तो मैं इधर ही सरपट दौड़ूँगा। बस, इधर ही…! मुझे मिल गया अपना रास्ता।”
और सच्ची-मुच्ची, उसी दिन से मैं पागल हो गया, अक्षर-पागल…! कहीं भी छपे हुए अक्षर देखता तो बेसबरा हो जाता और लगता कि पी जाऊँ। कहीं भी कोई किताब, पत्रिका देखता, तो उसे बीच में कहीं से भी खोलकर पढ़ना शुरू कर देता और मुझे होश नहीं रहता था कि मैं धरती पर हूँ या आकाश में…या कि इस समय सवेरा है, दोपहर कि रात! बस, अक्षर को देखते ही उसे पी जाने का मन होता।
यह एक नई ही भूख थी, ज्ञान की भूख। नई ही प्यास थी, कविता और कथारस की प्यास…और इसके आगे बाकी सारी चीजें बेमानी थीं।
याद पड़ता है, ‘प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ’ पुस्तक तो मैंने एकदम छुटपन में ही पढ़ ली थीं। शायद पाँचवीं में। उनके उपन्यास ‘निर्मला’, ‘वरदान’, ‘गबन’ कक्षा छह-सात से शुरू हो गए। फिर साथ ही शरत और रवींद्रनाथ टैगोर के उपन्यास। एक करुण दुनिया थी वह। पढ़ते-पढ़ते मेरे आँसू आ जाते। एक हाथ में किताब पकड़े हुए दूसरे से आँसू पोंछता जाता। मगर पढ़ना वैसे ही जारी रहता, ताकि जल्दी से जल्दी जान लूँ कि आगे हुआ क्या!
मजे की बात यह कि कोई मुझे बताता न था कि कुक्कू, यह किताब अच्छी है, तू पढ़ ले। पर हर किताब जो भी संयोग से हमारे घर आ जाती, उस पर मेरी निगाह पड़ती ही थी। ईश्वर ने कुछ ऐसी नेमत बख्शी थी कि किताब से मैं, और किताब मुझसे दूर रह ही नहीं सकती थी। और पढ़ता तो लगता, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। लगता, जैसे यह किताब तो मेरे लिए, बस मेरे लिए ही लिखी गई थी। मैं कितना अभागा था कि अभी तक उससे दूर रहा।
मैं किताब पढ़ता और एक नई दुनिया में पहुँच जाता। फिर उस दुनिया से वापस आने में बहुत समय लगता। बहुत खीज भी होती थी। लगता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसी दुनिया में रहूँ…इस दुनिया में आना ही न पड़े!
यह पागलपन की हद थी। लेकिन पागलपन मेरे सिर पर सवार था। अक्षर-अक्षर पढ़कर इस दुनिया से उस दुनिया में पहुँच जाने का पागलपन।
“देखो तो, दुनिया में कितना बड़ा खजाना है और यों ही यहाँ-वहाँ बह रहा है, किसी को खबर ही नहीं।” मैं सोचता, “पर नहीं, मैं तो सारे काम छोड़कर इसे पढ़ूँगा। इसलिए कि किताब को पढ़े बिना मैं रह ही नहीं सकता।”
हर किताब मुझे ऐसी ही लगती। मुझे लगा, इन किताबों के जरिए मैं खुद को समझ रहा हूँ, दुनिया को समझ रहा हूँ। दुनिया के अंदर की बहुत सारी दुनियाओं को समझ रहा हूँ। और किताब के जरिए एक रोशनी सी मुझमें उतर रही है। अपने से ऊपर उठकर भी दुनिया को देखा जा सकता है, अक्षरों की यह रोशनी मुझे बता रही है। इसी रोशनी के सहारे टोहते हुए, मैं अपने अंदर-बाहर इस सवाल का भी हल खोजता कि इस दुनिया में इतने ज्यादा दुख क्यों हैं? लोग एक-दूसरे को बिना बात इतना सताते क्यों हैं? पहले ही दुनिया में इतने सारे दुख हैं तो लोग उन्हें और ज्यादा क्यों बढ़ा देते हैं? मैं पढ़ता और रोता, रोता और पढ़ता। …
तब से आज कोई साठ बरस का लंबा अंतराल निकल गया, पर न मेरे सवाल खत्म हुए और न यह हैरानी भरी ऊहापोह कि, “हे राम जी, दुनिया में इतने दुख क्यों हैं? दुनिया क्या ऐसी नहीं हो सकती कि लोग थोड़ा दुख-दर्द से उबरकर हँसें। थोड़ी खुशी महसूस करें। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि दुनिया के दुख और तनाव थोड़े कम हो जाएँ?”
*
रास्ता तो तब भी नहीं था और आज भी यकीन से नहीं कह सकता कि मिल गया है। पर साहित्य के जरिए भी हम एक दुनिया बसाते तो हैं। एक अच्छी दुनिया, एक सुंदर दुनिया, जो हमें बहुत सारी बुराइयों और विद्रूपता से परे ले जाती है। पढ़ने वाले को भी लगता है, हम अंदर से कुछ बदल रहे हैं। फिर बाल साहित्य की तो शायद पहली शर्त ही यह है कि वह बच्चों को आनंदित करे, और खेल-खेल में ही उनके मन में कोई अच्छी बात भी उतार दे।
मुझे याद है, बरसों पहले मैं मत्त जी से मिला था। बच्चों के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल मत्त। मैंने उनसे पूछा कि “मत्त जी, आपके विचार से एक अच्छी बाल कविता क्या है?” सुनकर उन्होंने मुसकराते हुए कहा, “मनु जी मैं तो उसी को अच्छी बाल कविता मानूँगा, जिसे पढ़ या सुनकर बच्चे के मन की कली खिल जाए।…यानी जो बच्चों को आनंदित करे। वरना आप चाहे जितने भी जतन करें, चाहे जितने अच्छे-अच्छे विचार उसमें लेकर आएँ, अगर वह बच्चों को आनंदित नहीं करती तो अच्छी बाल कविता नहीं हो सकती।…”
मैं समझता हूँ, यह बात पूरे बाल साहित्य के लिए कही जा सकती है। और बाल साहित्य ही क्यों, समूचे साहित्य के लिए क्यों नहीं? अपनी रचना में आप चाहे करुणा का भाव लाएँ, या फिर कोई जीवन-दर्शन कोई विचार, जब तक वह पाठकों को रंजित नहीं करती और उनके मन में नहीं उतर जाती, उसे अच्छी साहित्यिक कृति तो नहीं ही कहा जा सकता। प्रेमचंद इस मामले में आज भी आदर्श हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में देश-समाज की एक से एक बड़ी समस्याएँ उठाईं, पर आज भी वे सबसे अधिक पढ़े जाने वाले साहित्यकार हैं। उनकी कहानियों और उपन्यासों में वह रस-आकर्षण है कि आप उन्हें पढ़े बिना रह ही नहीं सकते।
इसी ओर शायद मत्त जी भी इशारा कर रहे थे।…यानी यह आनंद भाव ही किसी कृति को पाठकों की पसंदीदा कृति बना देता है।
इसीलिए बरसों बाद जब बाल साहित्य की ओर आया तो मेरे मन में यह बात बहुत गहराई से गड़ी हुई थी कि बच्चों के लिए ऐसा लिखूँ जो उन्हें थोड़ी खुशी दे। साथ ही खेल-खेल में जो उनके अंदर की उलझनों और गुत्थियों को सुलझाए और चुपके से रास्ता भी बता दे।
जाहिर है, इसके लिए फिर से मुझे बचपन की ऊबड़-खाबड़ गलियों में जाकर उस जिए हुए को पुनःसृजित करने की जरूरत पड़ी। मेरी कई कहानियों में बेशक मेरे बचपन की झलक है। हालाँकि वे अऩुभव मेरी कहानियों में ढलकर कुछ नए रूप में तो जरूर ही ढल गए होंगे। हो सकता है, कुछ आज का बचपन भी उनमें जुड़ गया हो। पर बचपन की दुनिया सचमुच अमोल है। वह कल भी थी, आज भी है। बचपन ऐसा अनमोल खजाना है, जिसे खोजने निकलो तो पैर परिचित पगडंडियों और रास्तों पर चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं…और फिर वापस आने का मन नहीं करता।
**