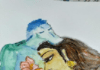तराज़ू
“तुम अगर फोन पर बता देती तो मैं बना देता ना कुछ, या फिर ऑर्डर ही कर देता। देर तो नही होती इतनी।”
विक्रम असहाय सा झल्ला रहा था।
“अब मैने देरी से आने का फोन किया था, तब ये सब कुछ तो तय ही था, अलग से बताने की क्या जरुरत थी?
रहने दो, हमेशा का ही है। आदत हो गई है मुझे।” वाणी बुझे मन से थके तन से रसोई में मशीन बनी हुई थी। विक्रम जैसे पूछताछ की औपचारिकता पूरी कर, पैर पटकता हुआ जाकर टीवी के सामने जम गया। भोजन के समय तक विक्रम तरोताज़ा था, टीवी ने सारी बातों को भुला दिया था।
“अरे, तुम्हे क्या हो गया, थकान ज्यादा हो गई है क्या? या उम्र हो चली है?” छेड़ने के अन्दाज़ में वह बोला।
“भूलने तो तुम लगे हो, उम्र दोनो की हुई है, असर तुम्हे हो रहा है।” वाणी अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराई।
“तुम औरतों को पहेलियों में बात करना क्यों अच्छा लगता है? इस दाल में कसूरी मेथी ड़ालती तो और बेहतर लगती।” और वाणी जान चुकी थी, बात बदलने में माहिर विक्रम ही क्या, इस पूरी मानसिकता को ही। समय पर ड़ालियों की काट छांट करने वाला माली, बेरहम नही कहलाता। उसे समर्पण और स्वाभिमान में संतुलन लाने के लिये अब तराज़ू अपने हाथ में लेना ही होगा।
“कल शायद फिर से देर हो जाए। फिर मत कहना कि पहले नही बताया। वो कसूरी मेथी लाल ढ़क्कन वाले कांच के मर्तबान में है।”
(२) शाश्वत
खूब प्यासी आंखे लेकर सुरेखा ने देहरी के अंदर पांव रखा था। भगवे वस्त्रों की महिमा से परे, रुद्राक्ष, चन्दन टीके से कोसो दूर आज वह पिता की ’रानू’ बनकर जीने आई थी। गोबर से लीपे जाने वाले फर्श पर अब पत्थर मढ़े हुए थे। दीवारें, आंगन और हवाएं भी लंबे समय के साथ अजनबी हो चली थी। लेकिन सुरेखा का मन अब भी किशोर था। ब्याह की लाल चुनरी ओढ़ाने को तत्पर परिवार के सामने उसने त्याग, तपस्या, भौतिकता की नि:स्सारता का दर्शन रख दिया था। अब गुरु का आश्रम ही उसका शाश्वत धाम था। परिवार ने पसीजकर, असंतुष्ट होकर और मन पर पत्थर रखकर ही उसे अनुमति दी थी। इस बीच आश्रम की जीवनचर्या को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था उसने। वर्षों की साधना, तपस्या, तीर्थयात्रा और संयमी जीवन के बीच, कई बार मन में घर की बेर निंबौलियां विद्रोह कर जाती। तब पिता के आखरी बार कहे शब्द वह मन ही मन दोहराती। “रानू बेटी, कभी भी लगे, कि ये निर्णय गलत हो गया है, तब बिना सोचे समझे घर आ जाना। मैं हमेशा ही तुम्हारी राह देखा करुंगा।” इस अबूझ सी बिदाई पर कोई भी पिता क्या कह सकता है भला। और सुरेखा के मन में घर की चौखट पर हमेशा ही कल्पना के फूल बिछे रहते। पिता की आंखों को जैसे उसकी ही प्रतीक्षा है, घर भर उसके आने से रौनक पा गया है। इन्ही, वर्षों तक सांस देती कल्पनाओं की पोटली थामे वह आज साक्षात पिता के सामने थी। पिता के जर्जर कांधे, पहले तो “वापसी” की अनहोनी सोचकर कांप उठे, फिर जब ’सिर्फ मिलने’ वाला अर्थ मिला, तब सहज हो पाए। झुकी कमर, थकी देह, बेटे की उपेक्षा से असहाय हो उठे ये वाले पिता, सुरेखा के लिये अजनबी थे। सन्यास की मर्यादा उसे ’रानू’ बन जाने से रोके रही लेकिन कोई बंधन न होने के बावजूद पिता ने कोई पहल नही की। उसकी दिनचर्या, अपनी बीमारी, खेती किसानी और परिवार की बातों के बीच के धागे में जाने कितनी गांठे आती गई। समय बहुत कुछ खा गया था। बुझे मन से सुरेखा चल दी, एक बार फिर, यह जानते हुए भी कि अब कोई रोकने वाला नही है, गिरते हुए मन के कांच के बर्तन को खूब सम्हालना चाहा, लेकिन भुलावे के हाथों में न आकर वह ’छन्न’ हो ही गया। उसे वास्तविक आत्मज्ञान अब हुआ था। कुछ भी तो शाश्वत नही है।
 अन्तरा करवडे
अन्तरा करवडे
संक्षिप्त परिचय
शिक्षा: बी.कॉम, एम.आई.बी
कार्यक्षेत्र: भाषा सेवाएं, बहुभाषी अनुवाद व वाणी सेवा, हिन्दी व मराठी साहित्य लेखन, श्रव्य कार्यक्रम लेखन,
निर्देशन व निर्माण.
प्रकाशन: तीन मौलिक व अनेक अनूदित पुस्तकें, वेब सामग्री, ऑडियो पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं व
वेबस्थलों पर नियमित प्रकाशन, पत्रिका इन्द्रदर्शन का सम्पादन.
उपलब्धियां: अखिल भारतीय अम्बिकाप्रसाद दिव्य रजत अलंकरण, महाराजा कृष्ण जैन स्मृति पुरस्कार, केशरदेव
बजाज पुरस्कार हिन्दीतर लेखन हेतु’भारति रत्न’ उपाधि, रेडियो वेरितास एशिया का ’सत्य स्वर’ रजत जयंति सम्मान, क्रोएशियन इन्डोलॉजिस्ट्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रह में लघुकथा चयनित.
संप्रति: प्रतिष्ठान ’अनुध्वनि’ के माध्यम से अनुवाद, वाणी, लेखन सेवाएं व रेडियो वेरितास एशिया
पर हिन्दी कार्यक्रम निर्माण.
संपर्क
अन्तरा करवडे
अनुध्वनि
117, श्री नगर एक्स्टेन्शन
इन्दौर, म.प्र, भारत – 18
+91 9752540202
greatantara@gmail.com
www.anudhwani.com