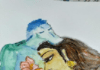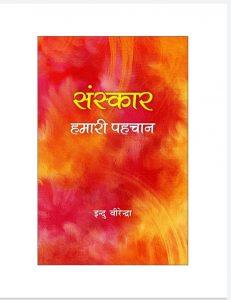
डॉ रवि रंजन ठाकुर
मनुष्य के जब मनुष्य होने की बात की जाती है तो मनुष्यता पर चर्चा पहले होती है। मनुष्यता को निखारने और सँवारने का काम संस्कार करता है। व्यक्ति चाहे जिस धर्म, जाति, समुदाय, समाज से संबंध रखता हो संस्कार ही उसे मनुष्य की कोटि प्रदान करता है तथा इसी से उसकी अपनी पहचान बनती है। ‘संस्कार हमारी पहचान’ पुस्तक में इसी तथ्य का प्रतिपादन लेखिका प्रोफेसर इन्दु वीरेन्द्रा द्वारा किया गया है। संस्कार शब्द पर विचार करते हुए वे मानती हैं कि “आचार -विचार की प्रेरणा देने वाले, यथोचित मार्ग दर्शन करने वाले तथा कर्म-संपादन की मर्यादा स्थिर करने वाले सूक्ष्म सूत्र, जिसकी अमिट छाप होती है, संस्कार कहे जाते है।” संस्कार ही वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा मनुष्य उचित-अनुचित का भेद कर पाता है।यही भेद उसे बौद्धिकता की श्रेणी प्रदान करता है जिससे समाज एवं राष्ट्र का उत्थान संभव हो पाता है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति के बाद जिस लक्ष्य तक पहुचने की बात हमारे प्राचीन ग्रंथों में कही गई है उसका सन्धान संस्कार से ही संभव हो सकता है। “केवल मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने से ही जीव का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता।” लेखिका का यह कथन कई बिन्दुओं पर सोचने को बाध्य करता है। जो धर्म से लेकर आधुनिकता तक पहुॅचता है। उनका मानना है कि “चरित्र का निर्माण व्यक्ति अपनी सहज प्रवृत्तियों को बुद्धि द्वारा नियंत्रित और संस्कारित करके करता है।” आज के समय मे चरित्र निर्माण की आवश्यकता कितनी अधिक है यह बताने की ज़रूरत नही है।
इन्दु वीरेन्द्रा द्वारा लिखित पुस्तक ‘संस्कार हमारी पहचान’ साल 2021 में ए.आर पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली से छपकर आई है। नाम के अनुकूल ही पुस्तक में संस्कार के महत्व को बताते हुए इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया है। पुस्तक को पढ़कर संस्कृत के प्राचीन विद्वान मार्तण्ड की एक उक्ति याद हो आती है कि “कवि का धर्म मनुष्य की आत्मा को बचाना नहीं बचाने के योग्य बनाना है।” इस पुस्तक के लेखन से इन्दु जी ने मनुष्य की आत्मा को पतन से बचाने के योग्य बनाने का प्रयास किया है। वर्तमान समय मे जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें एक बौखलाहट के साथ धैर्य का घोर अभाव दिखाई देता है। यहां स्वयं के लिए भी समय नही है।ऐसी स्थिति में संस्कार का विकास होना मुश्किल प्रतीत होने लगता है। “भौतिक अंधानुकरण ने हमारी बुद्धि, विचार, शक्ति,एवं विवेक-ज्ञान को कुंठित कर दिया है। प्राचीन ज्ञान को सुनने एवं स्वीकारने में लज्जा का अनुभव करने वाली हमारी पीढ़ी, तभी तो अपनी पहचान नही बना पा रही है।” आज भौतिक सुख प्राप्ति के लिए मनुष्यों में होड़ लगी हुई है। जिसके लिए गलाकाट प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर है। इस प्रतिस्पर्धा ने जहाँ नैतिकता, सद्भाव, दया, करुणा तथा मूल्यों का लोप कर दिया है, वहीं विभिन्न जघन्य अपराधों को जन्म दिया है। सम्पूर्ण विश्व इस व्यवस्था से त्रस्त एवं संक्रमण के इस माहौल से क्षुब्ध दिखाई दे रहा है। वर्तमान चिंतकों को इसका निदान प्राचीन संस्कारों एवं मूल्यों के विकास में दिखाई दे रहा है। हमारे ऋषियों-मुनियों द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसरण से जीवन मे शांति का उद्भव दिखाई दे रहा है। इन्दु वीरेंद्रा जी की यह नवीनतम पुस्तक इसी तथ्य की पहचान करवाती है। इसका पठन व अध्ययन चिंतन के कई द्वार खोलता है। जिसमें छोटे-छोटे प्रसंगों के माध्यम से जीवन की सहजता को दिशा देने वाले तत्वों को उद्घाटित किया गया है, जो कि सराहनीय है।
पुस्तक में उपनिषद काल से लेकर आधुनिक बंगाली विद्वान श्री विश्वनाथ शास्त्री तक के संदर्भ का प्रतिपादन है। इन संदर्भों के उल्लेख से लेखिका ने जिन तत्वों को दिखाने का प्रयास किया है वह मानवतावाद को प्रोत्साहन देते हुए मनुष्य को मनुष्य होने की शिक्षा देता है। यद्यपि लेखिका का आयाम यहाँ विस्तृत है लेकिन अपनी कुशल और सधी लेखनी से लेखिका ने इसे विवेचित कर ग्रहणीय बना दिया है। इन्द्र, लोमश, जनक, प्रह्लाद, ध्रुव, मुदगल इत्यादि पौराणिक पात्रों की कहानियों के द्वारा उन्होंने अहंकार, ऐश्वर्य, विलास इत्यादि से उपजे मद मत्सर की ओर संकेत किया है, तो भक्ति, वैराग्य, तपस्या की महत्ता के जीवनोपयोगी लाभ को स्पष्ट कर उसकी वर्तमान सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। गुरु नानक देव एवं दौलत ख़ाँ के प्रसंग श्रद्धा के मर्म स्थल पर पहुॅचने का संकेत देते हैं। शेख सदी के ‘गुलिस्तां’ के आख्यान द्वारा सुखमय जीवन के लिए भोग और स्वस्थ दृष्टि कोण को समझाने का प्रयास है। सुख केवल भोग में नही अपितु स्वयं को दुरुस्त रखने में है। अहंकार की व्यर्थता को लेखिका ने ‘केन उपनिषद’ की कथा से स्पष्ट किया है। इन सभी के माध्यम से यहाँ सिद्ध किया गया है कि मनुष्य की पहचान भौतिकता से नही संस्कार से है। “निरंतर धारण किया गया विचार ही कृत्य बन जाता है और सूक्ष्म शरीर पर अंकित होता रहता है। सूक्ष्म शरीर पर अंकित होने वाले कृत्य ही संस्कार बनते हैं जो अवचेतन मन के माध्यम से मनुष्य के मन और मनोवृति को प्रभावित एवं नियंत्रित करने के साथ ही उसे निर्देशित भी करते हैं। आगे चलकर संस्कारों की यही दृढ़ता चरित्र में परिवर्तित हो जाती है।” कहा जा सकता है कि वैचारिक उच्चता तथा शाश्वत मूल्य बोध ही हमे सांस्कारिक स्तर पर दक्ष बना सकते है। पौराणिक कथाओं से स्पष्ट होता है कि संस्कार से देवत्व की प्राप्ति संभव है। प्रह्लाद, विभीषण, त्रिजटा, इत्यादि दानव वंश के थे, फिर भी अपने संस्कार से देवताओं के करीब थे। तक्षक नागवंशी था, सुकेश रावण की मां कैकसी के पूर्वज थे लेकिन इन्हें देवताओं के साथ स्थान मिलने का कारण इनका संस्कार था। हनुमान, जामवंत, जटायू इत्यादि अनेकों उदाहरण दिए है जो संस्कारों के कारण देवता के समीपस्थ हुए। संस्कार किसी के लिए लाभदायक ही सिद्ध हुआ है। ‘हाजी पीर’ कच्छ के रन में आज अगर हिन्दू-मुस्लिम दोनो के द्वारा पूजे जा रहे है तो इसके पीछे उनका उत्तम आचरण है। इतिहास द्वारा उनके उत्तम आचरण की पुष्टि होती है जो संस्कार से ही संभव हो पाती है। हज़रत मूसा और गरीब लकड़हारे की कथा द्वारा अल्लाह को स्वयं में आत्मसात करने की बात कही गयी है। विष्णु पुराण में अजामिल प्रसंग नाम की महिमा को बताता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा का वर्णन किया है। अगर नाम महिमा के महत्व को हिन्दू और अल्लाह को स्वयं में आत्मसात करने की शिक्षा को मुस्लिम समझ लें तो वर्तमान मंदिर-मस्जिद का झगड़ा ही मिट जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि पौराणिक ग्रंथ अपने प्रसंगों में जिन अभिप्रायों को समेटे होता है वह कई गूढ़ तत्वों से अवगत कराने का काम करता है। इन्दु वीरेन्द्रा जी ने इस पुस्तक से यही समझाने का प्रयत्न किया है। भारतीय और यूनानी मिथक में पूरब पश्चिम का अंतर है। ययाति और एटिपस की कथाएँ इसे स्पष्ट कर देती हैं। एक तरफ बुजुर्ग के लिए यौवन का त्याग है तो दूसरी तरफ उसकी हत्या है। दोनो कथा के केंद्र में बुजुर्ग और युवा शक्ति की मौजूदगी है। लेकिन दोनों का प्रभाव कैसा है? यह स्वयं विचारणीय है। संस्कार वह शक्ति है जो औरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता तलाश कर लेती है। संस्कार से ही मनुष्य जन्म को सार्थकता मिलती है। “मनुष्य को अपना एक-एक पल नियमों का पालन और जीवन के वास्तविक उदेश्य की पूर्ति में लगाना चाहिए, इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है।” अपने इस कथन से लेखिका ने मनुष्य के चराचर जगत में उसके चेतनागत स्तर पर बौद्धिक आयाम को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुस्तक में जगह जगह वह अपने विचारों से अवगत कराती हैं।
डार्विन का विकासवाद जिस स्पीशीज के विकास की बात करता है उसका मूल यहाँ शुरु से मौजूद रहा है। माँ के गर्भ से ही संस्कार दिए जाने की बात भारतीय संस्कृति करती है। डार्विन के सिद्धांत में जिस एक जिन के बच्चे का विरोध दिखाई देता है वह भारतीय संस्कृति के संस्कार बिंदु पर संघात खाता है। संस्कार का निर्माण मूल रूप से माँ केंद्रित अध्यात्म और विज्ञान दोनों मानता है। लेखिका यहाँ यह तर्क देती दिखाई देतीं है कि “अपनी संतान को यदि सुसंस्कृत एवं राष्ट्रपयोगी बनाना है तो सर्वप्रथम इसके मूल में मातृशक्ति को मानना होगा।” माँ अपने संतति की उत्तम मार्गदर्शिका होती है। मनुस्मृति और पराशर स्मृति में माँ के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि गया में पिता के लिए एक बार पिंड देने से उनके ऋण से मुक्ति मिलती है तो मातृ ऋण से मुक्ति के लिए गया में सात बार माँ के लिए पिंड देना आवश्यक है। वेदों में ‘मातृ देवो भव’ कहा गया है। यहां पितृसत्तात्मक मानदंड में मातृ सत्ता का महत्व दिखाई देता है। लेखिका मानती है कि “मूल रूप से समूचे राष्ट्र के चरित्र का प्रकाशन एवं गौरव -गरिमा मंडन का आधार मातृ शक्ति है। “परिवार के विकास के साथ ही संस्कार की आवश्यकता महसूस की गई, श्वेतकेतु की कथा इसकी पुष्टि करती है। यह ऐसा सत्य है जो हर काल और समय में अटल रहा है। इस पुस्तक के एक प्रसंग में अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि “सत्य वह है जो प्रत्येक काल मे विद्यमान रहे।” संस्कार मनुष्य का सत्य है इसके विकास से ही उसका पूर्ण विकास संभव है। इसी को पाकर व्यक्ति विनयशील, दयालु, धार्मिक, सामाजिक, विचारवान बन पाता है। रज़िया सुल्तान का सूफ़ी संत कलीमुद्दीन के सामने नतमस्तक होना या ख्वाज़ा बख्तियार काकी से उपदेश प्राप्त करना, महान सम्राट अकबर द्वारा दीन-ए-इलाही का प्रतिपादन करना, दाराशिकोह का सूफ़ी सरमद से दीक्षा लेना इन सब के मूल में देखा जाए तो संस्कार की महत्वपूर्ण भूमिका दृष्टिगत होती है। लेखिका लिखती है कि “शासनाधिकार के कारण जिनका सिर अभिमान से सदा तना रहता था, आज वे कहाँ हैं?” इंसान की प्रतिष्ठा संस्कार से संभव है, अहंकार से नही। “इंसान जो संसार मे अपने को स्थिर समझे हुए है और अपने मद में किसी को कुछ नहीं जानता, कितने बड़े आश्चर्य की बात है?” जरूरत अहंकार को त्यागकर स्वयं को एक पूर्ण मनुष्य के रूप में विकसित करने की है, जिससे एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र का निर्माण संभव है। लेखिका का ध्येय इसी तथ्य को प्रतिपादित करना है।
इस पुस्तक को इन्दु वीरेन्द्रा जी ने आठ अध्यायों में बांटा है। प्रत्येक अध्याय अपने आप मे समग्र रूप से अपनी बात कहने में सक्षम है। पुस्तक में संस्कार के बाद लेखिका मनुष्य के उत्तम कर्म पर बल देती नज़र आती है। उनका मत है कि ‘उत्तम कर्म’ से ही सुखमय जीवन संभव है। “देखा जाए तो यह सत्य है कि किसान खेत मे जैसा बीज बोता है, उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है।” संसार की माया व्यक्ति को उसके लक्ष्य से पदच्युत कर देती है जिसको संभालने का काम संस्कार करता है। सुख की कामना ही दुःख का कारण बनती है। कालिदास ने कहा था कि इस संसार मे सुख की चाहत ऐसी है जैसे शमी के वृक्ष को पद्मपंखुरी की धार से काटना है। “दुनिया मे हरेक इंसान सुख का खोजी है। दुनिया की जितनी भी दौड़-धूप, खींचा-तानी और कशमकश होती दिखाई देती है, इन सबके पीछे यही सुख प्राप्ति की इच्छा है।” सुख की यह चाहत किसी भी स्तर तक पहुॅच जाती है जिसकी प्राप्ति के प्रयास में मनुष्य पतन की ओर निरंतर गतिशील होने लगता है। अगर उसमें उत्तम संस्कार है तो वह ग्राह्य और अग्राह्य का विचार कर पाता है। विचारों की शक्ति उसे पतनशील होने से बचा लेती है। लेखिका का मानना है कि स्त्री हो या पुरुष व्यक्ति रूप में संस्कार का औचित्य मूलतः मानवतावादी दृष्टि का विकास है जो युग सापेक्ष होकर मनुष्य के इतिहास दृष्टि का पोषक होता है।
संस्कार के कई पक्ष होते है। हिन्दू धर्म में, जन्म से मरण तक ,जो सोलह संस्कार निर्धारित किये गए है, उनमें यह देखने को मिलता है कि ब्राम्हण से शूद्र कहे जाने वाले वर्ण तक की बराबर भागीदारी होती है। यहाँ संस्कार सामाजिक सरोकारों को एक प्रकार से व्याख्यायित कर देता है। वहीं इसका दूसरा पक्ष व्यक्तिगत व्यवहार को निर्धारित करता है। तीसरे पक्ष की बात की जाए तो कर्म की प्रधानता को यह दर्शाता है जिसका विशद् वर्णन लेखिका ने इस पुस्तक में किया है। “संस्कार को वहन करने वाला जीव है। संस्कार को बनाने सँवारने, पोषण एवं नाश करने वाला कर्म है। जीव का कर्म से अभिन्न संबंध है। स्थूल शरीर से कर्म होता है। सूक्ष्म शरीर से संस्कार होते है। कारण शरीर में जीव रहता है। जीव कर्ता होने से सुख-दुःख का भोक्ता होता है।” अर्थात संस्कार और जीव का संबंध अगर घर है तो दोनों को बांधे रखने वाली रस्सी कर्म है। लेखिका कर्म को प्रधानता देती है। इस बिंदु पर उनके विचार ओशो से मिलते जुलते प्रतीत होते है। लेखिका का समर्पण और कर्म से सफलता की प्राप्ति चिरंतन काल से चली आ रही सद्भावना है ।
पुस्तक में रामचरितमानस तथा गुरुग्रंथ साहिब से कई प्रसंग लेकर उनकी विवेचना की गई है। यह एक नए आयाम के साथ उनके दृष्टिगत उर्वरता का परिचायक है। संस्कार कैसे पनपता एवं विकसित होता है किन-किन स्थितियों में यह फलता- फूलता है ,पुस्तक में इसका आकंलन देेखा जा सकता है। सुसंस्कार मनुष्य को बौद्धिक धरातल पर सचेत रखता है ऐसा लेखिका का मानना है। “जो शारीरिक एवं सांसारिक कार्य -व्यवहार करते हुए भी परमात्मा का नाम -सुमिरन ध्यान में लगाए, सच्चे अर्थों में ऐसा व्यक्ति जगा हुआ है।” दुनिया की भीड़ में स्वयं को खो देना मुश्किल नहीं है। स्व को स्थापित करना अवश्य मुश्किल है। यह संस्कार से ही संभव है कि भीड़ में हम अपनी अलग पहचान कायम कर सकें। वैभव से भी अलग पहचान बनाई जा सकती है। लेकिन विचारणीय यह है कि वैभव से बनी पहचान क्षणभंगुर है तो संस्कार से बनी पहचान शाश्वत है। जिंदगी है तो अनेकों उलझने सामने है इनसे निकल कर या इनका संयत संयोजन कर ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। पुस्तक के अंत मे इसी तथ्य का निरूपण किया गया है। सज्जन व्यक्ति और मेंढक वाली कहानी के प्रसंग द्वारा लेखिका ने बहुत रोचक ढंग से अपनी बात पुस्तक के अंत मे कही है जिसमें संवाद का गठन उनके व्यक्तित्व की पहचान करवाती हैं। इतना अवश्य है कि पुस्तक पठनीय है। सधी हुई भाषिक चेतना इसे सरलता से ग्रहणीय बना देती है। अगर पाठक धार्मिक, सांस्कृतिक पक्ष को समझने -पहचानने का पक्षधर हैं तो इसे पढ़ना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा।
वर्तमान समय मे हमारे जीवन मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। साहित्यकार अपने चिंतन से इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने में लगे रहते हैं। समय-समय पर समसामयिक बोध करने का कार्य इनके द्वारा सम्पन्न होता रहता है। कहना न होगा कि इन्दु वीरेंद्रा ने समय की जटिलता को पहचान कर ही इस पुस्तक का सृजन किया है। आज के संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर जिस संस्कार की आवश्यक्ता प्रमुखता से महसूस की जा रही है उसे इस पुस्तक में समझाकर इन्दु वीरेन्द्रा जी ने समाज -हित में अपना योगदान दिया है। आज जिस मार्गदर्शन की आवश्यक्ता है, वह केवल धर्म ग्रंथों के उपदेशों से संभव नही हैं। जरूरत उसे समझ कर उसके तत्व रूप से जनता को अवगत कराने की भी है।तभी उसके सार्थक परिणाम आना संभव है। इस क्षेत्र में इन्दु वीरेन्द्रा का यह योगदान उपयुक्त एवं प्रशंसनीय है।

डॉ रवि रंजन ठाकुर
संपर्क – traviranjan@gmail.com