भारतीय साहित्य में चित्रा मुद्गल के नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आवां, नाला सोपारा जैसी कृतियाँ आज आपकी पहचान बन चुकी हैं। पिछले ही साल ‘नाला सोपारा’ के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित चित्रा मुद्गल बीते लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के कारण भी चर्चा में आई थीं। आज साक्षात्कार श्रृंखला में युवा लेखक पीयूष द्विवेदी ने उनसे उनके व्यक्तित्व, कृतित्व सहित विविध पहलुओं पर बातचीत की है।
सवाल – अपने प्रारंभिक जीवन के विषय में कुछ बताइये। मैंने पढ़ा है कि आपका जुड़ाव आन्दोलनमुखी संगठनों से रहा है? ये कैसे हुआ और इसने किस प्रकार आपके जीवन और लेखन को प्रभावित किया?
चित्रा जी – मुझे लगता है कि कॉलेज के दिनों में जो विद्यार्थी विचारधारा से जुड़ा और अपने समय-काल के प्रति सजग रहता है, उसके मन में समाज के लिए कुछ करने की भावना आ ही जाती है। अपने अंदर मैंने ये महसूस किया कि गलत चीजों का प्रतिरोध मुझमे उपजता था और उन चीजों का विरोध मैं करती थी, जो मुझे सही नहीं लगती थीं। मेरे अंदर यह भी गुस्सा था कि पुरुषों के लिए स्त्रियाँ घर में घूँघट क्यों काढ़ती हैं? बाबा के घर में घुसते ही हुंकारी भरने पर सब स्त्रियाँ आड़ में हो जाती थीं। मुझे इससे विरोध था। दूसरी बात यह लगी कि पुरुष के अलावा दादी जो कि एक स्त्री हैं, उनके सामने भी घर की बहुएं क्यों पर्दा करती हैं? अगर वो घूँघट नहीं काढ़तीं तो दादी उनको फटकार लगाती थीं। मुझे ये बड़ा अजीब लगता था। इन चीजों के कारण मन में एक असंतोष उपजता था और वही असंतोष कॉलेज में आने के बाद प्रखर हुआ।
सोमैया कॉलेज जो मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत था, जहां मैं पढ़ती थी, में रक्षाबंधन के दिन कहा जाता था कि सब छात्र और छात्राएं आएंगे तथा हर लड़की सब लड़कों को राखी बांधेगी तथा वे आपस में भाई-बहन का रिश्ता रखेंगे। रक्षाबंधन के दिन चाहें जो भी सोच के ये उत्सव शुरू किया गया हो, लेकिन मुझे बहुत नागवार गुजरा। मैंने इसका विरोध किया और कहा कि रक्षाबंधन के दिन मैं घर पर रहूंगी और अपने भाईयों कुंवर कृष्ण प्रताप सिंह और कुंवर कमलेश बहादुर सिंह को राखी बांधूंगी। जिसके भाई-बहन न हों, वे अगर बांधते-बंधवाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इस उत्सव को स्वीकार नहीं कर सकती। गलत बातों के प्रति मेरे मन में जो असंतोष उपजा, उसने मेरे प्रारंभिक जीवन को बदला और इस बात की तस्दीक की कि कोई भी गलत काम हो रहा है, तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। मेरी इसी सोच ने मुझे ट्रेड यूनियन से जोड़ा और ट्रेड यूनियन ने मेरी जिन्दगी बदलकर रख दी। तब मेरे सामने जिंदगियों के वो पृष्ठ खुले जो मैंने कभी देखे नहीं थे।
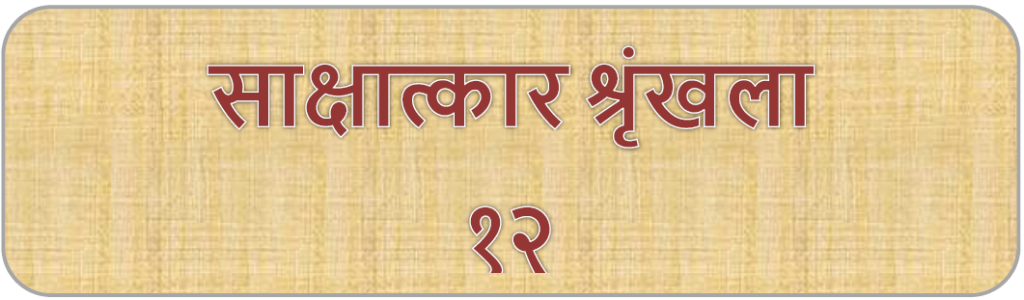
सवाल – साहित्य की तरफ कब और कैसे रुझान हुआ?
चित्रा जी – ट्रेड यूनियन से जुड़ने के बाद मजदूरों की बस्तियों, घरों में जाने लगी, तब एक अलग दुनिया मेरे सामने आई। कह सकती हूँ कि मेरी दुनिया बड़ी होने लगी। मैंने जाना कि जिस दिन इनके यहाँ मजदूरी नहीं पहुँचती, इनके पति दारू पीकर कहीं पड़ जाते हैं, उस दिन इनके घर चूल्हे नहीं जलते हैं। मुझे लगा कि मैं अभी इन लोगों के बीच बोलती तो हूँ, इन्हें समझाती तो हूँ, इनकी अप्लिकेशन तैयार कर देती हूँ, लेकिन ये सबकुछ इनके और मेरे बीच ही रह जाता है। लेकिन इन मजदूर बस्तियों के बाहर जो दुनिया सम्पन्नता के बीच डोलती है, उसतक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। तब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए। जब ये बात अखबारों में छपेगी, किताबों में छपेगी तो वो इस बस्ती और गलियों से निकलकर उन संपन्न लोगों तक पहुंचेगी। बस यहीं से लिखने की तरफ रुझान हुआ।
सवाल – आपके लेखन के आरंभिक दौर में कमलेश्वर जी, राजेन्द्र यादव जी जैसे लेखक हिंदी साहित्य में चर्चित नाम थे, क्या इनके लेखन व विचारों का कोई प्रभाव आपकी लेखनी पर भी पड़ा?
चित्रा जी – जहां तक मुझे याद है, मैंने राजेन्द्र यादव की कहानी ‘बिरादरी बाहर’ धर्मयुग में पढ़ी थी। सारिका में भी उनकी कहानी पढ़ी। तब सारिका के संपादक चन्द्रगुप्त विद्यालंकार हुआ करते थे। चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के समय में मैंने इन लोगों की कहानियाँ पढ़ी थीं। कृष्णा सोबती को भी पढ़ा। मुझे कुछ कुछ याद आता है कि तब कृष्णा सोबती को सारिका में ‘मित्रो मरजानी’ या ‘डार से बिछड़ी’ में अश्लीलता आदि कारणों से सारिका में बैन कर दिया गया था। तो बात ये है कि मैंने इन लोगों को पढ़ा जरूर था। कमलेश्वर जी की कहानियाँ मुझे अच्छी लगती थीं। मैंने उनकी ‘नीली झील’ ‘एक सड़क सत्तावन गलियां’ ‘देवा की माँ’ जैसी कहानियाँ, उनका छोटा-सा उपन्यास ‘डाक बंगला’ आदि पढ़े। लेकिन प्रभावित होने की जहां तक बात है तो वो अगर मैं किसीसे हुई हूँ, तो वो विश्व के दो लेखकों से – एक प्रेमचंद से उनकी कहानी ‘ठाकुर का कुआँ’ पढ़कर और दूसरा मैक्सिम गोर्की से उनका उपन्यास ‘माँ’ पढ़कर।
ठाकुर का कुआँ पढ़कर मुझे लगा कि ये तो मेरे घर की कहानी है। गाँव में मेरे घर के सामने दुआर पर जो पक्का कुआं बना हुआ है, उसमें अगर कोई पानी भर सकता है तो सिर्फ मेरे घर की कहारें, मेरे घर के लिए भर सकती हैं। बगल में ही दलितों का टोला था, लेकिन उनके पास जमीन पर खुदा हुआ एक कच्चा कुआं था, जिसमें से बाल्टी में रस्सी बांधकर पानी खींचते थे। लेकिन वो हमारे कुएँ से पानी नहीं खींच सकते थे, न ही उसे छू सकते थे। लेकिन ‘ठाकुर का कुआँ’ पढ़ने से पहले मुझे अपने घर की और समाज की ये विसंगति कि पानी पर भी जाति-बिरादरी का नाम लिखा गया है, नजर नहीं आई थी। इस तरह इस कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया।
इस तरह प्रेमचंद का प्रभाव मुझपर रहा और आगे मैंने उनकी सेवासदन, गोदान आदि सभी कृतियों को पढ़ लिया। इसी दौरान मैंने हिन्द पॉकेट बुक्स से मैक्सिम गोर्की की तीन रुपये में ‘माँ’ खरीदकर पढ़ी। इस उपन्यास में जारशाही के खिलाफ विद्रोहरत अपने बेटे पावोल पर उसकी माँ अविश्वास करती है कि ये बिगड़ चुका है, पता नहीं किन फ़ालतू के कामों में रहता है। उसे समझती नहीं है। लेकिन जिस दिन पावोल आन्दोलन के मैदान में गिर जाता है, उस दिन वो आगे बढ़कर पावोल का झंडा उठा लेती है कि वो भी जारशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। इस चीज ने मुझे ताकत दी कि लड़ाई लड़ी जा सकती है, बस मन में जो निजी सोच की गांठें बंधी रहती हैं, उनको खोलकर उससे आगे देखने की जरूरत है। इस तरह मैं अगर प्रभावित रही तो प्रेमचंद और गोर्की से।
सवाल – शायद 80 के दशक में आपकी एक कहानी आई थी ‘वाइफ स्वेपिंग’। क्या आपको नहीं लगता कि ये अपने समय से बहुत आगे याकि आज की कहानी थी? उस दौर में ऐसी कहानी लिखने का विचार कैसे आया?
चित्रा जी – खतरनाक था, उस दौर में ऐसी कहानी लिखना। भारतीय समाज में स्त्री के व्यक्तित्व व स्त्रीत्व को लेकर के जिस तरह की मर्यादाएं हैं और उन मर्यादाओं के साथ उन्हें अंकुशित व अनुशासित करती जिस तरह की परम्पराएं जुड़ी हुई हैं, उनके बीच किसी स्त्री का अपने पति के सिर पर हाथ रखकर कसम खाने की जुर्रत करना, वो भी मन में यह सोचते हुए कि ईश्वर मुझे माफ़ करना मैं झूठी कसम खा रही हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं। क्योंकि स्त्री के सतीत्व का प्रश्न एक निष्ठा का प्रश्न होता है, इसे हमारे दाम्पत्य जीवन की सफलता की पूँजी माना जाता है। ऐसे में यह कहानी लिखना जैसा कि मैंने कहा, खतरनाक था। मुद्गल जी ने तब सारिका का खेल विशेषांक निकाला था, जिसमें यह कहानी छपी। मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन बावजूद इसके मैंने कहा कि आप जैसे और लेखकों से पत्र भेजकर रचनाएं आमंत्रित करते हैं, वैसे ही मुझे भी पत्र भेजिए। मैं सोचती रही कि बचपन में मैंने खोखो से लेकर लॉन्ग रेस तक बहुत से खेल खेले थे, साइकलिंग में पुरस्कार भी जीते थे, लेकिन खेल को लेकर मेरे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था जिसपर मैं कहानी लिखती। अब अगर कोई कहानी मेरे अनुभव का हिस्सा नहीं है, तो मैं शोध करके रचना की सामग्री नहीं जुटा पाती। अतः मैं सोचती रही कि क्या करूँ। तभी एक देखा हुआ अनुभव याद आया। तिब्बत सीमा के पहाड़ी क्षेत्र में एकबार मैं गयी थी, वहीं मैंने यह देखा। सब लोग बीयर मग में अपनी गाड़ी की चाभियाँ डालते, फिर उस मग में हाथ डालकर जो चाभी हाथ में आए, उठा लेते। जो चाभी जिसके हाथ आती है, वो उस चाभी के मालिक की पत्नी के साथ संबंध बनाता है। वो पति कभी अपनी गाड़ी की चाभी नहीं डालता था, जिसे इस खेल में भाग लेना मंजूर नहीं था।
चूंकि ये जिस परिवेश का खेल था, मैं उसमें गयी हुई थी और मैंने देखा था कि उन लोगों को जिन कठिन परिस्थितियों में रहना होता है, उसमें अपने जीवन को रोमांचक बनाने के लिए वे अपने दाम्पत्य जीवन को भी दाँव पर लगाने को तैयार रहते । मुझे लगा कि इसमें स्त्रियों की मर्जी भी होती ही होगी, तभी उनका पुरुष अपनी गाड़ी की चाभी डालता है। अब कहानी उस अनुभव की बनती है कि खेल खेलने के बाद जब वे घर आते हैं, तो समाज के वही पारंपरिक नागरिक और पति-पत्नी होते हैं। सुरूर उतरने के बाद पुरुष का पूरा ध्यान अपनी पत्नी पर होता है कि तुम भी तो किसीके साथ गयी होगी। वो उससे तमाम सवाल पूछना शुरू करता है कि भीतर क्या-क्या किया और अंत में कहता है कि मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ, उसे लगता है कि मेरे सिर की झूठी कसम ये नहीं खा सकती। लेकिन पत्नी खाती है उसकी झूठी कसम। मेरी सोच इसमें ये थी कि सतीत्व वाले इस देश में जहां आज भी पत्नी पति की लम्बी उम्र के लिए तीज, करवाचौथ जैसे व्रत रखती है, उस देश में स्त्री अपने लिए गढ़ी गयी रूढ़ मर्यादाओं को तोड़कर आगे आ रही है। आपने प्रश्न में ठीक कहा, और भी कई लोगों ने कहा है कि ये बहुत आगे की कहानी है। ये विदेशों में संभव है, लेकिन भारतीय समाज में संभव नहीं है। सारिका के खेल विशेषांक में ये कहानी छपी और इसपर तीन अंकों तक चर्चा-विमर्श हुए। हालांकि मैं मानती हूँ कि यौनिक स्वतंत्रता से स्त्री को कोई स्वतंत्रता, स्वायत्तता नहीं मिल सकती क्योंकि उसकी काया के ऊपर एक अदद मस्तिष्क भी है। अतः पुरुष से बराबरी करनी है तो उसे मस्तिष्क से ही करनी होगी।
सवाल – जहां तक मेरी जानकारी है, आपका अधिकांश पालन-पोषण मुंबई में ही हुआ, इसलिये वहां के निम्नवर्ग का चित्रण तो आपकी कहानियों में समझ आता है। मगर ‘जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं’ जैसी कहानी लिखने की प्रेरणा कहां से मिली आपको?
चित्रा जी –‘जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं’ कहानी की प्रेरणा मुझे अपने गाँव, अपने घर, अपने खानदान से मिली। ये कहानी तब धर्मयुग में छपी थी। ‘जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं’ कहानी गाँव के लोगों का एक सपना है कि वे मंत्री हैं, तो गाँव के लिए जरूर कुछ करेंगे। गाँव में बदलाव लाएंगे। लोगों की उम्मीद है कि वे आएँगे तो भाषण देंगे और भाषण के साथ ही उनके वर्तमान व भविष्य को बदलने का सपना भी उन्हें थमाएंगे और उसको पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। कहानी में सुक्खन भौजी का एक विकलांग बेटा है, कांख में लकड़ी की बैशाखी के सहारे वो चलता है। फिर घोषणा होती है कि जगदम्बा बाबू आएँगे तो हड्डियों के डॉक्टर आएँगे और जहां-जहां कोई विकलांगता है, उसे देखेंगे और ह्वील चेयर बांटी जाएंगी। इस घोषणा से सुक्खन भौजी की उम्मीद खिलने लगती है, लेकिन अंत में लोगों की ऐसी उम्मीदों का क्या हश्र होता है, इसीकी ये कहानी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो कहानी में जगदम्बा बाबू आजादी के बाद की राजनीति का प्रतिनिधि चेहरा हैं, जिनसे लोगों को परिवर्तन की उम्मीद है। हालांकि ये उम्मीद खोखली साबित होती है। इस कहानी के छपने के बाद धर्मयुग को बहुत पत्र मिले लेकिन एक धमकी भरा पत्र मेरे घर से पहुँचा था। पत्र में कहा गया था कि घर की, खानदान की इज्जत तो ये अपने मन से एक ब्राह्मण लड़के से शादी करके पहले ही मिट्टी में मिला चुकी हैं, और अब घर की बातें कहानियों में लिख रही हैं, इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी अन्यथा हम मानहानि का दावा करेंगे। फिर भारती जी के कहने पर मैंने माफ़ी मांग ली ताकि धर्मयुग के ऊपर कोई आंच न आए।
सवाल – ‘आवां’ आपका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है (जिसमें शायद निजी अनुभव भी दिखाई देते हैं), जिसके लिए आपको पहला ‘अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान’ भी मिला। वहीं अभी ‘पोस्ट बॉक्स नं – 203 नाला सोपारा’ के लिए आपको साहित्य अकादमी मिला है। इन दोनों कृतियों में एक रचनाकार के तौर पर आपको अधिक संतुष्टि किस रचना से मिली?
चित्रा जी – ‘आवां’ के लिए के के बिड़ला का तेरहवां ‘व्यास सम्मान’ पाने वाली मैं पहली महिला हूँ। ‘आवां’ के लिए ही दो हजार की सहस्त्राब्दी का पहला इंदु शर्मा कथा सम्मान भी मिला। उसके लिए मैं लंदन गयी, जहां तेजेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी नैना व उनकी प्यारी बिटिया ने मुझे बड़े खुलूस के साथ रखा। निश्चय ही इस सम्मान से बहुत ख़ुशी हुई, लेकिन संतुष्टि का जहां तक प्रश्न है तो नेहरू सेंटर में मैंने यह सम्मान लेने के दौरान जो वक्तव्य दिया था, उसका जिक्र करना चाहूंगी। मैंने अपने उद्बोधन के अंत में कहा था कि – ‘कोई भी रचना लेखक लिखता है, लेकिन जबतक पाठक उसे अपने मानस पटल पर नहीं लिखता, तबतक वो अपना दाय नहीं प्राप्त कर पाती।’ ये बात मैंने गलत नहीं कही थी। बता दूं कि ‘आवां’ को मैंने पांच बार लिखा, पांच ड्राफ्ट किए, छठा ड्राफ्ट फाइनल हुआ, फिर तीन बार उसका फाइनल प्रूफ देखा लेकिन इतने के बाद भी आज जब मैं ‘आवां’ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे! मैंने पूरी मेहनत नहीं की, और मेहनत करनी चाहिए थी। लगता है कि मुझे जिस तरह के शब्द लिखने चाहिए थे, उनमें जिस तरह की अर्थछवियाँ खुलनी चाहिए थीं, नहीं खुल पाई हैं।
इसकी रचना-प्रक्रिया यूँ रही कि मजदूरों के लिए काम करते हुए उनके जीवन से जुड़े अनुभवों से मेरा जुड़ाव था, लेकिन नियोगी हत्याकांड जब हुआ तो इसने कई प्रश्न खड़े किए और यहीं मुझे लगा कि मुझे ‘आवां’ लिखना चाहिए। दो कहावतें मेरे दिमाग में थीं। पहली कहावत है – माँ की कोंख कुम्हार का आवां। ‘आवां’ नन्हे से पोखर की तरह एक गड्ढा होता है, उसमें लकड़ी के बुरादे, धान की भूसी आदि की लेयर बिछाई जाती है। उसके बीच में चाक पर बने खिलौने, बर्तन, सुराही बहुत सावधानी से रखे जाते हैं कि उनकी शैल्पिक बनावट में कोई खराबी न आए, क्योंकि पकाते वक़्त वो यदि टूट जाएं तो आवां का आवां खराब हो जाता है। माँ की कोंख में बच्चे के होने पर जैसी सावधानी रखी जाती है, वैसी ही इसमें मिट्टी की बनी चीजों को लेकर भी रखनी होती है। इसलिए इसे माँ की कोंख कहा गया है। दूसरी कहावत है- फलाने सिंह का आवां का आवां ख़राब हो गया यानी कि सबकुछ नष्ट हो जाना। अब ‘आवां’ उपन्यास में कोई कुम्हार और उसका आवां नहीं है, लेकिन इसमें आजादी के बाद समानता, स्वायत्तता, देश के विकास के सपनों का आवां है, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यानी आवां का आवां खराब हो गया। ‘आवां’ इन्हीं सब की कहानी कहता है, हालांकि ‘आवां’ के लिए मैं संतुष्टि की बात नहीं स्वीकार सकती।
इसी तरह ‘नाला सोपारा’ की बात करूँ तो इसे 2018 का साहित्य अकादमी मिला है। ये भी ‘आवां’ की तरह मेरे अनुभवों की ही दुनिया थी। उसमें मैं बतौर पात्र न होकर भी अपने अनुभवों के साथ जुड़ी हुई हूँ। नाला सोपारा मेरे अनुभवों से ही उपजा उपन्यास है। मैं भी ट्रांसजेंडर लोगों जिन्हें लोग हिजड़ा, छक्का आदि कहते हैं, से बाकी सबकी तरह ही घृणा करती थी। लोकल ट्रेनों में जब मैं इन्हें ताली बजाकर ध्यान आकृष्ट करते देखती थी तो मुझे लगता था कि कहाँ से ये आ गए। कभी यह जानने की कोशिश नहीं की थी कि आखिर जो ये काम वो जीवनयापन के लिए विवशता में कर रहे हैं, वो उनकी विवशता क्यों बनी? लेकिन जब मैं ट्रेन में एक ऐसे ही लड़के से टकराई जो कि मुंबई ही जा रहा था। खूबसूरत नौजवान था। बातों बातों में उसने बताया कि बोरीवली उतरकर लोकल पकड़कर नाला सोपारा जाऊंगा। वहां रात भर प्लेटफोर्म पर ही सोऊंगा और सुबह जब मेरी माँ घर से पूजा करने निकलेंगी तो थ्री ह्वीलर पकड़कर वे मुझसे मिलने चुपचाप स्टेशन आएंगी। मैंने कहा कि जब वहीं तुम्हारा घर है, माता-पिता हैं, तो तुम घर क्यों नहीं जाते? वो बोला कि घर जाने का निषेध है, मैं घर नहीं जा सकता। कोई आस-पड़ोस में भी नहीं जानता कि मैं उस घर का बच्चा हूँ। इसी घटना से प्रेरित होकर नाला सोपारा लिखा। जब इसे साहित्य अकादमी मिला तो मुझे उस लड़के बिन्नी की याद आई, बिन्नी आज नहीं है, लेकिन मैंने मन में कहा कि बिन्नी ये अवार्ड तुमको मिल रहा है। तुम जो जिन्दगी की तलाश में भटके जिंदगी भर, तुम्हे अपने घर की छत तक नसीब नहीं हुई, इसके लिए तुम्हारा अपना कोई गुनाह नहीं था। लेकिन अपनी उस बिरादरी जो एक गाली बन चुकी है समाज में, उसके साथ रहने को मजबूर थे। पढ़ना चाहते थे, लेकिन पढ़ नहीं पाए। तुम कम्प्यूटर सीखना चाहते थे, तुमने सीखना शुरू किया और कुछ ही दिनों में सीख लिया। यानी कि लिंग विकलांगता के बावजूद तुम्हारे धड़ पर जो एक मस्तिष्क था, वो बहुत तेज था। लेकिन उस लिंग विकलांगता के कारण तुम्हारे मस्तिष्क को भी धर्म, समाज द्वारा तड़ीपार कर दिया गया। धर्म, राजनीति, समाज और स्वयं मनुष्य इन चारों ने मिलकर मात्र एक लिंग विकलांगता के कारण मनुष्य की अपनी ही औलाद के साथ जो किया, वो भयानक था। तो जब नाला सोपारा को सम्मान मिला, तो अच्छा लगा, मन संतुष्ट हुआ या नहीं, मालूम नहीं।
मुझे लगता है कि लेखक अगर अपनी किसी कृति से संतुष्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। अगला उपन्यास ‘नकटौरा’ पूरा हो रहा है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट है, तो देखते हैं, शायद कहीं इससे संतुष्टि मिल जाए (हँसते हुए)।
सवाल – प्रवासी साहित्य को लेकर बहुधा भारतीय साहित्यकारों में एक उपेक्षा का भाव नजर आता है, जबकि इस साहित्य ने बहुत से अनूठे और अलग तरह के विषयों व रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आपकी इस विषय में क्या राय है?
चित्रा जी – नहीं! कोई उपेक्षा का भाव नहीं है। ऐसा उनका (प्रवासी लेखकों का) सोचना बहुत जल्दबाजी है। तेजेंद्र शर्मा, उषा राजे, दिव्या माथुर, सुषम बेदी आदि कई लेखक हैं, जिनकी खूब चर्चा हुई है और कई तो जगह-जगह पाठ्यक्रम में भी लगे हैं। किसीने मुझसे कहा कि जब आते हैं प्रवासी लेखक तो एक किताब के पांच शहरों में पांच लोकार्पण करवाते हैं। क्या यहाँ के लेखक के लिए ये सहज है? उसे ये सुविधा उपलब्ध है? तेजेंद्र शर्मा से लेकर तमाम प्रवासी लेखकों को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, आगरा हिंदी संस्थान के सम्मान मिले हैं।
ज्यादती तो यहाँ के भी बहुत से लेखकों के साथ हो जाती है। कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि जब बाकी लोगों की रचनाएं पाठ्यक्रमों में लगी हुई हैं, तो मेरी क्यों नहीं लग सकतीं? मैं तो किसीसे आग्रह नहीं कर सकती कि मेरी कहानी को लगाइए पाठ्यक्रम में। इन सब चीजों के विषय में नहीं सोचना चाहिए, बस लिखते रहना चाहिए। बहुत सी कमजोर रचनाएं पाठ्यक्रम में लगी हैं, तो जोड़-तोड़ भी होती ही होगी। हर क्षेत्र में हो रही है, यहाँ भी हो रही होगी। लेकिन प्रवासी लेखकों को लिखते रहना चाहिए। अपने समयकाल को जो लिखता है, वो कहीं न कहीं मूल्यांकित अवश्य होता है, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है।
सवाल – वर्तमान स्त्री-साहित्य में दो समस्याएँ नजर आती हैं। एक, स्त्री-स्वतंत्रता के नामपर स्वच्छंदता की पैरवी और दूसरा, पुरुष-विरोध। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा है?
चित्रा जी – पितृसत्ता ने रूढ़ दृष्टिकोण स्त्री के साथ सदियों से अपनाया है। लेकिन अब जब स्त्री शिक्षित हुई है, आत्मनिर्भर हुई है और अपने बारे में उसने सोचना शुरू किया है, तब भी उसके प्रति लोग जो रूढ़ विचार रखते थे, उससे पूरी तरह से समाज मुक्त नहीं हो सका है। आज जब एक पढ़ी-लिखी राह चलती लड़की से लेकर नन्ही बच्ची तक के साथ बर्बरता होती है, तो इससे मालूम होता है कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या अब भी है। सोचा जाता है कि लड़की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगी तो समाज में उसकी अपनी आवाज होगी, लेकिन नहीं है। इसलिए पितृसत्ता के खिलाफ स्त्री की चेतना और उस चेतना को स्वर देना स्त्रियों द्वारा लेखन में भी शुरू किया गया।
लेकिन इसमें कुछ अतिवाद भी नजर आ रहे हैं। स्त्री को पुरुषों से घृणा नहीं करनी है, क्योंकि पुरुष तो उसका पुत्र, पिता, भाई पति भी है। इन्हें एक स्त्री ही जन्म देती है, पुरुष पुरुष को जन्म नहीं दे सकता। पितृसत्ता ने जो ज्यादतियां की हैं, उसके खिलाफ आक्रोश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, लेकिन घृणा नहीं होनी चाहिए। स्त्री को बेटी-बेटे में विषमता भाव छोड़ पुत्र को भी समझाना चाहिए कि तुम्हारी बहन के सिवा बाहर की युवती-नवयुवती भी समाज की एक स्वतंत्र इकाई है, अतः उसे सिर्फ मादा के रूप में मत देखो, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में देखो। लेकिन पुरुष के प्रति जो प्रतिशोध की भावना आ रही है कि पुरुष नहीं चाहिए, फांसी दे दो, वो गलत है। ये निदान नहीं है।
इसका परिष्कार मेरी नजर में बस एक ही है कि पहले स्त्री स्वयं सोचना शुरू करे कि उसके धड़ के नीचे जो योनी है, वही सबकुछ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो एक अदद मस्तिष्क है, वह सबकुछ है। अपने बेटे को सिखाए, अनुशासित बनाए, उसमें ऐसे नैतिक मूल्य भरे कि वो घर के बाहर जो स्त्री नजर आती है, उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखे। इसी तरह अगर बेटी है तो उसे भी लड़कों की इज्जत करना सिखाए ताकि वो उनके प्रति घृणा न पाले। लेकिन आज तो एक फार्मूला बना लिया है लेखन में। स्त्री-विमर्श तो चल रहा है, उसके साथ-साथ पुरुष से प्रतिशोध-विमर्श भी चल रहा है। पुरुष के बिना तो समाज संभव नहीं है। आप लेस्बियन समाज बना लें, इससे क्या होता है, ये तो एक तरह से परवर्जन है। अतः मुझे लगता है कि साहित्य में स्त्री-विमर्श को लेकर एक विवेकपूर्ण सोच पैदा होनी चाहिए और पैदा हो भी रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन इस विषय में अति तो कुछ संपादकों ने की कि स्त्री को कहा कि तुम स्वयं अपने कपड़े उतारकर खड़ी हो जाओ सड़क पर। ज्यादा क्या कहूँ, मेरा तो एक उपन्यास ‘एक जमीन अपनी’ इसीपर है।
सवाल – लोकसभा चुनाव से पूर्व नरेंद्र मोदी के समर्थन को लेकर आपका साहित्यिक समाज में एक ख़ास गुट द्वारा बड़ा विरोध किया गया। एक तरह से साहित्यिक समाज में आपके बहिष्कार का अभियान चलाने की कोशिश हुई। लेकिन अब मोदी पुनः विशाल बहुमत से विजयी होकर सत्ता में हैं, तो अब इस पूरे प्रकरण पर, उन विरोधियों के लिए, कुछ कहना चाहेंगी?
चित्रा जी – मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि विचारधारा को जब भी रूढ़ बना लेता है कोई भी लेखक, तो वो विचारधारा के विवेक को खो देता है। मुझे लगता है कि मोदी जी के संदर्भ में हमारे बहुत-से प्रगतिशील लेखकों ने समझने में यह गलती की। बस इतना ही कहना चाहूंगी।
सवाल – आपके बहिष्कार का जो अभियान चला, उसपर कुछ नहीं कहेंगी?
चित्रा जी – बहिष्कार का जो अभियान चला, उसे चलाने वाले अपने आप चुप हो गए। मैंने गलत का समर्थन नहीं किया। मैंने तो देश के विकास, अखंडता, भ्रष्टाचार के विरोध का समर्थन किया। मैंने ‘आवां’ लिखा है जिसका सार है कि आजादी के बाद के सत्तर साल में देश का आवां का आवां खराब हो गया। तो इस आवां को ठीक करना पड़ेगा न! उस आवां को ठीक करने का जिम्मा अगर मोदी जी ने उठाया है तो वे किसी पूंजीपति का सपना लेकर नहीं बैठे हुए हैं न!
किसी भी विचारधारा में अगर कुछ गलत रूढ़ चीजें हैं, तो बहुत धैर्य से उन्हें दूर करने की जरूरत होती है, जिसमें बुद्धिजीवियों की तो बहुत बड़ी, सचेतक की भूमिका होती है। उस भूमिका को छोड़कर आप तो कहेंगे कि ये पेड़ नहीं चाहिए, इसे जड़ से काटकर फेंक दीजिये। लेकिन ये तो कोई निदान नहीं है। समय दीजिये, देखिये, परिवर्तन की आंधी को कोई रोक नहीं सकता है।
सवाल – आप विश्व हिंदी सम्मेलनों से एक लम्बे अर्से से जुड़ी हैं। इसके आयोजनों में आपकी सक्रियता रहती है। हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में इस सम्मेलन को आप कितना सफल देखती हैं?
चित्रा जी – बहुत बुराई करते हैं लोग! इसको मेले-ठेले के नाम से पुकारते हैं। इसकी कोई भूमिका नहीं है, यह भी कहते हैं। फिर भी उत्सुक होते हैं कि किसी प्रकार उन्हें विश्व हिंदी सम्मेलन में जाने का अवसर मिले। ये बहुत गलत आचरण है, क्योंकि हिंदी सम्मेलन में केवल वही लोग नहीं आते जो इसकी आलोचना करते हैं बल्कि वो लोग भी आते हैं जो देश-विदेश में इसके पठन-पाठन को विस्तार दे रहे हैं। वो लोग भी अपनी कठिनाइयों और आवश्यकताओं की जानकारी देते हैं। ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आपसी संवाद की संभावनाओं को विकसित करता है। हाँ, जो लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं, वो तो अपने सत्र में उपस्थिति दर्ज करके चले जाते हैं, वे विदेशी विद्वानों से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। और विश्व हिंदी सम्मेलनों की जो परिणितियां सामने हैं, वो बहुत अच्छी हैं।
सरकार जो करोड़ों रुपये खर्च करती है, उसका मकसद यह भी है कि भारत के बाहर जो भारतवंशी हैं, जो हिंदी के प्रवासी लेखक हैं, वे सब भी एकजुट हों। एकदूसरे से मिले-जुलें और उनको भी ये अहसास हो कि हिंदी भाषा के बहाने उनका भारत देश उनके संपर्क में है। इस सम्मेलन के विषय में मेले का भाव तो वही रखते हैं, जो सोचते हैं कि विदेश जाने का अवसर मिला है, हम दूसरों के सत्रों को सुनेंगे नहीं, घूमेंगे। हम तो खोजते हैं कि उषा राजे से कैसे मुलाक़ात हो, तेजेंद्र शर्मा से कहाँ मुलाक़ात हो।
विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी के प्रसार में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसके पीछे एक अहम कूटनीतिक बात भी नजर आती है कि जिन देशों में भारतवंशी हैं, उन देशों में इन सम्मेलनों का आगाज अधिक होता है। इसी बहाने सरकार वहां उन लोगों तक पहुँचती है और उन सब लोगों को प्रेरित करती है एक होने के लिए कि जहां जिस देश में भी रहें, भले वहाँ के नागरिक हों, लेकिन ये कभी न भूलें कि वे मूलतः भारतवंशी हैं।
सवाल – हिंदी साहित्य पर एक समय के बाद से एक ख़ास विचारधारा का प्रभाव रहा है। इस कारण हिंदी साहित्य को क्या हानि-लाभ आप देखती हैं?
चित्रा जी – प्रगतिशील विचारधारा के संदर्भ में ये बात की जाती है। निश्चय ही इस विचारधारा को मानकर जो लोग चले उनका लेखन एक प्रतिबद्ध रूप से हुआ। उनके लेखन से समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों के दमन-शोषण को लेकर साहित्य में जो कमी थी, वो कमी पूरी हुई। अतः हम यह नहीं कह सकते कि साहित्य में विचारधारा ने नुकसान किया। मार्क्स ने हमें प्रेरित किया कि मजदूर वर्ग के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। मैं स्वयं ट्रेड यूनियन से जुड़ी रही हूँ और उस सोच की पैरवी के लिए हमेशा सन्नद्ध रही हूँ। लेकिन अगर दूसरी विचारधारा के लोगों को यह विचारधारा अपना शत्रु समझती है, हेय समझती है और समझती है कि इनका लिखा गया साहित्य कूड़ा है, इनके साहित्य में आम जन की बात नहीं है, तो ये गलत है। अन्य विचारधारा के साहित्य में जिस जन, चाहें वो किसी भी वर्ग-जाति या समुदाय का हो, की बात होती है, उसकी भी तो बात होनी चाहिए। ये जो शत्रु समझने और गोलबंदी करके उसपर सत्ताधीशी करने वाली बात है, यह ठीक नहीं है।
हिंदी साहित्य में इस वाम विचारधारा ने जिस तरह अमृतलाल नागर को अलग किया, भगवती चरण वर्मा को अलग किया, नरेश मेहता को अलग किया, ये गलत है। मुझसे एकबार जिक्र किया था बाबूजी (अमृतलाल नागर जी) ने कि – “जानती हो बहू, मेरे ऊपर जेएनयू में नामवर ने पीएचडी नहीं होने दी।” पाठ्यक्रमों में किनको होना चाहिए, ये तक ये लोग तय करते रहे। अब भी वही हो रहा है और अंदर बैठे लोग उन गलत चीजों को प्रश्रय दिए हुए हैं। कहने का अर्थ है कि एक दुराग्रही आचरण इन लोगों (वाम विचारधारा) ने किया है, जो कि गलत है।
हर विचारधारा के प्लस पॉइंट भी होते हैं और माइनस पॉइंट भी होते हैं। माइनस पॉइंट तब होते हैं, जब उस विचारधारा के लोग शासक बनने की चेष्टा करने लगते हैं। ये गलत है और इन लोगों ने ये किया। दलबंदी बनाकर इन्होने तमाम बड़े लेखकों को किनारे किया। ये भूल गए कि हिंदी साहित्य केवल इनके लेखन के लिए ही नहीं जाना जाएगा, वरन अपने सम्पूर्ण वैविध्य और समग्र समाज की आवाज के रूप में जाना जाएगा। हर तरह के नए विचारों का स्वागत करना चाहिए। अतः मैं मानती हूँ कि सामाजिक हाशिये के लोगों की परिस्थितियों को साहित्य में उठाना महत्वपूर्ण है, लेकिन वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जो शेष समाज के राग-द्वेष, उनके भावनात्मक द्वंद्व, प्रेम को उठाते हैं। कोई भी विचारधारा जब दुराग्रह के पाले में जाकर खड़े हो जाती है और दूसरी विचारधारा के लोगों को अपना शत्रु समझने लगती है, तो उसपर मुझे लज्जा आती है।
सवाल – आपके आज के प्रिय लेखक/लेखिका?
चित्रा जी – मुझे मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी ‘स्वांग’ बहुत अच्छी लगती है। तेजेंद्र शर्मा की ‘ढिबरी टाईट’ अच्छी लगती है। इसी तरह दिव्या माथुर की ‘पंगा’, अल्पना मिश्रा की ‘छावनी में बेघर’, गीताश्री की कहानी ‘मेकिंग ऑफ़ बबिता सोलंकी’ आदि बहुत सी रचनाओं के नाम गिनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन कहानियों का नाम ले रही हूँ तो इसका अर्थ है कि नयी पीढ़ी जब बहुत अच्छा लिखती है और हम उसको पढ़ते हैं, तो एक आश्वस्ति होती है कि बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। पिछले दिनों सूर्यनाथ सिंह का उपन्यास ‘नींद क्यों रात भर नहीं आती’ बहुत अच्छा लगा। प्रवासी साहित्य में उषा वर्मा की एक कहानी है नस्लभेद को लेकर, वो भी बड़ी अच्छी लगी। तो बहुत-से लोग हैं, किन-किनका नाम लूं।
सवाल – नए लेखक/लेखिकाओं के लिए कोई सन्देश?
चित्रा जी – संदेश क्या दूं, मैं खुद आजकल एक बेहतर संदेश की तलाश में हूँ जिसे पढ़कर मैं प्रेरित होऊं। प्रेमचंद के उस संदेश की तरह कि साहित्य, राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। ऐसे सन्देश प्रेरित करते हैं, आपकी इच्छाशक्ति को मजबूत बनाते हैं, आपकी विचलनों को कहीं न कहीं संवारते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं अभी किसी प्रकार का सन्देश देने के लायक नहीं हूँ, लेकिन इतना कहूँगी कि नयी पीढ़ी अपने समयकाल के संक्रमणों को अपनी चेतना की दृष्टि से मैग्नीफाईंग ग्लास लगाकर तटस्थ होकर देखे और उसके बारे में सोचे, फिर लिखे।
पीयूष – हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चित्रा जी – धन्यवाद!


