
रूपा सिंह हिन्दी जगत का एक ऐसा नाम है जिसे आप नकार नहीं सकते हैं। या तो आप सीधे सीधे उनसे जुड़ जाते हैं या फिर उनके लिये मन में नकारात्मक भाव बना बैठते हैं। वैसे राजेन्द्र यादव के बारे में भी कहा जाता था “Either you love him or you hate him. You can’t ignore him.” मगर रूपा सिंह को जैसे इस सब से कोई सरोकार नहीं है। वह अपनी धुन में अपनी राह चलती रहती हैं। वैसे उनका प्रिय क्षेत्र आलोचना का है, मगर जब कविता उतरती है तो कविता लिख लेती हैं और जब “दुखाँ दी कटोरी : सुखाँ दा छल्ला” जैसी कहानी लिख देती हैं तो फ़ेसबुक पर तहलका मचा देती हैं। उनका व्यक्तित्व बिंदास है… अपने में मस्त। रूपा सिंह से उनकी रचनाओं, रचना-प्रक्रिया एवं स्त्री-विमर्श आदि विषयों को लेकर पुरवाई की प्रतिनिधि नीलिमा शर्मा की बातचीत की। लीजिये आपके लिये भी पेश हैं नीलिमा जी के प्रश्न और रूपा सिंह के खरे-खरे उत्तर।
प्रश्नः रूपा जी आपकी शख़्सियत ऐसी है कि हिन्दी साहित्य से जुड़े हर व्यक्ति को लगता है कि जैसे वह आपको जानता है। दिल्ली आपको अपना समझती है और अलवर अपना। यह दिल्ली और अलवर की जो दो रूपा सिंह हैं, उन्हें समझना हो तो उनके बारे में क्या कुछ जानना ज़रूरी है?
उत्तरः सुन्दर प्रश्न! कितनी अद्भुत बात कही है आपने कि हिन्दी साहित्य से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति मुझे जानता है। हिन्दी के एक आदमी की हिन्दी जानती समझती हूं तो यह मेरे लिये गौरव की बात है। मेरे पाठक जानते हैं कि मेरा जन्म स्थान दरभंगा बिहार है और बचपन के दिन विद्वान कवि नागार्जुन की छत्रछाया में बीते हैं। आपने दिल्ली की बात कही है जहां 1993 से मैं दरभंगा छोड़कर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की दुनिया में दाख़िला लिया और तब से दिल्ली मेरी नगरी बन गयी। मेरा घर, द्वारा, बाल-बच्चे, दोस्तों, साहित्य, नाटकों और व्यवस्थित समृद्ध पुस्तकालयों की दुनिया।
दिल्ली राजनीति और साहित्य का प्रमुख केन्द्र है। लेकिन जिस दरभंगा और अलवर (राजस्थान) से मेरे जीवन का गहरा तादात्म्य रहा वह दूर तक प्रभावित करने वाला भी हुआ। जैसे दरभंगा बंगद्वार था तो अलवर को राजस्थान का सिंहद्वार माना गया।
दरभंगा के लोहिया सराय, जहां मेरा जन्म हुआ था, ‘बालक’ पत्रिका का संपादन आरंभ हुआ था जिसे रामवृक्ष बेनीपुरी जी और शिवपूजन सहाय जी ने मिलकर शुरू किया था। वहां ‘पुस्तक भण्डार’ जैसा नामी पुस्तक केन्द्र था। मंडन मिश्र और भामती जैसे प्रकांड विद्वान हुए जिनके बारे में किंवदन्ती प्रचलित है कि उनका तोता भी संस्कृत बोलता था। हमारे विद्यापति, जिनकी सेवा में साक्षात शिव उगना बनकर आठों पहर खड़े रहते। ऐसी बहुत सी महिमा है हमारे दरभंगा की… शायद आपको मालूम न हो कि काशी नागरी प्रचारिणी की स्थापना होने लगी तो दरभंगा नरेश ने आर्थिक सहयोग दिया था। दरभंगा महाराज ने मदन मोहन मालवीय जी को भी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये लाखों रुपये की आर्थिक सहायता दी थी।
प्रश्नः और फिर अलवर…
उत्तरः हाँ, अब अलवर के बारे में जानिये कि अलवर नरेश ने शुक्ल जी को बुलाया था। शुक्ल जी यहां आये और रहे थे। कुछ दिनों पश्चात वे वापिस गये। अलवर प्राचीन इमारतों, राजसी किले, और महारानी की छतरियों के लिये तो मशहूर है ही, सरिस्का महल और सफ़ेद बाघ परियोजनाओं के लिये भी जाना जाता है। लेकिन मुझे सबसे अधिक मोहता है यह अलवर से जुड़ाव का कारण। देवताओं की यह नगरी के चप्पे-चप्पे मुझे दरभंगा के छुट गये विद्यापति के संयोग श्रृंगार और नचारी पदों की याद तो दिलाते ही हैं, आगे की यात्रा की अनासक्त उड़ान को भी प्रेरित करते हैं। भर्तृहरि के तीनों शतक – शतकत्रयी (श्रृंगार, नीति और वैराग्य) तक की यह यात्रा अद्भुत है, जिसमें दिल्ली एक ऐसा ठौर है जो मुझे वापिस अपनी भौतिक दुनिया से ला जोड़ता है। यहां सब रूपा सिंह को पहचानते हैं लेकिन यह पहचान स्वयं रूपा ने दरभंगा और अलवर की उन्नत और प्रखर भूमि से ग्रहण की है।
प्रश्न: रूपा जी, पहले एक कहावत मशहूर थी कि पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने के लिये पहली शर्त होती थी लेखक का न रहना। यानि कि जीवित लेखक पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते थे। अब साहित्य को लेकर नयी शुरूआत हुई कि बहुत से विश्वविद्यालयों ने जीवित साहित्यकारों की रचनाओं को पाठ्यक्रम में जोड़ा। विश्वविद्यालयों में जो कहानियाँ पाठ्यक्रम में लगाई जाती हैं, उनके चयन का मानदण्ड क्या रहता है?
उत्तरः प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं कहूंगी कि भई मेरी समझ में इसका कोई विशेष तात्पर्य नहीं है। रचना को हमें चुनना है या रचनाकार को? क्या आपके कहने का तात्पर्य यह लिया जाए कि मृत रचनाकार महान हो जाते हैं? या महान रचनाकार अल्पायु होते हैं या फिर रचनाकार के जीवित या मृत होने से रचनाओं की उत्कृष्ठता के मापदण्ड की कोई इकाई तय होती है?… नहीं ना?
देखिये मुझे लगता है कि यह फ़िज़ूल बात है। रचना का मूल्यांकन इन थोथी बातों से नहीं किया जाना चाहिये। हाँ, इसमें इक बात अवश्य सिद्ध होती है – वह है रचना परिपक्वता। नये-नये रचनाकार लिख कर ही परिपक्व होते हैं और रचनाएं भी क्रमशः व्यक्ति से समष्टिगत होती जाती हैं। लेकिन फिर भी यह कोई नियम या फ़ॉर्मूला नहीं है कि किसी रचना को हम इसलिये नकार देंगे कि उसका रचनाकार अभी जीवित है।
आपके प्रश्न के दूसरे अंश से गन्ध आती है इस बात की, कि कहीं रचनाकार पाठ्यक्रम में अपनी रचनाएं लगवाने के लिये अपनी राजनीतिक पैठ या रसूख़ का प्रयोग भी करता है? तो यह तो जगजाहिर बात है। इसमें संदेह की गुंजाइश क्या? हालांकि पाठ्यक्रमों में रचनाओं का चुनाव, रचनाओं के अंतर्पाठ की सोद्देश्यता को ध्यान में रखते हुए उसे पढ़ने और पढ़ाने योग्य छात्रों के भविष्य निर्माण को देखकर किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्धारण पैनल में सावधानीपूर्वक चुनाव इस ओर संकेत भी करता है, जिसके अनेक मुद्दों में राष्ट्र-निर्माण की भावना के अतिरिक्त सही ब्यौरों का दिया जाना भी एक कसौटी है। आपके संकेत मैं समझ रही हूं और यह संकोच के साथ कहती हूं कि इसमें पूरी कोशिश की जाती है कि रसूख़दार हस्तक्षेप कर अपनी कृतियों का चयन करा सकें। कई बार यह संभव नहीं भी होता है। चयन-प्रक्रिया, चाहे कोई भी इसे गुप्त रखने का यथासंभव प्रयास हम सबका दायित्व है।
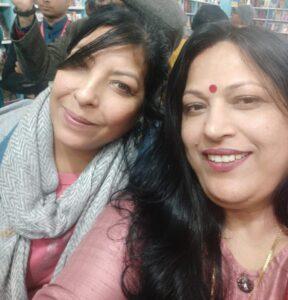







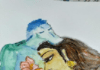
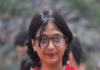

रूपसिंह का साक्षात्कार सराहनीय है।
रूपा सिंह ने जितनी सहजता और स्पष्टता से उत्तर दिए, वह शानदार है। अमूमन ऐसा होता नहीं। अच्छा साक्षात्कार है। प्रश्न भी अच्छे किए गए।
राजा अवस्थी, कटनी