नवीन कृषि बिल को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड व बारिश में भी किसान डटे हुए हैं। इस आंदोलन को हर क्षेत्र से समर्थन मिल रहा है। बॉलीवुड भी उन्हीं में से एक है। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो यहां ऐसी कई फिल्मों का निर्माण हो चुका है जो किसानों के दर्द को बयां करती हैं।
अनाज दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। इस अनाज के लिए ही तो तमाम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दुनिया जिस पैसे के पीछे भागती फिर रही, अनाज उस पैसे से भी कीमती है। जब अनाज इतना कीमती है तो इसे उपजाने वाला किसान कितना कीमती होगा! लेकिन अफसोस कि किसान की हालत साल दर साल खराब ही होती गई है। किसानों के संघर्ष को सिनेमा ने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। किसानों पर कई ऐसी फिल्में बनी हैं। जिन्हें देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि एक किसान के सामने कितनी चुनौतियां होती हैं।

दो बीघा जमीन (1953)
भारतीय किसान के वास्तविक दर्द को पर्दे पर उकेरने वाली फिल्म थी। बिमल रॉय की दो बीघा जमीन हृदय-स्पर्शी और परिष्कृत रूप से एक बेदखल किसान का जीवंत चित्रण है। एक किसान केo नज़रिए से देखा जाए, तो फिल्म भारतीय किसान समाज का बड़ा ही मानवीय चित्रण प्रस्तुत करती है। इस फिल्म में न सिर्फ सार्वकालिक उपेक्षितों की, बल्कि शोषितों की भी पीड़ा है। अपनी आंतरिक श्रेष्ठता, नेकनियती के ही कारण यह वंचित वर्ग का गहरा दर्द प्रस्तुत कर सकी थी।
किसान के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी ज़मीन होती है। ज़मीन उसके लिए मात्र एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि महान विरासत होती है। सोचिए जब वही ज़मीन किसान से छीन ली जाए, उसे दाने-दाने को तरसाया जाए तब उसे कैसा दर्द होगा। इसी पीड़ा का गहन चित्रण इस फिल्म के केंद्र में है। भारतीय परिवेश में कैसे कोई किसान कर्ज के जाल में फंसता है। कर्ज़ की भरपाई के लिए उस किसान का तिनका तिनका बिखर जाता है।
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसका पलायन व किसान से मजदूर बनने की कहानी को बखूबी पेश किया गया। दो बीघा ज़मीन विकास की भेंट चढ़ रही ज़मीनों की ओर संकेत करती है। फिल्म का मुख्य पात्र शम्भू एक गांव में दो बीघा जमीन का मालिक है। पत्नी, बेटे व पिता के साथ उसका सुखी परिवार है। गांव में अकाल के बाद हुई बारिश से सब खुश हैं।
गांव के जमींदार की नज़र शम्भू की ज़मीन पर है। जमींदार वहां कारखाना लगाना चाहता है। जब जमींदार कर्ज़ के बदले शंभू की जमीन लेने की बात करता है। जमींदार का कर्ज़ चुकाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन जमींदार का हिसाब कुछ और ही होता है। शम्भू अन्याय के विरुद्ध अदालत जाता है। फिल्म में न्याय व्यवस्था की सच्चाई भी उस समय उजागर हो जाती है जब शम्भू मुकदमा हार जाता है।
हीरा मोती (1959)
मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा पर आधारित व बलराज साहनी अभिनीत कृष्ण चोपड़ा की फिल्म ‘हीरा मोती’ साहित्य में किसान के रूपांतरण के नज़रिए से महत्वपूर्ण थी। बलराज साहनी हिंदी सिनेमा की एक अविस्मरणीय शख्सियत रहे हैं।
अभिनय में आज भी बलराज को बड़ा आदर्श माना जाता है। बलराज साहब लीक से हटकर काम करने के लिए जाने जाते थे। वह एक जुझारू एवं समर्पित कलाकार थे। बलराज साहनी और प्रेमचंद के सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्ष में वैचारिक आदर्शों की एक समानता समझ आती है। उसके माध्यम से एक साझा संवेदना को स्पर्श किया जा सकता है।
इन दो शख्सियतों में जो कुछ साझा था, कह सकते हैं कि उसका एक अंश इस फिल्म के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ। प्रगतिशील आंदोलन ने संस्कृति कर्म से जुड़े लोगों को साझा मंच दिया था। इस अभियान में प्रेमचंद व बलराज साहनी की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। प्रेमचंद का व्यक्तित्व इस क्रांतिकारी अभियान में प्रेरणा का स्रोत था। उधर सिनेमा के स्तर पर विचारधारा समर्थन में बलराज दलित-शोषित-वंचित किरदारों को जीवंत कर रहे थे। एक तरह से इन पात्रों को जीवंत करके इनकी तकलीफों को भी साझा कर रहे थे। उन्होंने संस्कृति कर्म को सहयोग का माध्यम बनाया। ग्रामीण पात्रों को निभाना कठिन होता है।
नगरीय पात्रों की परतें उसे विशेष रूप अवश्य देती हैं लेकिन, देसज पात्रों की बात जुदा है। इस मिज़ाज के पात्रों को बलराज ने अनेक बार जीवंत किया। अपनी मिट्टी के होने की वजह से गांव के किरदारों में अपार आकर्षण है। सिनेमा ने इन्हें बड़ी पारी नहीं दी। कह सकते हैं कि पॉपुलर सिनेमा में नगरीय कहानी व पात्रों को तरजीह मिली। फिर भी कम समय में ही ग्रामीण पात्र स्मरणीय बनकर उभरे। इन किरदारों का वक्त आज भी याद किया जा सकता है।

मदर इंडिया (1957)
मशहूर फिल्ममेकर महबूब ख़ान की ‘मदर इंडिया ‘ गरीबी से पीड़ित राधा की कहानी है जो कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। वो शोषण के शिखर रूपी महाजन से स्वयं को बचाने का संघर्ष कर रही है। मदर इंडिया मेहबूब खान की ही फिल्म ‘औरत’ का एक्सटेंशन थी। मदर इंडिया का शुमार भारतीय सिनेमा के माइलस्टोन फिल्मों में होता है ।
फिल्म की शुरुआत वर्तमान काल में गांव के लिए पानी की नहर के पूरा होने से होती है। गांव की मां राधा नहर का उद्घाटन कर रही है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब वो एक नई दुल्हन थी। विवाह का खर्चा राधा की सास ने सुखीलाला से कर्ज लेकर पूरा किया था। इसी कारण वो गरीबी व शोषण के कभी न खत्म होने वाले चक्रव्यूह में फंस जाती है। कर्ज़ की शर्तें विवादास्पद थीं ।
परन्तु फैसला सुखीलाला के तरफ सुनाया जाता है। शामू और राधा को अपनी फसल का एक तिहाई हिस्सा सुखीलाला को ब्याज़ के तौर पर देना होगा। इस चक्रव्यूह से निकलने की शामू कोशिश करता है। मगर असफल हो जाने पर सब कुछ छोड़ कर हमेशा के लिए कहीं चला जाता है। जल्द ही राधा की सास भी गुज़र जाती है। राधा अपने दोनों बेटों के साथ खेतों में काम करना जारी रखती है।
अपना संघर्ष जारी रखती है। उसे कर्ज़ के चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए सुखीलाला उसके सामने शादी का कपटी प्रस्ताव रखता है। राधा खुद को बेचने से इंकार कर देती है। गांव के तूफान की चपेट में आने से राधा एवं उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। गांव की सारी फसल नष्ट हो जाती है। पूरा गांव पलायन करने लगता है। लेकिन राधा के मनाने पर सभी वहीं रुककर हालात से संघर्ष करते हैं।








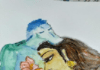


सैयद एस तौहीद ने किसानों के संघर्ष पर बनी फिल्मों का उम्दा जिक्र ,किया है ,ये फ़िल्म तो जब बनी थीं तब भी ग्रामीण
अंचल के कृषकों तक नहीं पहुँची, आज टेलीविजन के माध्यम से
देख रहे होंगें ।सारे फिल्म मेकर्स को कृषकों पर बनी फ़िल्म से कमाए पैसे का आधा ग्रामीण इलाकों के आर्थिक विकास पर लगाना था ।कृषकों को शिक्षित करने के उपायों पर भी सोचना था ।
प्रभा