जब भी लाल, पीला, गुलाबी, श्वेत गुलाब उसके वाॅल पर खिल उठता, अंकित चिढ़ जाता।
“इतने कठिन समय में भी तुम्हें पोस्ट करने की पड़ी है? लोगों को कितना बुरा लगता होगा, नहीं सोचती तुम? “
“क्यों… क्यों बुरा लगेगा भला?”
“इतना तकलीफ़देह है सब कुछ, इसीलिए।”
“और मैं इसी समय की मार के दंश से बचाने के लिए…। “
“…बस, जवाब हाजिर। सवाल के आने भर की देर है कि…”
“…हीऽऽ!…हीऽऽ!”
“ओह! कुछ कहो तो हँसी में उड़ा दोगी। समय की नजाकत को समझना ही नहीं है।”
“नहीं। वैसी बात नहीं। समझती हूँ, तभी तो गुलाब की…।”
“कहाँ समझती हो, कितने लोग हताश, निराश हैं। कितनों ने अपनों को खो दिया है।”
“हाँ, न जाने कितनों के इस महामारी में सर्वस्व लुट गए। मैं उनमें सुकून भरना चाहती हूँ अंकित।”
“ऐसे में तुम्हारे गुलाब देखेगा कौन?”
“जिन्होंने खोया शायद वे अभी एफबी पर सक्रिय न हों लेकिन हताश-निराश, बेचैन, अवसादग्रस्त लोग देखेंगे तो…” “…तो नाचने लगेंगे? यहाँ लोगों को बचाने-बचने की छटपटाहट कम नहीं हो रही है और…।”
अंकित की चिढ़ सदा ऐसे वाक्य में ढल जाती।
“मेरे गुलाब बच गए लोगों में उम्मीद भरेंगे। उन्हें जीने का हौसला देंगे। मुस्कराहट की वजह बनेंगे अंकित।”
बंद कमरे की बंद हवाओं में घुलती तल्खी को दरकिनार करती शुचि अपने मोबाइल सहित बेड रूम से बाहर आ गई। बाहर भी पाबंदियोंं की साँकलें थीं। दरवाजा नहीं खोलना है। खिड़कियाँ भी बंद रखनी हैं। बालकनी में बैठने की जरूरत नहीं। बल्कि उधर का द्वार भी नहीं खोलना है। जैसे हवा को भी कैद कर लिया जाएगा।
“हवा में घुल गया है वायरस का जहर।” – चहुँ ओर यह भी अफवाह थी।
बहुत जिम्मेदार होने के बावजूद ए सी की हवा कितनी जिम्मेदारी निभा सकती थी। यूँ शुचि को वह रुचती नहीं। कार में भी बाहर की हवा की मुरीद शुचि जब-तब विंडो खोल ही लेती। उसे लगता, हर जगह की हवा की खुशबू अलग, मीठी सी सिहरन-छुअन अलग, एहसास अलग तो क्यों न उनका आन्नद ले।
दोनों अपने-अपने काम में व्यस्त हो गए। अंकित सदा की तरह न्यूज चैनल के बिहड़ों में खोने लगा। इन चौबीस घंटे की न्यूजवाली बकबक और बकझक, कुतर्कों से चिढ़ने के बावजूद वह कभी-कभार अंकित का साथ देती ही देती है। थोड़ी देर बाद वह भी सोफे पर बिराजमान हो, न्यूज में खो गई। कब शुचि की आँखें भींगीं, कब आँसू बाहर आए, कब अविरल बहने लगे, उसे एहसास ही नहीं हुआ। अंकित गौर से उसकी ओर देखने लगा। यह तो शुचि का चरित्र नहीं। वह दोनों हथेलियों से गालों को पोंछें जा रही थी।
“बंद कर दो।…बंद कर दो। अब मैं और नहीं देख सकती।”
“अरे! इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है शुचि।”
“ये कुछ और नहीं दिखा सकते, जैसे उपाय, बचाव सावधान करने की…? केवल मौत की खबरें…केवल हताशा परोस रहे हैं।”
“कोविड का इतना बड़ा अटैक फिर हुआ है। लोग समझ ही नहीं रहे तो बताना इनकी जिम्मेदारी है।”
शुचि ने पहलू बदला। उसे वह काली छाया वाला पहला वर्ष भी याद आया, जब अनायास एक अदृश्य बीमारी की चपेट में पूरा संसार मौत की आगोश में जा रहा था। एक अदना से वायरस ने सारे संसार को उसकी औकात दिखा दी थी। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या निर्धन, क्या अति संपन्न, क्या विकसित और क्या विकासशील देश सभी के सभी उस अदृश्य कोरोना वायरस के आगे बेबस हो चुके थे। उसकी लहर में कितने घर टूट गए। कितनों का साथ छूट गया।
कितने मजदूर लाचार पाँव के छालों के संग घर की ओर लौट पड़े, इसकी गणना संभव नहीं। वह दर्द भरी स्थितियाँ मन के दरवाजे पर दस्तक देतीं और अपना हाथ खोल देने को मजबूर करती रहीं। पहले भी शुचि अपनी जरूरतें कम रखती थी। अब महसूस हुआ कि जरूरतों को और कम कर दिया जाए। जो भी घर आ पा रहे थे, उनकी मदद की जाए। एमएनसी में कार्यरत अंकित काफी समृद्ध था। समयाभाव के अलावा घर में कोई अभाव न था। लेकिन शुचि शुरू से ही हाथ बांँधकर चलने की आदी रही थी। उसे सबकी मदद करना भाता।
उसे अखरता कि सब घर में बंद…सब तकलीफ से भरे…सब डरे हुए…कुछ अनजाने में तो कुछ जिदभरी लापरवाही से काल का ग्रास बन रहे थे।
“पहले का दर्द ही कम नहीं कि अब कोविड दो शुरू। डेल्टा वेरिंएट की भयानकता समझने से पूर्व कला को खो दिया था हमने।…मुझमें अब और किसी को खोने का साहस नहीं है।”
अंकित कह उठा, जब एकाएक अपने भाई साहब के एडमिट होने की खबर सुनी। वेंटीलेटर पर, आॅक्सीजन लेवल कम। आशंकाओं की कुहेलिका में भटकने लगे दोनों। नए वेरिंयट की शिकार भतीजी कला दो दिन तक अस्पताल में रही थी। देर से एडमिट करने का खामियाजा पूरे परिवार ने भुगता था। लेकिन भाई साहब को समय पर अस्पताल पहुँचाया गया। खबर मिलते ही एम्बुलेंस गेट पर लग गया था। पूरे परिसर में एम्बुलेंस की दहशत पहुँच गई। घर के दरवाजे और कसकर बंद कर लिये गए।
“कुछ भी, कभी भी हो सकता है शुचि।”
“ओह! बर्दाश्त के बाहर है। अभी उनका एक भी बच्चा सेटल नहीं हुआ है।”
“यह रात बहुत भारी है।”
अंकित ने गालों पर हाथ रख कुछ सोचते हुए कहा तो शुचि निःशब्द! बस, उसका हाथ सहलाती रही। दीदी-भाई साहब से अंकित बहुत जुड़ा था। इन दोनों ने उसकी परवरिश में अहम भूमिका निभाई थी। गुरुतुल्य थे अंकित के लिए दोनों। पापा की असमय मौत पर उन दोनों ने ही उसकी पढ़ाई पूरी कराई थी। इंजीनियर अंकित माँ को नहीं देख पाने का गम दीदी में ही तो भुला पाता था।
और तीसरी रात बस, एक सूचना बनकर आए भाई साहब,
“अंकित के भाई साब नहीं रहे शुचि।”
उधर से शुचि के भाई ने फोन किया। शुचि ने मेज के कोर का सहारा लिया।
“…कैसे?…कितने लोग ठीक भी तो हुए हैं।”
“इस दूसरी लहर में नहीं। कुछ समझने से पहले ही लोग चले जा रहे हैं। न जाने क्या दिन देखना लिखा है।”
“हम दोनों आते हैं।”
“नहीं! नहीं आना है। अंकित की दीदी, बच्चे तक हाॅस्पिटल नहीं जा सके। पीपीई किट में लिपटे भाई साब को सीधे श्मशान ले जाया गया। मैंने रोने की आवाज सुनकर फोन से पूछा। बगल में रहकर भी कहाँ जा पाया।”
“अंकित को आप न बताएँ भैया। उन्हें अचानक खबर देने पर… “
जोर की रुलाई बाहर निकली। शुचि ने दोनों हथेलियों से दबा ली। दुबारा फोन को कान से लगाया।
“ओह! किसी ने मुँह में गंगाजल और तुलसी तक नहीं दिया होगा।”
उसे समझा-बुझा कर भाई ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया।
बताना ही था, अंततः शुचि ने हौले से अंकित को बता दिया।
सन्नाटा खिंच गया। खिंचा रहा। अंकित और घर की चुप्पी खल रही थी उसे। पर उपाय क्या?
जब-तब इस सन्नाटे के आदी हो जा रहे थे सब लोग। चीत्कार के बाद का सन्नाटा! घोड़े पर सवार रहनेवाला वक्त कछुआ की चाल धारण कर चुका था। बेमन से अंकित वर्क फ्राॅम होम के लिए दिन-रात लैपटॉप से जूझने लगा और शुचि अकेली पड़ती गई…और भी अकेली। बेटी के अमेरिका पढ़ने जाने के बाद शादी पूर्व किया गया ब्यूटीशियन का कोर्स काम आया था। शुचि ने एक भव्य पार्लर मेन रोड में खोला था और अपने को व्यस्त कर लिया था। खालीपन की अचूक दवा…आजकल उसका ब्यूटी पार्लर भी तो बंद है।
न्यूज देखना भारी लगता। अखबार की सूचनाएंँ, खबरें डरातीं। आमो-खास लोग अवसाद में जा रहे थे। आस-पड़ोस की खबर न मिलती। कभी मिलती भी तो मौत में लिपटकर। शुचि से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी मौतों के आँकड़ों को झेलना कठिन। रिंगटोन बजता, आशंकाएँ सर उठातीं। और बुरी खबर मिल ही जाती हर दो-तीन दिन में।
“बच्चे अनाथ! बूढ़े बेबस!…ओह! यह दूसरी लहर युवाओं को ग्रास बना रहा है।”
विचलित होकर अंकित के खाली होते ही उसके पास जा बैठती। उसके चेहरे पे सदा खिली रहनेवाली हँसी की गौरैया उड़ गई।
“ब्यूटीशियन खुद सुंदर न हो तो कौन आएगा?” – कह कर सदा सजी-धजी रहनेवाली गौरांग, छरहरी, खूबसूरत शुचि अब नहीं सज पाती। अक्सर उसके नथूने अगरबत्तियों के धूम्र गंध से भरे होते, जो कभी जलाए ही नहीं जाते। लाशें घर कहाँ आ रही थीं। आस-पास का रूदन गुपचुप सिसकियों में ढली होतीं…किसी को भनक न लग जाए। अछूतों से व्यवहार का भय बड़ा था। सब कुछ गुपचुप!…चुपचुप!!
और तभी उसने निर्णय लिया, ‘कुछ कर नहीं सकती पर लोगों को सुकून, हिम्मत देने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। उम्मीद और धैर्य तो थमा ही सकती हूँ।
चलो, यह भी नहीं न सही, माहौल को हल्का तो कर सकती हूँ। पहले कोविड लहर के समय भी तो यही किया था। और अपने बस में है भी क्या।’
शुचि ने गैलरी खंगाली और कब से क्लिक कर रखे गए फूलों को छोटे संदेशों के साथ पोस्ट करने लगी।
अभी अनेक मौतों का बोझ कम भी नहीं हुआ था कि फोन की ट्रिंग!… ट्रिंग!!
“हम सब क्वारेंटाइन हैं। पूरे परिवार को कोरोना ने दबोच रखा है।” – दिल्ली से सुरेश जी थे।
“अरे! कैसे? बाहर गए थे?”
“नहीं! पर बेटा मुंबई से लौटकर सेल्फ क्वारेंटाइन था। फिर एक शादी में तीन दिन रहा।”
“उसी से। वहीं से आपके घर आया कोविड। अब सावधान रहें और कड़ाई से गाइड लाइन का पालन करें।”
“हाँ, अवश्य।” – एक कमजोर आवाज।
“बाहर ‘सहायक’ की चिट पर उचित हिदायतें लिख चिपकाई गई हैं। गनीमत है, इस बार घेराबंदी नहीं की जाती।” – सुरेश जी आगे कहने लगे।
शुचि ने हाँ में हाँ मिलाई,
” सही। घेरेबंदी से जन मानस में छूत की बीमारी फैल जाती है। सब कटने लगते हैं।”
अंकित ने सुना तो,
“तो क्या? यही उपाय सही है। सोशल डिस्टेंसिंग ही निजात दिलाएगा न? पर लोग मानते कहाँ हैं। एजुकेटेड लोग भी नहीं मानते। इस का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है।”
अभी थोड़ी फुरसत को शुचि और अंकित साथ जी रहे थे।
“इस बार नासमझ पब्लिक को खुद समझने की जरूरत है।…न मास्क, न दूरी। उल्टे जुलूस, धरना प्रदर्शन, समारोहों की गहमागहमी में व्यस्त हैं सब।”
“हाँ! जाके पाँव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। ये लोग अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं।”
शुचि सहमत होती और गहरे भँवर में डूब जाती, उसे कला और भाई साहब की एकांत मौत दहशत में डाल देती। अंकित भी जैसे कहीं खो जाता। चुप्पी गहरा उठती। फिर बड़ी कठिनाई से दोनों अपने को सहेजते, उपाय क्या है।
तीसरे दिन मोबाइल पर सुरेश जी का नं. मिलाते ही बेचैनी भरी लरजती आवाज – “बेटे को आॅक्सीजन की कमी के कारण हाॅस्पिटलाइज करना पड़ा है। हालत गंभीर…।”
“ईश्वर पर भरोसा रखें। ठीक हो जाएगा।”
“उसकी माँ सब देवी-देवता को गच्छे जा रही है ( मनता मानना )”
सुरेश जी धर्मांध नहीं थे, कर्मयोगी थे। समाजसेवी व क्रांतिकारी विचारधारा से ओत-प्रोत कर्मठ नास्तिक व्यक्ति। आज वे भी प्रार्थना में थे, प्रार्थना उनमें थी। उनकी प्रार्थनाओं में भी ईश के प्रति विश्वास था।
टुकड़ों में सूचनाएँ थमा रहा था वक्त।
“अभी हालत बिगड़ने पर दूसरा बेटा शानू रानू को लेकर दूसरे शहर के बड़े अस्पताल में ले जा रहा है। मैं रास्ते में हूँ।”
कह न सकी,
“बीमारी की हालत में आप क्यों…?”
“रानू बड़े हाॅस्पिटल में एडमिट… अब ठीक हो जाएगा। मुझे रास्ते से लौटना पड़ा।”
“रानू ने फोन किया था कि सोमवार से आॅफिस ज्वाइन कर लेगा।”
स्वर में विश्वास का पुट। कुहेलिका से बाहर आने का आभास।
“आप दोनों अपना, बहू व बेटी का ख्याल रखें।”
दूसरे दिन क्षितिज पर लालिमा को दबा कालिमा गहराने लगी थी कि शुचि ने फोन लगाया।
दहाड़ मार कर रोने का स्वर।
“आप रो क्यों रहे हैं?…सब लोग ठीक हैं न।”
“बेटा नहीं रहा शुचि… बेटा नहीं…।”
“ये क्या कह रहे…?”
उन्होंने फोन काट दिया।
अविश्वसनीय था। किससे पुष्टि करूँ? जरूर कानों को धोखा हुआ है। लेकिन खबर सही थी। आज तक शुचि ने किसी पुरुष को ऐसे दहाड़़ मारकर रोते नहीं देखा था।
‘परुष से पुरुष भी अंदर से ऐसे होते हैं?’ – वह अपने आप से प्रश्न करती रही। अगरबत्तियों के धूम्र रेख धुंध सी गहरा गई, जो अगरबत्तियाँ जलाई ही नहीं गईं थीं। रानू की मृत देह अपने शहर, अपने मुहल्ला, अपने मकान की देहरी लाँँघ न सकी थी। शानू ने जीवन के कटु यथार्थ से पहली बार भेंट की और पीपीई किट में लिपटे बड़े भाई रानू को अकेले अग्नि के हवाले कर घर लौटा। लौटा तो पर उसका सारा वजूद वहीं ठिठका रह गया, पूरा लौट न पाया।
शानू के बचपन का साथी, उसके गिल्ली-डंडा, कंचे का संगी, आम-अमरूद तोड़ साथ में एक-एक कट्टे के लिए झगड़ने वाला साथी, क्रिकेट व पढ़ाई का गाइड एकाएक छिन गया…जैसे नन्हें बच्चे के हाथ से सर्वाधिक प्रिय खिलौना।
अपने व्हाट्स एप समूह में यह सूचना गाज की तरह गिरी। सबको स्तब्ध, निष्क्रिय कर गई। अन्य मौतें भी। लगभग हर दिन श्रद्धांजलियों के साथ नए नाम जुड़ने लगे। जिन्होंने इस यथार्थ को बहुत करीब से देखा, वे टूट चुके थे पूरी तरह। किशोर, युवा बेटे जा रहे थे। नन्हें बच्चों के साथ अजन्मे बच्चों के पिता भी। इस बार कोरोना युवाओं पर मेहरबान थी। ऐसी कि त्राहिमाम का शोर हर घर, गली, मुहल्ले, शहर, राज्य, देश-महादेश से उठने लगा। सबके सब हिल गए। हर तरफ की कुसमय मौतों के समाचार से भरने लगा हमारा व्हाट्स एप। कहीं पिता, तो कहीं बच्चे। अभी की सच्चाई…। सबका सारा सुख-चैन छिन गया। सत्ताइस वर्षीय रानू के नाम ने सबको दहला दिया।
साँसों पर भारी पड़ता समय बस, सकारात्मकता परोसने को उकसाता है। और कोई उपाय भी तो नहीं!’ – वह सोचती।
एक दिन शुचि ने सुरेश जी से बहुत हिम्मत कर के बात की।
“रानू को खोकर भी हम खुलकर नहीं रो पा रहे, अपनी आवाज दबा लेते हैं।”
“क्यूँ?” – धीमे स्वर में मुश्किल से पूछ पाई।
“प्रेगनेंट रेखा दहाड़ें मारकर रोती है या बेहोश हो जाती है।”
“बहू… प्रेगनेंट?…ओह! समझ सकती हूँ।”
रानू की माँ, वयोवृद्ध दादा-दादी उसकी पत्नी की क्या हालत होगी, उसे एहसास था। पर उनकी बहू प्रेगनेंट है, नहीं जानती थी।
“फिर भी हम दोनों ने दिल पर पत्थर रख लिया है।…नहीं रोते खुलकर।”
घुटी-घुटी, घुट गई आवाज थी यह। घबराकर उसने आँखें बंद कर लीं। सामने बस उबड़-खाबड़ धरती थी।
एक बार कहा सुरेश जी ने -“हाँ, रानू से आखिरी बार बात हुई थी शुचि। उसने कहा था – मैं साँस नहीं ले पा रहा हूँ पप्पा।…कानों में गूँजती रहती है। मेरा बेटा आॅक्सीजन के बिना…।”
‘क्या मैं पीड़ितों के मन को सुकून नहीं दे सकती।’
‘दिमाग और मन में पड़े फफोले और जलन पर शायद मरहम भरा फाहा रख सकूँ।…शायद!’ – सोचा शुचि ने।
अंकित को भी बताया। और कुछ अंतराल पर फोन करने लगी। मीलों दूरी थी। पास रहकर भी कहाँ पास थे सब।
“एक बात कहूँ?”
“हाँ, कहो।” – जैसे गहरे गह्वर से आवाज आई। टूटे सपनों को महसूस कर रही थी वह।
“आएगा, आपका रानू फिर आएगा। बस, उसे दुबारा पालना-पोसना पड़ेगा। इतना ही फर्क होगा।”
“हाँ, आएगा या आएगी न?…वही होगा न मेरा रानू?”
सुरेश की विह्वलता मन को छू रही थी, निःशब्द कर रही थी उसे। फिर भी हिम्मत कर कह ही डाला,
“हाँ! तब देखिएगा, मन कैसे उसमें रम जाएगा और रानू की कमी कम हो…।” – शुचि को खुद नहीं पता, वह क्या बोल रही है। बस, उसे बाकी जिंदगियों को बचाना था।
“कुछेक महीनों की बात है। मैं अपने पोते के लिए घोड़ा बन जाऊँगा।”
हल्की सी हँसी उधर उभरी। शुचि समझ नहीं पाई, हँसी थी? रूदन था? या भयंकर घुटन? एक साथ पत्नी, बहू, दूसरे बेटे, बेटी और आगत शिशु की जिम्मेदारी सुरेश जी के प्राध्यापक कँधे पर आ गई थी।
बहुत संकोच और डर के साथ शुचि ने दूसरे दिन एक सामान्य पुष्प व्हाट्स एप से भेजा। टाइप किया,
“आनेवाले कल के लिए। जूनियर रानू की किलकारियों के लिए।”
फिर भी मंजिल अभी दूर थी, बहुत दूर।
शुचि का भी धैर्य जवाब दे रहा था लेकिन वह थकने-रूकनेवालों में से नहीं थी। एक-दो दिन के अंतर से भेजती रही फूल। रास्ते में फूल ही फूल नहीं, काँटे भी होते हैं, सबको पता है। लेकिन उसकी कोशिश थी, उन काँटों की चुभन की याद धुंधली कर दे। उधर फेसबुक पर पोस्ट किए जानेवाले गुलाबों ने, सरसों के पीले फूलों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था।
कमेंट बॉक्स में आने लगा था –
“कोविड की इस दूसरी डरावनी लहर में सुकून के कुछ पल।”
“सकारात्मकता फैलाते इन फूलों से राहत मिली।”
“सुखद, शांतिदायक!”
“आपकी पोस्ट ने मरहम का काम किया है।”
“घबराए मन को तसल्ली देते हैं ये फूल।”
“अभी ऐसी पोस्ट की जरूरत, मौत की खबरों ने हिला दिया था।”
आदि…आदि… इत्यादि!
शुचि के सुमन उन खो गए अनामों, परिचितों-अपरिचितों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी थे।
शुचि ने दो काम किए। एक सुरेश जी, उनकी पत्नी एवं माता जी से लगातार बात, दूसरा फूल के संदेशों का प्रेषण। पत्नी या माता जी दो-चार हाँ-हूँ के बाद मोबाइल सुरेश जी को पकड़ा देतीं। पहली बार जब एक पुष्प सुरेश जी के व्हाट्स एप पर खिला, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी। बाद में एक प्रणाम की इमोजी। फिर दो-तीन प्रणाम की, फिर प्रणाम की इमोजियों संग छोटे फूल की इमोजी। अब शुचि के सामान्य फूलों की जगह फूलों के राजा ने ले ली थी।
समय निकट आ रहा था। सुरेश जी की बहू को भी विश्वास और उम्मीद थमाने की कोशिशें रंग ला रही थीं, थोड़ी सही। घाव ताजा था, समय लगना था।
उसके मन में शंका थी। ससंकोच पूछ लिया,
“कहीं फूल भेजकर आपकी तकलीफ बढ़ा… “
“…नहीं! नहीं! मुझे सुकून मिल रहा है। फिर से जीने की प्रेरणा मिल रही है।”
विश्वास और आश्वस्ति का दामन थामे शुचि लगी रही।
वह आज सवेरे ही सींचते वक्त देख चुकी थी, गमले में श्वेत-नारंगी गुलाबों का पूरा बंच हरी-हरी पत्तियों के बीच क्या शोभा पा रहा था। उसने पतले धागे से इस तरह सबको एक साथ बाँधा कि बच्चे, किशोर, प्रौढ़, वृद्ध सारे गुलाब एक सीध में आ गए। थोड़ी मशक्कत हुई तो क्या। संतुष्टि का पलड़ा ज्यादा भारी रहा।
वे फ्लैट की कैद हवा को कब का मुक्त कर चुके थे। चिकित्सक की सलाह थी, खिड़कियाँ खुली रखें। अब भी कुछेक घर नहीं मान रहे थे। अब भी वायरस की जहरीली हवा कह खिड़कियाँ बंद रखते। कोविड 2 का असर कम हो गया था, भय का कद बड़ा।
अंकित के उठने पर शुचि काॅफी के प्यालों संग उसके सामने। सुबह काॅफी लेकर अंकित दोपहर तक सोता है।
‘अभी बैठ लें, फिर कब अंकित फुरसत की साँस लेगा, कहना मुश्किल। रातें तो उसकी हैं ही नहीं।’ – सोचा उसने।
कला और भाई साहब बीच में आ गए। माहौल बोझिल हो उठा। हर दिन अंकित दीदी को फोन लगाता। शुचि भी बात करती। कुछ सांत्वना कुछ हिदायतें, कुछ अश्रुबूंदें, कुछ चुप्पियाँ!
थोड़ी देर बाद,
” जितनी बर्बादी औ तबाही करनी थी, डेल्टा वेरिंयट ने कर दी है। अब कुछेक संस्थान खुल रहे हैं। शायद मेरा आॅफिस भी आॅफ लाइन चले।”
“हाँ, हाॅस्पिटल में भी सामान्य मरीजों, गर्भवती स्त्रियों को एडमिट किया जाने लगा है।”
“सुरेश जी की बहू का क्या हाल है? कितने दिन बाद डिलेवरी…?”
“अभी हफ्ते भर की देर है।”
अंकित की निगाहें अपने वाल पर घूम रही थीं कि एकाएक वह चहका,
“अरे, देखो तो ये सुरेश जी हैं न?”
“हाँ!…हाँ! वही हैं। लगता है, आज ही डिलेवरी हो गई।”
“देखो, क्या लिखा है – मेरा रानू वापस गोद में।”
दोनों उत्सुकता के साथ गुलाबी तौलिए में ढँके-तुपे नन्हें शिशु को देखने लगे, जो सुरेश जी के सुरक्षित हाथों के बीच में निर्द्वद्व सोया था। अभी ठीक से आँखें भी कहाँ खोल पाया था। उतावले सुरेश जी का चेहरा स्मितरहित होते हुए भी शांति और उम्मीद से भरा था।
अपने व्हाट्स एफ समूह में देखा तत्काल। वहाँ भी वही तस्वीर। वे ही लफ्ज! शुचि ने अपने भीतर एक सुकून की साँस महसूस की।
शुचि ने गमलों में सजे गुलाबों में से सबसे सुंदर एक सीधवाले बंच को चुना। क्लिक की और सेंट कर विश लिखने लगी –
“आपका अश्वारोही आ गया। अब घोड़ा बनने की तैयारे शुरू कर दें।”







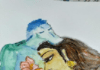


हार्दिक धन्यवाद मेरी कहानी के प्रकाशन के लिए।
अनिता रश्मि
Bahut marmik kahani. COVID ke samay ka jivant chitran.is andhere se bhi ujala aaya.
कोविड की भयावहता का मार्मिक और यथार्थ चित्रण है इस कहानी में। लेकिन अंधेरे के बीच से ही निकलते उजाले की किरणें इस ग़मज़दा माहौल को आंशिक रूप से बदल देती हैं।