हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रेम जनमेजय का नाम किसी परिचय का मोहताज़ नहीं है। व्यंग्य विधा के संवर्द्धन एवं सृजन के क्षेत्र में प्रेम जनमेजय का विशिष्ट स्थान है। व्यंग्य को एक गंभीर कर्म तथा सुशिक्षित मस्तिष्क के प्रयोजन की विधा मानने वाले प्रेम जनमेजय ने हिंदी व्यंग्य को सही दिशा देने में सार्थक भूमिका निभाई है। अबतक उनकी दर्जन भर से अधिक व्यंग्य-कृतियों सहित नाटक, संस्मरण आदि विधाओं की व सम्पादित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पिछले डेढ़ दशक से प्रेम व्यंग्य विधा पर केन्द्रित चर्चित पत्रिका ‘व्यंग्य यात्रा’ का संपादन-प्रकाशन कर रहे हैं। आज साक्षात्कार श्रृंखला की पांचवी कड़ी में प्रस्तुत है प्रेम जनमेजय से युवा लेखक पीयूष द्विवेदी की बातचीत :
सवाल – अपनी अबतक की जीवन-यात्रा के विषय में बताइए। विशेषकर ये कि जीवन के किस दौर में साहित्य की तरफ गंभीर रुझान हुआ और कब व्यंग्य-लेखन की तरफ मुड़े?
प्रेम जनमेजय – यह प्रश्न मुझसे अनेक बार पूछा गया और अनेक बार ही जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं टरे – चन्द्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चन्द्र का टरै न सत्य विचार – वैसे ही मेरा सत्य विचार नहीं टरा कि मैं जन्मजात लेखक नहीं हूं। मेरा जन्म न तो किसी साहित्यिक परिवार में हुआ है, और न ही बचपन में, मेरे पड़ोस में कोई छोटा-बड़ा साहित्यकार रहता था। और रहता भी हो तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे गिल्ली-डंडा, और बिल्लियों के बच्चों से खेलने से ही फुरसत नहीं मिलती थी। मेरे खानदान में भी लेखक नामक कोई जीव पैदा नहीं हुआ है। साहित्य की ओर मुड़ना एक बाई प्रोडेक्ट के रूप में था।
मेरा जन्म इलाहबाद के कमला नेहरू अस्पताल में 18 मार्च, 1949 को दोपहर ढाई बजे हुआ था। मेरा जन्म इलाहबाद में हुआ है, यह मात्र घटना है और इस घटना के आधार पर मैं अपनी श्रेष्ठता का दावा प्रस्तुत कर सकता हूं। हिंदी साहित्य के खाड़े-अखाड़े‘बाज’, उठापटकाउ और इसकी महत्वपूर्ण दिशा तय करने वाले श्रेष्ठी, दलित, वंचित सभी यह जानते हैं कि आज चाहें हिंदी साहित्य की राजधानी दिल्ली है, इससे पहले इलाहबाद थी। अगर आप साहित्यकार हैं और इलाहबाद से जुड़े हुए हैं, तो आपके साहित्यकार होने में कोई शक होने का मतलब ही नहीं होता है तथा दूसरों से दो-तीन इंच ऊंचे उठे होने का आरक्षण भी आपको मिल जाता है। अब किसने देखा और किसे पता है कि मैंने बचपन में क्या किया है?
मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि उन दिनों हमारे पिता हम भाईयों को सुबह समय घुमाने ले जाते और अक्सर दारागंज से होकर जाते थे। वे मुझे हर बार निराला का घर दिखाकर कहते थे कि तुम्हें ऐसा बनना है। और मुझे लगता है कि निराला की उस गली का कोई साहित्यिक कीड़ा मेरे मस्तिष्क में घुस गया और मैं साहित्यकार बन गया। निराला के साहित्य में व्यंग्य भी है, इसलिए हो सकता है कि वो कीड़ा व्यंग्य वाला हो। इसलिए कैलाश वाजपेयी जैसे अध्यापक से पढ़ने के बावजूद मैं निराला की गली के कीड़े के कारण व्यंग्यकार बन गया। मेरा एक चित्र महादेवी वर्मा के साथ भी है। वह भी तो इलाहाबाद की थीं, और फिर चित्र भी है, तो कहने में क्या हर्ज है कि जब मैंनें उन्हें अपनी व्यंग्य कविता सुनाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए यही मार्ग श्रेष्ठ है।
वास्तव में, मेरे लेखन का आरंभ सायास नहीं, अनायास ही हुआ जैसे प्रथम दृष्टि में प्रेम अनायास होता है। जहां तक लेखन की दुनिया में आने का दिन और समय बताने जैसी जिज्ञासा है, मेरा जीवन पगडंडियों की तरह आड़ा-तिरछा बेतरतीब रहा है। ग्यारहवीं की परीक्षा देने के बाद मेर पास कुछ करने को न था। उन दिनों इंजीनियरिंग आदि की परीक्षाओं के लिए गर्मियों की छुट्टियों का बलिदान नहीं करना पड़ता था। मेरे अंदर का लेखक फिर जागा और मैंने एक प्रेम-कथा लिखी– कल आज और कल। इसे मैंने गाजियाबाद से उन दिनों अपने शीघ्र प्रकाशन की घोषणा करने वाली पत्रिका ‘खिलते फूल’ में भेज दिया। से.रा. यात्री उसके परामर्शदाता थे। ‘कल आज और कल’ कहानी ने मेरे जीवन की दिशा बदली। 1966 में हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम आए। जासूसी उपन्यासों एवं लेखन के कीड़े ने अपना प्रभाव दिखाया। अंक इतने अच्छे नहीं थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल सके। उन दिनो रामकृष्ण पुरम् के साथ लगती सरकारी कॉलोनी, मोतीबाग में, डिग्री कॉलेज के नाम से, जो बाद में हस्तिनापुर कॉलेज और आजकल मोतीलाल नेहरू कॉलेज के नाम से जाना जाता है, खुला था। वहां मैंने अपने प्रिय विषय मैथ्स ऑनर्स में प्रवेश ले लिया। उन्हीं दिनो मेरी कहानी, ‘कल आज और कल’, ‘खिलते फूल’ पत्रिका के प्रवेशांक में प्रकाशित होकर आई। मैं हिन्दी के ‘किसी’ अध्यापक को ढूंढ रहा था, तो किसी ने डॉ. महेन्द्र कुमार की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे हिन्दी के अध्यापक हैं और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी।
मैंने उनसे कहा– सर! देखिए ये मेरी कहानी छपी है।’
उन्होंने मेरी ओर ध्यान से देखा और कहा- तुमने क्या अभी हिंदी ऑनर्स में प्रवेश लिया है। इससे पहले तो तुम्हें क्लास में कभी देखा नहीं।
मैंने कहा – सर! मैं मैथ्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूं।
उन्होंने अपने हाथ में ली पत्रिका को एक बार और देखा और कहा – हिंदी में कहानी लिखते हो। तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी है, तुम हिंदी ऑनर्स क्यों नहीं लेते?’
बहुत कम लोग हिंदी ऑनर्स अपनी रुचि से लेते थे। इस विषय को या तो लड़कियां लेती थीं या फिर वे जिनके अंक कम आते थे और उन्हें किसी अन्य ऑनर्स में प्रवेश नहीं मिलता था। डॉ. महेंद्र कुमार हिंदी ऑनर्स का पहला बैच बना रहे थे और एक अध्यक्ष के रूप में एक शिकारी की तरह अच्छे विद्यार्थियों को हिंदी ऑनर्स में प्रविष्ट कराने के लिए बाड़ा तैयार कर रहे थे, शिकार कर रहे थे।
मैंने कहा – सर! मैंने तीन साल तक हिन्दी बिलकुल नहीं पढ़ी है।’
– तो क्या हुआ, मैंने भी बी.एस.सी. के बाद हिन्दी में एम.ए, किया है।’ उसी समय हाथ में रजिस्टर पकड़े नरेन्द्र कोहली वहां आए। उन्होंने उनसे कहा, ‘देखो इस लड़के की कितनी अच्छी कहानी छपी है। साईंस स्टूडेंट होकर इसने कहानी लिखी है। मैथ्स ऑनर्स में है। मैं इसे कह रहा हूं कि तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी है, हिंदी ऑनर्स में एडमिशन ले लो। पर कहता है कि मैने हायर सेकेंडरी में हिंदी नहीं पढ़ी है। इसे समझाओ।’’ फिर मेरी ओर घूमकर डॉ. महेंद्र कुमार बोले — ये नरेंद्र है, इसने भी इंटर तक विज्ञान पढ़ा है। बाद में हिंदी में ऑनर्स और एम ए फर्स्ट क्लास में किया है। लेक्चरर बन गया है। कहानियां लिख रहा हैं। तुम इनसे बात करो।’’
नरेंद्र कोहली ने मेरे मन में हिंदी के प्रति विश्वास भरा। एक तरह से मेरा ब्रेन वाश हो चुका था। मैं मैथ्स ऑनर्स से हिंदी ऑनर्स का विद्यार्थी बन गया।
मैंने गंभीरता के साथ साहित्य अध्ययन एवं लेखन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किया। इसे मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि साहित्य पढ़ाने वाले मेरे अनेक साहित्य-विरक्त अध्यापकों के अतिरिक्त नरेंद्र कोहली और कैलाश वाजपेयी जैसे साहित्यकार प्राध्यापकों के रूप में मिले। ये दोनों लेखकीय दंभ के शिकार नहीं थे, अतः मन से सहायता करने को तैयार थे। समझ लें कि सत्रह-अठारह वर्ष की आयु में साहित्य अध्ययन और लेखन की अल्प समझ पैदा हुई। अब एक ओर कैलाश वाजपेयी जैसे नई कविता के कवि और दूसरी ओर कथाकार व व्यंग्यकार नरेंद्र कोहली के साथ ने मुझे व्यंग्य की ओर क्यों और कैसे मोड़ा, इसे सरलीकृत रूप में नहीं कहा जा सकता है। लगता है, यहां आपकी जमीन काम करती है। या कहें आपका स्वभाव काम करता है। आप सार-सार गहि लेते हैं।
वैसे तो प्रत्येक रचनाकार आरंभिक अवस्था में कवि ही होता है। प्रेमप्रकाश निर्मल के नाम से आरंभ में मेरी कुछ कविताएं प्रकाशित हुईं फिर शताब्दी, खिलते फूल, कहानीकार में कुछ कहानियां भी छपीं। प्रेम जनमेजय के नाम से मेरे व्यंग्य पहले ‘माधुरी’ में और फिर ‘धर्मयुग’ में प्रकाशित होने आरंभ हुए।
विधा के चुनाव में अनेक फैक्टर काम करते हैं- रचनाकार का व्यक्तित्व, उसका परिवेश, जीवन दृष्टि, रचनात्मक पसंद, लेखकीय शैली आदि। मेरे माता-पिता ने हम तीनों भाईयों को आरम्भ से अनुचित को न सहने, सत्य पर दृढ़ रहने, सात्विक क्रोध को अभिव्यक्त करने तथा असीम विषम परिस्थितियों में भी किसी के सामने हाथ न पसारने के जो संस्कार दिये और संयोग से अपने लेखन के शैशव में वरिष्ठ रचनाकारों से जो साहित्यिक संस्कार मिले, हो सकता है उन्हीं कारणों से मेरा व्यंग्यकार व्यक्तित्व बना हो। उन दिनों हिंदी साहित्य में धर्मयुगीन और साप्ताहिकी काल चल रहा था। व्यंग्य की ओर निरंतर बढ़ती रुचि ने उस समय के व्यंग्यकारों के लेखन की ओर आकार्षित किया। इधर मैं साहित्य की किताबों में कबीर को पढ़ रहा था, व्यंग्य के संस्कार ग्रहण कर रहा था और उधर पत्रिकाओं में परसाई के व्यंग्य लेखन से रु-ब-रु हो रहा था। परसाई को पढ़ता और वैसा लिखने को प्रेरित होता। ‘धर्मयुग’ का बैठे ठाले और साप्ताहिक हिंदुस्तान का ‘ताल बेताल’ स्तंभ पहली पसंद बन गये । परसाई, जोशी और त्यागी की तिकड़ी का हास्य-व्यंग्य लेखन अपने रंग में रंगने लगा। उन दिनों टाईम्स ग्रुप की फिल्मी पत्रिका ‘माधुरी’, जिसके संपादक अरविंद कुमार थे, में मेरे व्यंग्य यदा-कदा प्रकाशित होने लगे। उनसे प्रसिद्धि मिली। धर्मयुग में प्रकाशित ‘समीक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन’ व्यंग्य को मैं अपने व्यंग्य लेखन का शुरुआती व्यंग्य कह सकता हूँ।
मेरा पहला संग्रह, ‘राजधानी में गंवार’ 1978 में गुरु कृपा से, पराग प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। श्रीकृष्ण ने एक नए लेखक के पहले संकलन को बिना कुछ लिए दिए प्रकाशित किया, इसके पीछे गुरु नरेंद्र कोहली का बल था। उन दिनों के चर्चित युवा कवि एवं चित्रकार अवधेश ने इसका कवर बनाया था। इस संकलन ने मुझे व्यंग्य की मुख्यधरा में ला खड़ा किया। दिविक रमेश ने दिशाबोध के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की थी। इस गोष्ठी की अध्यक्षता रवींद्रनाथ त्यागी ने की थी। गोष्ठी में सुधीश पचैरी, शेरजंग गर्ग और नरेन्द्र कोहली ने विस्तृत आलेख पढ़े थे। हरीश नवल, डॉ. हरदयाल, डॉ. विनय, अवध नारायण मुद्गल, सुरेश कांत, रमेश बत्तरा नरेन्द्र निर्मोंही आदि ने अपने विचार रखे थे। अध्यक्ष रवींद्रनाथ त्यागी ने विस्तृत टिप्पणी की, पर उनकी इस बात ने मुझे बल दिया कि यह पुस्तक शेल्फ में रखने योग्य है। इसी पुस्तक ने मुझे व्यंग्य के टेढ़े मार्ग पर डाल दिया।
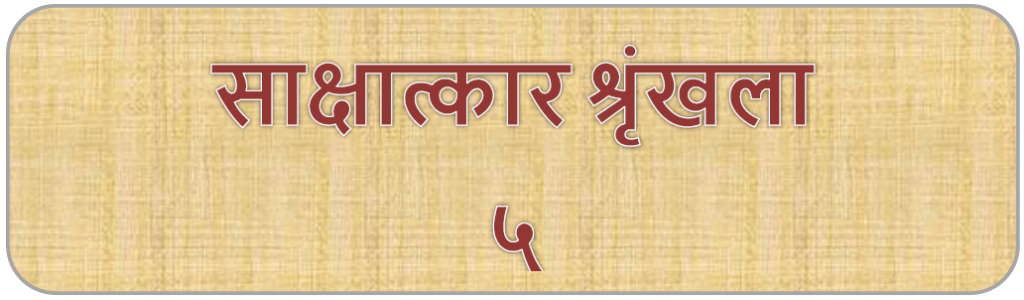



पढ़कर सुखद अनुभूति हुई, बहुत बधाई आपको।