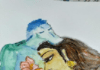विकलांगता का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव जाति का इतिहास। मानव जीवन के साथ विकलांगता का संबंध किसी-न-किसी रूप से जुड़ा हुआ है। हर युग में विकलांगों का अस्तित्व रहा है। किसी भी समय में किसी स्थान के सभी मनुष्य पूर्णतः स्वस्थ या सकलांग नहीं हो सकते। दरअसल ‘सकलांगता’ तथा ‘विकलांगता’ सापेक्षिक शब्दावली है। कोई भी व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो सकता, भले ही वह बाह्य दृष्टि से कितना ही स्वस्थ क्यों न दिखाई दे।
सामान्यतः किसी अंग विशेष की क्षति को विकलांगता कहा जाता है। विकलांगता से तात्पर्य होता है कि बहुत सारी समस्याओं तथा चुनौतियों से घिर जाना। सामान्य भाषा में विकलांगता का अर्थ कम क्षमतावान, जीविकोपार्जन में व्यवधान या जिन्दगी की रोजमर्रा के क्रियाकलापों को निष्पादित करने में विफलता से लगाया जाता है। इसके अनेक रूप होते हैं-अस्थि विकलांगता, दृष्टि बाधित विकलांगता, मानसिक विकलांगता तथा श्रुति-बाधितार्थ विकलांगता। कुछ लोग जन्मजात विकलांग होते हैं तो कुछ बीमारी, दुर्घटना, युद्ध, प्राकृतिक आपदा, कुपोषण, अशिक्षा व लापरवाही आदि अन्य कारणों से विकलांगता की चपेट में आ जाते हैं।
प्रायः हरेक समाज में विकलांगता की संकल्पनाओं में विविधता होती है। विकलांग व्यक्तियों में विकलांगता की मात्रा में भी भिन्नता होती है। श्रवण तथा दृष्टिबाधित व्यक्तियों की विकलांगता की मात्रा में भिन्नता होती है, अस्थि विकलांगता से ग्रस्त कुछ व्यक्ति सामान्य स्थितियों में चल फिर सकते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ व्यक्ति गंभीर रूप से मानसिक रुग्णता के शिकार होते हैं, जबकि दूसरे मनोरोगी सामान्य रूप से। विकलांगता कई मामलों में स्थैतिक होती है तथा कुछ मामलों में निरंतर बढ़ने वाली। मल्टीपल सेलोरोसिस, मस्क्यूलर डिस्ट्राफी, क्राइस्टिक फेबरोसिस, विजुअल एण्ड हियरिंग इम्पेयरमेन्ट्स कुछ खास तरह के कैंसर तथा हृदय रोग संबंधी बीमारियाँ लगातार विकसित होने वाली विकलांगता की स्थिति होती है।
1970 के बाद के दशकों में विकलांगों के प्रति सामाजिक अवधारणा में महत्त्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी परिवत्र्तन शुरू हुआ। पहले जहाँ विकलांगता को दैवीय प्रकोप, पूर्वजन्म का फल मानकर विकलांगों को घृणा या दया का पात्र माना जाता था, वहाँ अब उसे समाज के अभिन्न रूप में देखा जाने लगा है। विकलांगता की समस्या सिर्फ व्यक्तिगत और चिकित्सकीय न होकर मानवाधिकार एवं सामाजिक-राजनीतिक मुद्दा बन गयी है। स्वयंसेवी संस्थाओं और बौद्धिक वर्ग ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकलांगों के पुनर्वास के लिए सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए। विकलांगता अधिकार आन्दोलन के कारण ही सामाजिक अवधारणाएँ बदलती गईं और दया एवं सहानुभूति के स्थान पर अधिकार आधारित परिप्रेक्ष्य सामने आया। फलस्वरूप, विकलांगों का सशक्तिकरण कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जाने लगा।
चिकित्सा तथा टेक्नालाॅजी के क्षेत्र में हासिल की गयी उपलब्धियों के बावजूद विकलांगों के प्रति सामाजिक धारणा अपरिवर्तित रही तथा विकलांग व्यक्तियों को दया एवं सहानुभूति का पात्र माना जाता रहा। 19वीं सदी के दौरान पुनर्वास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गयी। फिर 20वीं सदी में औद्योगीकरण ने जोऱ पकड़ा तथा विकलांगों तथा वंचित तबके के लोगों के कल्याण हेतु कानून-निर्माण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। पुनर्वास की दिशा में उठाए जा रहे इन कदमों को प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध ने नया आयाम प्रदान किया। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध की परिस्थितियों ने विकलांगों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के चैथे चरण का सूत्रपात किया। इस चरण में विकलांगों के सामाजिक समंजन के प्रति जनचेतना विकसित होनी शुरू हुई।
विकलांग व्यक्ति भी मानव प्राणी हैं। समाज के अन्य लोगों की तरह उनकी भी भोजन, आश्रय, प्रेम-स्नेह, यौनिकता तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताएँ होती हंै। मानवाधिकारों के संवर्द्धन तथा सुरक्षा की दिशा में व्यवस्थित तथा संगठित प्रयास 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद ही जोर पकड़ा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 1975 में विकलांगों के अधिकारों का घोषणा-पत्र पारित किया गया। विकलांगों के अधिकारों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय 2006 में पारित हुआ। भारत सरकार के द्वारा 2008 में इस अभिसमय को अनुसमर्थित किया गया। विकलांग व्यक्तियों के समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 में पारित हुआ, जिसकी जगह हाल ही में संसद द्वारा पारित विकलांगों के अधिकार अधिनियम 2016 ने लिया है। विकलांगों को इसका कितना और क्या लाभ मिल रहा हैं, यह विचारणीय पहलू है।
संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 1975 में विकलांगों के अधिकारों से संबंधित घोषणा पत्र का पारित किया जाना, वर्ष 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष तथा 1983 से 1992 के दशक को विश्व विकलांग दशक के रूप में मनाया जाना, 1993 में विकलांगों के समान अवसर से संबंधित मानक नियमों तथा 2006 में विकलांगों के अधिकारों से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का पारित किया जाना, इस संदर्भ में विशेषतः उल्लेखनीय है। भारत सरकार के द्वारा भी मई 2008 में विकलांगों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय (2006) को अनुसमर्थित किया जा चुका है। दूसरे शब्दों में, इस अभिसमय के अनुसमर्थन से भारत सरकार की नैतिक बाध्यता हो गई है कि विकलांगता से संबंधित कानूनी तथा सरकारी प्रावधानों में आमूल परिवत्र्तन लाकर उसे अभिसमय में निहित आदर्शों के अनुरूप बनाया जा सके। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा विकलांगों के अधिकारों से संबंधित अधिनियम 2016 (जिसने पूर्ववर्ती अधिनियम का स्थान ले लिया है) के पारित किए जाने को इसी कड़ी में मील का पत्थर माना जा सकता है।
यहाँ तक कि इस क्षेत्र में सरकारी क्रिया-कलापों के मूल्यांकन से सहज ही इस बात की पुष्टि हो सकती है कि उपरोक्त अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में कितनी उदासीनता बऱती गई है। 1995 के अधिनियम के दौरान भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों तथा स्वायŸाशासी निकायों (जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं) की नौकरियों में ए, बी, सी तथा डी संवर्गों में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया; जिसमें 1 प्रतिशत अस्थि विकलांग, 1 प्रतिशत दृष्टि बाधितार्थ तथा 1 प्रतिशत श्रुति बाधितार्थ के हेतु आरक्षित किया गया।विकलांगों के अधिकार अधिनियम 2016 के द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा पाँच प्रतिशत कर दी गयी है।
किसी भी काल और स्थान की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति को जानने के प्रमुख स्रोतों में साहित्य भी होता है। साहित्य हमें न केवल संवेदनशील बनाता है बल्कि हमारी संवेदनशीलता का दायरा बढ़ता है। साहित्य हमें उनकी पीड़ा से परिचित कराता है जिनसे हम कभी मिले भी नहीं होते हैं। हम अपने जीवन में रोज ही अनेक विकलांग व्यक्तियों को अपने आस-पास देखते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी परेशानियों और समस्याओं को सही मायने में नहीं समझ पाते परन्तु जब हम साहित्य के किसी विधा में ऐसे पात्रों को पाते हैं तो उनकी पीड़ा, अपमान, शोषण, उपेक्षा आदि को गहराई से समझ पाते हैं।
साहित्य के दोनों ही रूपों (यथा, गद्य तथा पद्य) में विकलांगों का चित्रण नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों ही रूपों में किया गया है। साहित्यकार विकलांगता का चित्रण उपहासात्मक ढ़ंग से प्रवृत्त होकर करते हैं-मानो शारीरिक सुंदरता आत्मा की सुंदरता से जुड़ी होती है तथा विकलांगता या वक्रता शारीरिक कुरूपता से जुड़ी होती है। सक्षमता तथा विकलांगता लोगों के दिलो-दिमाग में इस तरह बैठ जाता है, जैसे विकलांगता तथा शारीरिक पूर्णता में विरोधाभाषी संबंध हो।
समकालीन परिस्थिति में विकलांगता अधिकार के दौर में यह माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता। समाज ही उसे भला या बुरा बनाता है। हिन्दी साहित्य में भी ऐसा नहीं है कि विकलांग पात्र नकारात्मक रूप में ही चित्रित हुए हैं। हिन्दी साहित्य में जहाँ अनेक विकलांग पात्रों का चित्रण मिलता है वहीं विकलांग साहित्यकारों ने भी अनेक अद्भुत और उत्कृष्ट रचनाएँ कर हिन्दी साहित्य-भंडार को समृद्ध किया है। इस क्रम में मध्यकाल के दो प्रमुख कवियों का नाम महत्त्वपूर्ण है। जायसी और सूरदास दोनों ही शारीरिक रूप से विकलांग थे। इन दोनों कवियों की महत्ता स्वयं-सिद्ध है। इन दोनों ने जैसी उत्कृष्ट रचनाएँ की है, उसमें इनकी विकलांगता बाधक नहीं होती। मध्यकाल के ही प्रमुख कवि तुलसी लिखते हैं —
‘‘काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानी’’ …
अर्थात् कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। तुलसी की इस उक्ति से तत्कालीन समय में विकलांगों के प्रति सामाजिक अवधारणा अभिव्यक्त होती है। प्रेमचन्द अपनी कालजयी कृति ‘रंगभूमि’ के आरम्भ में सूरदास का परिचय देते हुए लिखते हैं- ‘‘भारतवर्ष में अंधे आदमियों के लिए न नाम की जरूरत है न काम की। सूरदास उनका बना-बनाया नाम है और भीख माँगना बना-बनाया काम है।’’ विकलांगता को भिक्षावृत्ति से जोड़ने वाली प्रवृत्ति के कारणों की पड़ताल करने की भी आवश्यकता है। विकलांगों का नामकरण उनकी विकलांगता के आधार पर करने की प्रवृत्ति तथा विकलांगों के लिए समाज में प्रचलित कहावतों और लोकोक्तियों के अनेक उदाहरण ‘राग दरबारी’, ‘तुम्हारे हिस्से का चाँद’, मुर्दहिया आदि गद्य रचनाओं में देखने को मिलते हैं।
जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक उपन्यास ‘ध्रुवस्वामिनी’ में हिजड़ा, कुबड़ा और बौना तीन विकलांग पात्रों का चित्रण हुआ है। इन पात्रों का प्रयोग नाटककार ने हास्य प्रस्तुत करने के लिए नहीं किया है, बल्कि उन विकलांग पात्रों के माध्यम से मर्यादाविहीन, कायर एवं नपंुसक मानसिकता वाले रामगुप्त और शिखरस्वामी पर व्यंग्य किया है। इसी तरह धर्मवीर भारती की रचना ‘अंधायुग’ काव्य नाटक में विकलांगता से ग्रस्त मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई है।
इस संकलन के माध्यम से यह देखने का प्रयास किया गया है कि इन कहानियों में अभिव्यक्त विकलांग पात्रों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कैसी है? इसमें 1900 ई. से अब तक की कुछ उन चुनिंदा कहानियों को लिया गया है जिसमें विकलांगता के किसी-न-किसी पहलू को स्पर्श किया गया है, इन कहानियों में कुछ समस्याएँ तो समान है पर कुछ अलग-अलग। क्या वर्ग, वर्ण, लिंग, परिवेश और विकलांगता के प्रकार की भिन्नता के कारण विकलांगों की समस्याएँ भिन्न-भिन्न हो जाती है? उन्हें रोजमर्रा की जिन्दगी में किन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, उनकी मुख्य और गौण समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? विकलांग बच्चों के प्रति अभिभावकों के दोहरे व्यवहार की अभिव्यक्ति ‘खुदा की देन’ (चन्द्रकिरण सौनरेक्सा), ‘कंपनी राजेश्वर सिंह का दुख’ (उमाशंकर चैधरी), ‘उपहार’ (कुसुमलता मलिक) आदि कहानियों में हुई है।
पुरुषसत्तात्मक समाज की खामियों से विकलांग व्यक्ति भी मुक्त नहीं हैं। विकलांग होने पर भी पुरुष पत्नी पर हावी रहना चाहता है, जो अनेक कहानियों में देखने को मिलता है। ‘सीढ़ियों का ठेका’ (मेहरून्निसा परवेज), ‘खुदा की देन’ (चन्द्रकिरण सौनरेक्सा) में विकलांगता के पश्चात् भिक्षावृत्ति को रोजगार के रूप में अपनाने की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। धर्मवीर भारती की कहानी ‘गुलकी बन्नो’, सच्चिदानन्द धूमकेतु की ‘एक थी शकुन दी’ मैत्रेयी पुष्पा की ‘सहचर’, कहानियों में विकलांग स्त्री के जीवन संघर्षों को उद्घाटित किया गया है। पारिवारिक विघटन के कारण विकलांग सदस्यों की देखभाल में परेशानी होती है। इस समस्या से रू-ब-रू कराती है- रमेश खत्री की कहानी ‘मैं तलाक ले रही हूँ।
विकलांग गर्भस्थ शिशु के भ्रूण-हत्या के औचित्य-अनौचित्य का सवाल खड़ा किया है तेजेन्द्र और उपासना ने अपनी कहानियाँ ‘मुझे मार डाल … बेटा!’ और ‘मुक्ति’ में। विकलांगता के कारण आर्थिक परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। आर्थिक परेशानियों की वजह से कई बार समय पर और सही इलाज न होने के कारण व्यक्ति ऐसी विकलांगता का शिकार हो जाता है जिससे उसे बचाया जा सकता था। ‘खुदा की देन’, ‘अन्ना’ (पानू खोलिया) तथा ‘रोशनी से दूर’ (छत्रपाल) कहानियाँ इसी विषय-वस्तु को लेकर लिखी गई हैं।
मानसिक रूप से विकलांग पात्रों को लेकर लिखी गयी कहानियों को भी इस संकलन में शामिल किया गया है। अमरकांत की कहानी ‘जिंदगी और जोंक’, मार्कण्डेय की ‘हंसा जाई अकेला’, माधव नागदा की ‘जहर काँटा’ आदि ऐसी ही कहानियाँ हैं। एक तरफ विकलांगता से कुंठित चरित्र है तो दूसरी ओर खितीन बाबू और शकुन दी, मुन्नी जैसे जागरूक, जिंदादिल और आत्म विश्वास से भरे चरित्र भी हैं। ये कहानियाँ अलग-अलग काल खण्डों में लिखी गई हैं। क्या इन कहानियों में समय के साथ कोई विकसित चेतना नजर आती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है? इन सभी चरित्रों के शोषण के सामाजिक हथकंडें एवं धार्मिक अंधविश्वास क्या हैं, इनका स्वरूप क्या है?
आमतौर पर जन्म से विकलांग तथा बाल्यावस्था में विकलांगता से ग्रस्त बच्चे विकलांगता की परेशानियों को झेलते हुए अभ्यस्त हो जाते हैं, यदि उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाय तो ऐसे बच्चों में अपनी विकलांगता को लेकर न तो कोई कंुठा का भाव होता है न ही हीनता-बोध। वे सामान्य बच्चों की उपेक्षा झेलकर भी उनके साथ न सिर्फ खेलना चाहते हैं बल्कि वे भी आम बच्चों की ही तरह जिंदादिल होते हैं। चाहे वे ममता कालिया की मुन्नी होे या उमाशंकर चैधरी के नर्मदा, या पानू खोलिया की अन्ना या फिर जगदीशचन्द्र की वीरो। इन सबों में विकलांगता की भयावहता का कोई आतंक नहीं दिखता। छत्रपाल की कहानी ‘रोशनी से दूर’ का बच्चा अपनी विकलांगता को लेकर भयाक्रांत है। बाहरी दुनिया से कटा रहना चाहता है। वह नैरेटर से कहता भी है कि- मैं कभी स्कूल नहीं जाऊँगा, लड़के मुझे छेड़ेंगे।
जब किसी परिवार में कोई विकलांग बच्चा पैदा होता है या किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण विकलांगता की चपेट में आ जाता है तो उसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की जिंदगी भी प्रभावित हो जाती है, विशेषतः माता-पिता की। विकलांग बच्चों की देखभाल, प्रशिक्षण, पढ़ाई-लिखाई में सामान्य बच्चे की तुलना में कई गुना अधिक श्रम लगता है। कुछ बच्चों को दैनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित करने में ही वर्षों लग जाते हंै। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को विशेष धैर्य की आवश्यकता होती है। परिवार के बाकी सदस्यों में भी आपस में प्रेम, सौहार्द्र एवं जिम्मेदारियाँ निभाने की भागीदारी की भावना आवश्यक होती है। तभी एक सुखद माहौल उपस्थित हो सकता है और बच्चे की सही परवरिश हो सकती है।
परिवार में घोर उपेक्षा की शिकार ‘उपकार’ कहानी की विजया अपने आप को इतना असहाय और कमजोर मानने लगती है कि उसे अपनी इस अवस्था से मुक्ति का एक मात्र रास्ता मौत ही प्रतीत होता है। विजया की ऐसी मानसिकता का जिम्मेदार कौन है ? विजया, उसके अभिभावक या समाज।
उपेक्षा, उपहास, भेदभाव का यह सिलसिला अभिभावकों, भाई-बहनों, सहयोगियों, पड़ोसियों तक ही सीमित नहीं रहता। राह चलते लोग भी विकलांगों का मजाक उड़ाने या अपमान करने से नहीं चूकते। हद तो तब हो जाती है जब विकलांग व्यक्ति की स्वयं की संतान उसकी विकलांगता को लेकर हीनता-बोध से ग्रसित हो जाय।
प्रायः सुन्दर लड़कियों को लेकर ही साहित्य-सृजन की परम्परा रही है। इसके विपरीत कुछ साहित्यकारों ने समाज के नजरिये से कुरूप, असुन्दर, विकलांग स्त्री पात्रों को लेकर भी कहानियाँ लिखी है। ‘आधा टिकट’ विकलांग (बौनी) लड़की बीरो की मर्मस्पर्शी कहानी है। इस कहानी में लेखक ने दिखाया है कि किस तरह से एक विकलांग व्यक्ति समाज द्वारा हाशिए पर चला जाता है।
विकलांग बच्चों के प्रति सामाजिक रवैये पर कैलाश वनवासी ने ‘उनकी दुनिया’ कहानी में एक अलग ढ़ंग से विचार किया है। विकलांगों के लिए चाहे जितनी भी संस्थाएँ खुल जायें लेकिन जब तक समर्पित, आत्मीय और स्नेहशील रूप से उनकी देखभाल नहीं की जायेगी, विकलांगों के प्रति सामाजिक मानसिकता में बदलाव नहीं आ सकता।
बच्चे की विकलांगता का माता-पिता पर दो तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। कुछ माता-पिता इसे नियति का क्रूर मजाक समझकर बौखला जाते हैं। उन्हें यह लगने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उनके ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। यह किस पाप की सजा मिली है आदि-आदि। ऐसी सोच का वास्तविक कारण क्या है? क्यों अपने बच्चे की विकलांगता को लेकर माता-पिता लज्जित एवं अपमानित महसूस करते हैं, उनकी ऐसी कुंठा की वजह क्या है ? दरअसल समाज में हर चीज को कर्म-फल से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति के कारण वे बीमारी या विकलांगता को सहज रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। अंधविश्वास के कारण उन्हें अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दाँव पर लगी महसूस होने लगती है। इस तरह की भावना से ग्रस्त होने के कारण वे हताशा और निराशा के शिकार होकर कंुठित हो जाते हैं। उनकी मनोदशा का प्रभाव उनके बच्चे पर भी पड़ता है और बच्चे की जिजीविषा प्रभावित होती है।
कुछ अभिभावक अपने बच्चे की विकलांगता को अभिशाप के रूप में मानते हैं। कुछ अभिभावक शुरू-शुरू में तो पूरे उत्साह के साथ इलाज करवाते हैं, परन्तु जब बच्चे में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिखता तो वे निराश और उदासीन हो जाते हैं। उन्हें वह सारा काम बोझ लगने लगता है। खासकर तब, जब यह उम्मीद ही न बची हो कि वह ठीक हो सकता है, तो उन्हें जिंदगी भर बोझ ढ़ोने के सिवा कुछ भी नहीं लगता। यही अन्ना की माँ उमा के साथ होता है। पानू खोलिया की कहानी ‘अन्ना’ इसी विषयवस्तु पर आधारित है।
चन्द्रकिरण सौनरेक्सा की कहानी ‘खुदा की देन’ में भी आरंभिक दिनों में नज्जो को उसकी माँ गले तक चादर से ढ़के रहती थी लेकिन बाद में उसकी दोनों सूखी टाँगें लकड़ी की तरह मैले गरारे से लटकती रहती थी। बिना धुले, मैल से अटे उसके भूरे बाल, जटाओं में परिवर्तित हो गए थे। इस तरह हम देखते हैं कि आरंभिक उत्साह के स्थान पर उदासीनता आसन जमा लेती है। इसी तरह कुछ माता-पिता अपने बच्चे में विकलांगता से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं कर पाते और सही जानकारी के अभाव में बच्चा अधिक कुंठित हो जाता है।
समाज के लोगों को भी विकलांगों के प्रति सामान्य व्यवहार करना चाहिए ताकि इलाज में नाकामयाबी मिलने पर भी वह अपनी जिंदगी को सहजता से ले सके, विकलांगता उसके मनोबल पर हावी न हो पाये। सामान्य और सरल व्यवहार ही विकलांगों को सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकता है। उनके प्रति उपेक्षा भाव उन्हें निराशा की गहरी खाई में धकेल देगा। इस कहानी में एक तथ्य यह भी उभर कर आता है कि अभिभावकों को अपने सामान्य बच्चों को विकलांग बच्चों के प्रति मैत्री और सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार के लिए प्रेरित करना चाहिए।
जो अभिभावक विकलांगता को चुनौती मानकर उसका सामना करते हैं, विकलांग बच्चे के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, उनके बच्चे विकलांगता के बावजूद ऊँचाइयाँ हासिल करते हैं और अपनी विकलांगता को स्वीकार कर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अरूण यादव की कहानी ‘परफेक्शनिस्ट बाबू’ के शेखर बाबू की तरह। माता-पिता के व्यवहार के सकारात्मक प्रभाव को ममता कालियां की कहानी ‘मुन्नी’ के माध्यम से समझा जा सकता है।
प्रायः विकलांग बच्चों के प्रति अभिभावकों का दोहरा मापदंड होता है। कुसुमलता मलिक की ‘उपहार’ तथा उमाशंकर चैधरी की ‘कंपनी राजेश्वर सिंह का दुःख’ में यह सत्य उद्घाटित हुआ है। संयुक्त परिवारों के विखंडन एवं एकल परिवारों के प्रचलन के कारण विकलांगों की देख-रेख में समस्या उत्पन्न होती है। रामदरश मिश्र की कहानी ‘बहुत देर कर दी’ तथा रमेश खत्री की कहानी ‘मैं तलाक ले रही हूँ’ इस समस्या की ओर ध्यानाकृष्ट करती है। रमेश खत्री की यह कहानी शादी के बाद विकलांग जीवनसाथी के साथ निर्वाह या तलाक के प्रश्न तलाशती है। विकलांग व्यक्ति की शादी में भी अड़चनें उत्पन्न होती हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी विकलांग से शादी करना चाहता भी है तो उसमें भी कई अड़चनंे आती हैं। परिवार वालों का विरोध झेलना पड़ता है। उन्हें इससे अपना सामाजिक स्तर प्रभावित होता नजर आता है। विकलांग व्यक्ति के साथ स्वस्थ व्यक्ति की शादी को हमारे समाज में शक की निगाह से देखा जाता है। लोगों को इसमें कोई साजिश या स्वार्थ नजर आता है। कई बार अपना घर बसाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को पैसे देने पड़ते हैं या किसी-न-किसी तरह का समझौता करना पड़ता है।
मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी ‘कठपुतलियाँ’ का तीस वर्षीय विधुर और एक पैर से विकलांग रामकिसन दो हजार रूपये चुका कर तेरह साल की सुगना से शादी कर लेता है। रामकिसन विकलांग होने के बाद भी आत्मनिर्भर है। वह गाँव-गाँव में घूम-घूम कर कठपुतलियों का नाच दिखाकर पैसे कमाता है। वह अपनी किशोर पत्नी से किसी प्रकार का जोर जबर्दस्ती नहीं करता बल्कि उसे पूरा समय देता है घर परिवार की जिम्मेदारियाँ संभालने का। किसी अन्य पुरुष से गर्भधारण करने के बाद वह उसे भला-बुरा कहता जरूर है पर जल्दी ही इसे भी अपनी ही कमी मान लेता है। जया जादवानी ने ‘जो बचा, वह शब्द नहीं था’ में शादी की समस्या को एक अन्य रूप में रंखांकित किया है। समस्या इतनी जटिल है कि विकलांग व्यक्ति भी सकलांग से ही शादी करना चाहता है अगर विकलांग से शादी करता भी है तो अपनी तरह की विकलांगता ही उसे स्वीकार्य होती है उससे भिन्न विकलांग के प्रति उसमें भी उपेक्षा का ही भाव होता है। समान विकलांगता तो गा्रह्य है पर विकलांगता की भिन्नता के साथ संवेदनाएँ समाप्त हो जाती हैं। सम्पत्ति के उत्तराधिकार का प्रश्न भी विकलांगो के घर बसाने में प्रमुख अड़चन होता है, यही नहीं कई बार सम्पत्ति ही विकलांगो के शोषण के प्रमुख कारणों में एक होता है।
विकलांग स्त्रियों की जिंदगी घर-परिवार में और भी दयनीय हो जाती है। धर्मवीर भारती की कहानी ‘गुलकी बन्नो’, सच्चिदानन्द धूमकेतु की कहानी ‘एक थी शकुन दी’ तथा मैत्रेयी पुष्पा की कहानी ‘सहचर’, (शैलेश मटियानी) हमें विकलांग स्त्रियों के जीवन-संघर्षों से रू-ब-रू कराती है। पति यदि विकलांग हो तो पत्नी उसकी हर प्रकार से सेवा और देखभाल करती है। पत्नी के विकलांग होने पर पति एवं सुसराल वालों का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। ‘सहचर’ के बंशी की तरह बहुत कम ही पति होते हैं जो विकलांगता के बाद भी पत्नी का साथ दे पाते हैं। पति चाहे विकलांग ही क्यों न हो पुरुष होने के श्रेष्ठता के भाव से ग्रसित रहता है और पत्नी पर धौंस जमाना अपना अधिकार समझता है।
मृदुला गर्ग की कहानी ‘जिजीविषा’ का पति भी अपनी बीमारी से इतना कंुठित हो गया है कि दिलोजान से सेवा करने वाली पत्नी की सेवा-भाव के पीछे उसे उसका स्वार्थ ही दिखाई देता है। पत्नी एवं परिवारवालों के द्वारा ठीक करने की कोशिश उसके इस अहसास को और गहरा कर रहा है कि अब वह एक सामान्य इंसान की हैसियत खो चुका है। यह हीनताबोध उसमें अधिक उद्विग्नता, झुँझलापन और चिड़चिड़ाहट पैदा कर रही है।
धर्मवीर भारती की ‘गुलकी बन्नो’ और सच्चिदानन्द धूमकेतु की ‘एक थी शकुन दी’कहानियाँ विकलांगता से ग्रस्त स्त्रियों की जीवटता को उद्घाटित करती है। शकुन दी एक ऐसी संघर्षरत महिला के रूप में हमारे सामने आती है। पुरुषसत्ता ने स्त्री को संपत्ति का हक नहीं दिया है। अतः स्त्री यदि विकलांग है तो उसकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। विकलांग स्त्री यदि बेसहारा हो तो सिवाय भिक्षावृत्ति का उसके समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। ऐसी बेसहारा विकलांग स्त्रियों का हर जगह शोषण होता है। विकलांग व्यक्तियों में भी अन्य विकलांग के प्रति सदाशयता का प्रायः अभाव देखा जाता है। शिव प्रसाद सिंह की कहानी ‘कर्मनाशा की हार’ में भैरो पाण्डे की चेतना एक अंधी लड़की और एक अपाहिज बुढ़िया को बाढ़ की भेंट चढ़ाने पर सुुषुप्त ही रहती है लेकिन फुलमतिया और उसकी अवैध संतान को नदी में फेंके जाने के गाँव वालों के निर्णय का पुरजोर विरोध उनकी मानवीयता है या अपने वंश-बेल को बचाने की कोशिश?
नेत्रहीन तथा मानसिक रूप से विकलांग स्त्रियों के यौन शोषण के उदाहरण अनेक कहानियों में मिल जायेंगें। असामाजिक तत्व ऐसी स्त्रियों की विकलांगता का लाभ उठाने से बाज नहीं आते। अमरकांत की कहानी ‘जिंदगी और जोंक’ में हम देखते हैं कि किस तरह भात खिलाने का लालच देकर रजुआ एक मानसिक विकलांग स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है।
विकलांग बच्चों के संबंध में सोचते-विचारते, बात करते समय जो एक अहम प्रश्न उभरकर आता है, वह यह कि क्या विकलांग बच्चों को जन्म लेने का अधिकार है या उनकी भ्रूण हत्या कर देनी चाहिए। तेजेन्द्र शर्मा एवं उपासना ने क्रमशः ‘मुझे मार डाल बेटा…!’ तथा ‘मुक्ति’ कहानियों में विकलांग शिशु भ्रूण हत्या के औचित्य के प्रश्न को उठाया है। जो अभिभावक के लिए मुक्ति है क्या वाकई उन शिशुओं के लिए भी मुक्ति ही है?
विकलांगों के सामाजिक एकीकरण के लिए उनके प्रति सामाजिक जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ विकलांगों के लिए मनोचिकित्सकीय परामर्श की भी आवश्यकता होती है। विकलांगता एक ओर व्यक्ति में कुंठा भर देता है तो दूसरी ओर उसे अभिमानी भी बना देता है। एक बेहतर सामाजिक वातावरण के लिए दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। अतः एक मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती है जो विकलांग व्यक्ति और उसके करीबी लोगों को सही परामर्श दे सकें। भारत जैसे देश में गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव भिक्षावृत्ति और पागलपन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गरीब व्यक्ति रोजगार के अभाव में न चाहते हुए भी कई बार भिक्षावृत्ति अपना लेता है। कभी-कभी किसी सदमा, दुःख या जीवन की विपरीत परिस्थितियों के कारण उपजे तनाव से अच्छा खासा इंशान भी पागल बन जाता है -हंसा जाइ अकेला के हंसा और जहरकाँटा के ‘रामा’ की तरह। इन दोनों के पागलपन का जिम्मेदार कौन -हमारा समाज, प्रशासन या पूरा तंत्र?
विकलांगता के बावजूद कुंठित न होकर उसकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उसे अपने व्यक्तित्व पर हावी न होने देने की प्रवृत्ति कम मनुष्यों में मिलती है। अज्ञेय ने ऐसे ही जिंदादिल चरित्र ‘खितीन बाबू’ के रूप में प्रस्तुत किया है। खितीन बाबू तमाम शारीरिक परेशानियों के बीच हमेशा खुशमिजाज रहते हैं। खितीन बाबू का चरित्र इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि यदि व्यक्ति अपने साथ होने वाली दुर्घटनाओं को नियति मान ले और जीवन जैसा भी है उसे खुशी से स्वीकार कर ले तो जीवन न तो कभी बोझ लगेगा और न ही कुंठा के भाव मन में आयेंगे। कंुठित व्यक्ति न तो खुद आत्म-सम्मान और खुशी के साथ जी पाता है न किसी और के सम्मान और खुशी का ख्याल रख पाता है। कई बार शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति अपनी ओर सबका ध्यान ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करना चाहता है और इसके लिए तरह-तरह से परिवार वालों को परेशान करता है।
धार्मिक अंध-विश्वास के कारण भारतीय समाज में विकलांगों को तरह-तरह का भेदभाव झेलना पड़ता है। समाज में विकलांगों के लिए लांछना का भाव होता है। लोगों की आम धारणा होती है कि सुबह-सुबह विकलांगों को देखने से पूरा दिन व्यर्थ हो जाता है या हानि उठानी पड़ती है। कोई गर्भवती महिला उसे देख ले तो बच्चे के विकलांग होने की संभावना बन जाती है। इस तरह की कूपमंडूकता के कारण विकलांगों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है।
विकलांगता के कारण अनेक आर्थिक समस्याएँ झेलनी पड़ती है। जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति किसी बीमारी या दुर्घटना या फिर किसी अन्य कारणों से विकलांग हो जाता है तो उसका प्रभाव उसकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। विकलांग या बीमार व्यक्ति के इलाज-दवाओं पर परिवार के अर्थ का एक बड़ा हिस्सा व्यय हो जाता है जिससे आर्थिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। आर्थिक सम्पन्नता के बावजूद भी सांस्कृतिक अंधविश्वास के चलते कई परिवारों में विकलांगों की स्थिति दयनीय हो जाती है। यह स्थिति मरीज की जिजीविषा तो खत्म करती ही है परिवार का माहौल भी खराब हो जाता है और सुख शांति गायब हो जाती है। सरकारी अस्पतालों की जर्जर व्यवस्था भी अनेक व्यक्तियों की असमय मृत्यु और विकलांगता का कारण बन जाती है। ‘खुदा की देन’ की नज्जो इसका प्रमाण है।
उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकलांग व्यक्तियों और उसके परिवारजनों के संघर्ष और समस्याओं को कहानी का कथ्य बनाने की प्रवृत्ति स्वातंत्र्ायोत्तर कहानीकारों में, उसमें भी समकालीन कहानीकारों में अधिक है। इसे वैश्विक स्त्तर पर विकलांगता आंदोलन और विकलांगता अध्ययन का प्रभाव भी माना जा सकता है। कहानीकारों ने इन कहानियों के माध्यम से कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं जैसे- गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता और इलाज के अभाव के कारण विकलांगता का होना। विकलांगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर होने वाले प्रयासों की न्यूनता तथा जो योजनायें चलाई जा रही हैं विकलांगों को उनकी जानकारी न होना, उससे लाभान्वित न होने की ओर रचनाकारों ने ध्यानाकृष्ट किया है। सवाल उठता है कि हमारे तंत्र में क्या खामियाँ हैं जिनसे उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती, क्या इसके व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की आवश्यकता नहीं? सरकार के द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं का तो व्यापक प्रचार-प्रसार होता है पर विकलांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विज्ञापन कम ही होता है। क्या इसके पीछे वोट-बैंक की राजनीति तो नहीं? चूँकि समाज में विकलांगों का कोई वोट-बैंक नहीं होता इसलिए उनके प्रति सबकी उदासीनता होती है।
इन कहानियों में विकलांगों एवं उनके परिवार वालों की समस्याओं का तो चित्रण है पर उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का कहीं भी जिक्र नहीं है। विकलांगता के पश्चात् भिक्षावृत्ति को अपनाने की बात है पर उनके सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर कम ही लिखा गया है। विकलांग व्यक्ति कृत्रिम अंगों की सहायता से भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। इस संकलन में ऐसी कहानियों को भी लिया गया है जिसमें विकलांगों के लिए कोई प्रेरणाप्रद या सम्मानजनक बातें नहीं हैं जिन्हें पढ़कर पाठक्-मन निराश और विक्षोभ से भर जाता है। प्रश्न है कि ऐसी कहानियों के नीछे रचनाकार का क्या उद्देश्य है? साहित्यकार हमें समाज से रू-ब-रू करवाता है। समाज का सफेद पक्ष से भी और स्याह पक्ष से भी। हमारे समक्ष समाज की नग्न वास्तविकता को भी उपस्थित करता है। इस तरह से विभिनन सामाजिक रूपों को समझने में मदद मिलती है। समस्या से नजरें चुराकर नहीं बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप को समझकर, मूल कारणों को ढ़ूँढ़ कर ही उसका सही समाधान किया जा सकता है।
रचनाकार समाज का संवेदनशील प्राणी होता है। हिन्दी साहित्य में दलित, स्त्री और पीछड़े वर्गों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर जिस तरह की कहानियाँ लिखी गई हंै, विकलांगों से संबंधित ऐसी कहानियों का अभाव है। इन कहानियों में समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं पर सशक्तिकरण की कोई राह नहीं, बावजूद पाठक में संवेदना जरूर जागृत करती हैं, ये कहानियाँ। उन्हें विकलांगों के ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों के जीवन की समस्याओं से भी रू-ब-रू करवाती हैं। समाज के संवेदनशील होने पर ही विकलांग और उसके घर वाले कुंठा से मुक्त हो सकते हैं। ये कहानियाँ ये बताती है कि विकलांगों के प्रशिक्षण की, चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है जिससे वे समाज के तथाकथित सकलांग लोगों की मदद से आहत या कंुठित न हो बल्कि उसे सहज रूप में लें। मिलने वाली विशेष सुविधाओं को उपकार, दया या भीख न मानकर उसे अपना अधिकार समझें।
इन कहानियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि विकलांगता के पश्चात् जीवन के सारे आयाम बन्द हो जाते हैं। शिक्षा और रोजगार की कोई आवश्यकता नहीं होती। विकलांग ऊब, संत्रास और कंुठा में डूबकर अन्ततः मृत्यु को गले लगा लेता है। क्या यही हमारे समाज में विकलांगों की वास्तविक स्थिति है? आज हमारे समाज में अनेक विकलांग शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से समाज के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहें हैं। हिन्दी साहित्यकार विकलांगों की इन उपलब्धियों से इतना अनजान क्यों हैं? इन कहानियों में ऐसे पात्रों की न्यूनता क्यों हैं यह एक विचारणीय पहलू है। स्त्री सशक्तिकरण, दलित आंदोलन की तुलना में विकलांगता अधिकार आंदोलन की शुरूआत वैश्विक स्तर पर तथा भारत में भी काफी बाद में होना, कहीं इसका कारण तो नहीं।