दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत हंसराज महाविद्यालय की एक अलग ही प्रतिष्ठा है। इस हंसराज महाविद्यालय की वर्तमान प्राचार्या हैं डॉ. रमा। एक निम्न मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मीं डॉ. रमा ने कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ मीडिया आदि क्षेत्रों में काम करते हुए आज यह मुकाम हासिल किया है। मीडिया पर कई पुस्तकों का लेखन व संपादन भी कर चुकी हैं। विद्यार्थियों से लेकर साहित्य जगत के लोगों में उनकी बड़ी लोकप्रियता है। साक्षात्कार श्रृंखला की दसवीं कड़ी में पुरवाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी अनुराग सिंह और युवा लेखक पीयूष द्विवेदी ने डॉ. रमा से उनके निजी जीवन तथा हिंदी भाषा-साहित्य की दशा-दिशा को लेकर बातचीत की है।
सवाल – मैम सबसे पहले परिचय स्वरूप अपने जीवन यात्रा के बारे में कुछ बातें हमारे पाठकों से साझा कीजिए ताकि वो आपसे अच्छे से रू-ब-रू हो सकें।
रमा जी – मैं एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ और मेरे अपने परिवार में साहित्य की दुनिया में कोई नहीं गया। पिता जी मिलिट्री में थे, हम पांच भाई-बहन और बेहद सामान्य सा जीवन। मेरी माता जी लोगों के घरों में काम कर के, कपड़ों की सिलाई कर के अपने स्तर से सहयोग दे रही थीं और हम आगे बढ़े। संयोग कहिये या माता-पिता का आशीर्वाद कहिए, मैं उच्च शिक्षा की ओर आ गयी और उच्च शिक्षा में भी मैंने साहित्य को चुना।
साहित्य को चुनने का भी कारण था, एक तो शुरू से ही मैं बहुत संवेदनशील थी, दूसरा साहित्य से इतर विज्ञान और इंजीनियरिंग की पुस्तकें बहुत मंहगी थीं और हमारे परिवार में इतना सामर्थ्य ही नहीं था। उस समय सोशल मीडिया था नहीं, मोबाइल होते नहीं थे। इस तरह मैं इस क्षेत्र में आ गयी और दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.ए.(आनर्स) में दाखिला लिया। इससे पहले बतौर वक्ता मैं आर्य समाज के कार्यक्रमों में बचपन से जाती रही थी।
मैंने मंच से सबसे पहली बार गायत्री मंत्र का ही उच्चारण किया था और वह पिता जी का सबसे अच्छा निर्णय था कि जब भी आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाएँ तो मुझे हमेशा ले कर जाएँ। वहां उन लोगों ने मुझे गायत्री मंत्र बोलने के लिए प्रोत्साहित किया और धीरे-धीरे मैं आर्य समाज की एक प्रतिष्ठित वक्ता बन गयी। यह प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद भी जारी रही। लोग बताने लगे कि मैं यहाँ भी एक प्रतिष्ठित वक्ता बन गयी और मेरे लिए यह आर्थिक सहयोग का जरिया भी बना।
मैंने पांचवीं कक्षा के बाद ही नर्सरी के बच्चे का ट्यूशन लगा लिया। वहां से कमाई का एक जरिया मिल गया। यहाँ डिबेट्स में तो भाग लेने लगी, भाग्य की बात थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे दाखिला मिला था। तब यहाँ बहुत अच्छी डिबेट्स होती थीं और हमारी पॉकेट मनी अच्छे से निकल जाती थी। पढ़ाई का खर्चा वजीफा से निकला जाता था, कॉलेज ने बहुत सुविधा दी, फीस माफ़ कर दी। डिबेट, क्रिएटिव राइटिंग, कविता प्रतियोगिता, साहित्य से जुड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मेरे पास 850 से ज्यादा पुरस्कारों के प्रमाण-पत्र हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी जी ने मुझे ‘चैम्पियन ऑफ़ चैम्पियंस’ का पुरस्कार दिया। इस तरह रास्ते खुलते चले गए।
यहीं से बी.ए व एम.ए. करने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान से मीडिया में एक वर्ष का डिप्लोमा किया जो मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वहां से टेलीविजन, दूरदर्शन, रेडियो व समाचार पत्रों के साथ जुड़कर काम किया। उन दिनों रेडियो पर सुबह 3 बजे की मेरी शिफ्ट होती थी, मैंने सुबह से लेकर रात तक खुद को व्यस्त कर लिया, काम और अपनी पढ़ाई आदि में। फिर एक पहचान मिलनी शुरू हो गयी। साथ में ठीक-ठीक कमाई भी होने लगी। लेकिन एक सामान्य परिवार की सोच थी कि अभी तक ठीक है, लेकिन शादी के बाद कैसे चलेगा? डिप्लोमा के बाद मेरे साथ के लोग परमानेंट नौकरी में चले गए लेकिन मुझे मीडिया का वह माहौल बहुत रास नहीं आया क्योंकि मैं एक सामान्य निम्न मध्य वर्ग से थी और वहाँ का माहौल थोड़ा एडवांस होता है। इधर मैंने अपनी अकादमिक पढ़ाई जारी रखी। एम.फिल. व पीएच.डी. मैंने यहीं से की।
एम.फिल.करते ही मुझे हंसराज कॉलेज में 1991 में अस्थाई नौकरी मिल गयी। इससे घर वाले भी खुश थे क्योंकि यह नौकरी ठीक थी, उन्हें लगता था कि इससे घर भी संभल सकता है और नौकरी भी। हालांकि उस समय तक मेरे पास नौकरियों की कमी नहीं थी। जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे मीडिया का ही पेपर पढ़ाने को मिला। धीरे-धीरे विद्यार्थियों के मध्य मेरी अच्छी पहचान बनी। फिर मुझे भी लगने लगा कि इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। अब तो 2015 से यहाँ की प्राचार्या भी हूँ, आप लोग के सहयोग से शैक्षणिक और प्रशासनिक दुनिया का सामंजस्य बना हुआ है।
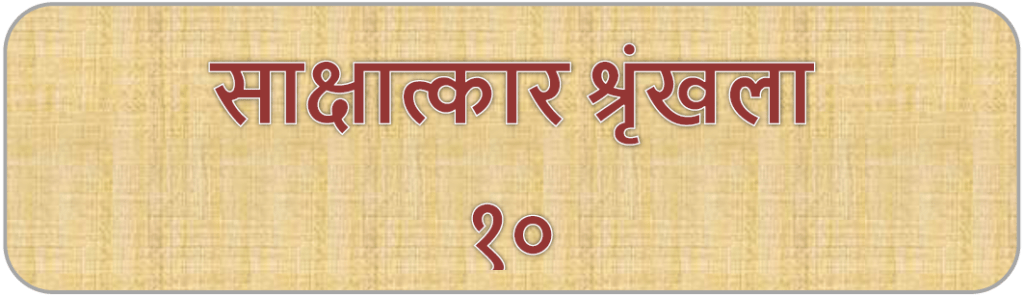
सवाल – क्या दक्षिण भारत की ओर से लगातार हिन्दी को लेकर भाषाई राजनीति नहीं हो रही है? हिन्दी के इस राजनीतिकरण को आप कैसे देखती हैं?
रमा जी – मैं पिछले दिनों खुद वहां गयी थी और मुझे लगा कि लोगों में हिन्दी को लेकर विरोध नहीं है। राजनेता लोग विरोध पैदा करते हैं और मुझे लगता है कि भाषा का विरोध पैदा करना एक बहुत बड़ा हथियार है। अंग्रेजों ने भी तो यहाँ की भाषाओँ पर कब्जा ही किया। हम अंग्रेजों से मुक्त हुए लेकिन हमारी मानसिकता अंग्रेजी ही हैं न! दक्षिण भारत के लोग अच्छी हिन्दी बोलते हैं। मैंने उनसे बात भी की, मैंने पूछा कि आप लोग इतनी अच्छी हिन्दी बोलते हैं तो विरोध क्यों करते हैं हिन्दी का? उन्होंने कहा कि हम हिन्दी का विरोध नहीं करते हैं, हम यह चाहते हैं कि जैसे हम लोग हिन्दी बोलें और सीखें तो अन्य लोग भी दक्षिण भारत की कोई एक भाषा सीख लें।
हमारे बच्चों को यदि हिन्दी सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो बाक़ी भारत के सभी स्कूलों में हमारी भाषा सीखने के लिए मजबूर किया जाए। यह बात तो खराब नहीं है। इसलिए राजनेताओं ने इसे अपनी राजनीति से जोड़ लिया है। दिक्कत है कि हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अब हिन्दी की स्थिति सुधरी है, उच्च पदों पर बैठे हमारे माननीय हिन्दी बोल रहे हैं, लेकिन आज भी हिन्दी बोलना कहां बहुत अच्छा माना जा रहा है। आम जन को तो मतलब विचार विनिमय से है। मैं एक तमिल परिवार को जानती हूँ, उनका दिल्ली में व्यापार है, वो कहते हैं कि बिना हिन्दी के हमारा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन आप जबर्दस्ती नहीं करा सकते ना। हमें भाषा का विरोध नहीं करना करना चाहिए, हिन्दी के प्रति एक माहौल बनाना चाहिए। हमें सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना होगा।
सवाल – क्या हिन्दी भाषा की वजह से इसकी बोलियों को सच में खतरा है या यह केवल मनगढ़ंत बातें भर हैं?
रमा जी – नहीं मुझे नही लगता। सिंधी व भोजपुरी को लेकर पीछे बातें उठीं। हिन्दी को लेकर कहा जाता है कि यह तो बड़ी समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। कोई भी भाषा समृद्ध कैसे होती है जब उसमें अनेक बोलियां होती हैं। हर बोली का अपना एक सौन्दर्य है। वह सौन्दर्य वहां से फिर भाषा में निकल कर आता है। कोई भी बोली राष्ट्र भाषा नहीं बन जायेगी, राजभाषा नहीं न बन जायेगी।
हमें बोलियों और हिन्दी भाषा को एकदूसरे के विरोध में नहीं खड़ा करना है। अंग्रेजी वालों ने कभी नही कहा कि अंग्रेजी सीखो लेकिन उन्होंने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि लोग आज सीख रहे हैं। अगर कोई भोजपुरी का व्यक्ति यह कहे कि उसके बच्चे को भोजपुरी आनी चाहिए तो यह अच्छी बात है। जहाँ कुछ सुविधाएं भोजपुरी को मिलनी चाहिए वह बिल्कुल मिलें। मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध इसमें होना चाहिए।
सवाल – ठीक इसी के उलट यह भी बात कही जाती है कि हिन्दी की विभिन्न सहायक बोलियों को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से हिन्दी भाषा को खतरा है। आपका इस पर क्या मत है?
रमा जी – नहीं मुझे नहीं लगता कि हिन्दी को कोई ख़तरा है। क्या अभी तक जो बोलियाँ शामिल हैं उनकी वजह से हिन्दी को कोई ख़तरा हुआ? यह केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। ये बोलियाँ भी तो हिन्दी भाषा की थाती हैं। हमें इससे नहीं घबराना चाहिए।

सवाल – सरकारी या आधिकारिक तौर पर हम जिस हिन्दी का प्रयोग करते हैं, वह अधिक बनावटी क्यों लगती है?एक सामान्य हिन्दी बोलने वाला उसमें थोड़ा असहज नहीं महसूस करता?
रमा जी – कई बार हम अपनी विद्वता दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं। अगर एक अध्यापक के तौर पर मैं लगातार एक घंटे विद्वता पूर्ण भाषण दे कर आ जाऊं और बच्चों को कुछ न समझ आये तो क्या लाभ? बच्चे उस समय तो प्रभावित हो जायेंगे लेकिन बाद में उन्हें यह पता चलेगा कि कुछ नहीं समझ आया। विद्वता नहीं दिखानी है, बस बात समझ आनी चाहिए। भाषा सहज होनी चाहिए, लेकिन सहज और सरल बनाने के चक्कर में अशुद्ध भाषा का भी प्रयोग नहीं करना है। भाषा का मूल व्याकरण जो है उससे नहीं हटना है। भाषा की गरिमा उसी से है। हिन्दी की सहजता को शुद्धतावादी दृष्टिकोण के कारण समाप्त न करें। वर्तनी व उच्चारण की शुद्धता तक ठीक है, व्याकरण शुद्ध हो इतना ठीक है। हमें लोगों में रुचि पैदा करनी है, रुचि को मारना नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि आपकी विद्वत्ता के कारण घबड़ाकर लोग फिर हिन्दी पढ़ना ही न चाहें।
सवाल – हिन्दी पट्टी के लोगों में हिन्दी को लेकर एक अगाम्भीर्य क्यों दिखाई पड़ता है? उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में लाख बच्चे तो केवल हिन्दी भाषा में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों उपजी हैं?
रमा जी – मुझे लगता है कि ये चिंता सिर्फ भाषा को लेकर ही नहीं होनी चाहिए। आजकल हर चीज को लेकर हमारी ‘चलता है’ की एक सोच बन गयी है। हम नौकरी करते हैं, तो उसमें भी यही मानते हैं कि सब चलता है। यह अनुशासन की कमी की बात है। इसी प्रकार जब हम भाषा की बात करते हैं, तो मेरी, तेजेंद्र जी आदि लोगों की जो पीढ़ी है, उसने भाषा पर बहुत मेहनत की है। मेहनत की बात जब मैं करती हूँ, तो बताना चाहूंगी कि उस समय तख्ती होती थी, उसपर हम लोग कलम-स्याही से लिखा करते थे। व्याकरण के अनुसार तब हमें लिखना सिखाया जाता था। आज की पीढ़ी में ऐसे लिखने की आदत खत्म हो गयी है। मोबाइल फोन, फोटोस्टेट जैसी सुविधाएं ये आदत खत्म होने में बड़ा कारण रही हैं।
जिस तरह हम लिखा करते थे, उससे लिखने का हमारा अभ्यास होता था। लिखते-लिखते कई शब्द हम पढ़ा भी करते थे। इसमें मेहनत लगती थी, लेकिन अब आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। नोट्स ‘पीढ़ी दर पीढ़ी’ फोटोस्टेट होते जाते हैं। सब रेडीमेड सामग्री होती है, जिसे आपने पढ़ा भी नहीं होता और बस परीक्षाओं में ही पढ़ते हैं। ऐसे में परीक्षा में जब लिखना पड़ता है, तो कमजोरी सामने आने लगती है।
आपकी नियमित पढ़ाई में तो ये तरीका कभी चल भी जाए, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं चल सकता। नेट परीक्षाओं की परीक्षक के तौर पर कई बार मैंने काम किया है, तो वहाँ हिंदी के बहुत-से प्रतिभागी विद्यार्थियों की स्थिति देखकर बहुत कष्ट होता है। गैर-हिंदीभाषी यदि गलतियाँ करते हैं, तो उसे हम एकबार के लिए नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हिंदीभाषी छात्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं में जब हम गलतियाँ दिखती हैं, तो आश्चर्य होता है।
मुझे लगता है कि अब हमें जागना होगा, गंभीरता दिखानी होगी। खासकर हिंदी प्रदेश के लोग अगर इस विषय में गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो ये चिंताजनक है। लेकिन एक पक्ष यह भी है कि ऐसा आज नहीं हो रहा, हमेशा से ही रहा है। हिंदी को किसने बढ़ाया? गैर-हिंदीभाषी लोगों ने बढ़ाया है और उन लोगों ने बढ़ाया जिनकी अपनी दूसरी भाषाएँ बहुत बेहतर होती थीं। तो पहले भी हिंदी के बढ़ने के रास्ते निकले हैं, आगे भी निकलेंगे।
सवाल – अकादमिक स्तर पर भी हिन्दी विषय के साथ उच्च शिक्षा के बाद बच्चों में भाषा एवं वर्तनी संबंधी बड़ी अशुद्धियाँ पायी जाती हैं। इसके पीछे आपको क्या वजहें जिम्मेदार लगती हैं?क्या अध्यापक बच्चों में हिन्दी भाषा के प्रति रुचि नहीं पैदा कर पा रहे हैं?
रमा जी – इसके लिए प्राध्यापकों को भी सरासर दोषी नहीं माना जा सकता और विद्यार्थियों को भी नहीं। हमारी जो व्यवस्था है, वो तेजी से बदल रही है। पहले प्राध्यापक पढ़ने-पढ़ाने, लिखने-लिखवाने का काम ज्यादा करते थे, अब जिस प्राध्यापक की कक्षा में साठ-सत्तर विद्यार्थी होंगे, सेमेस्टर सिस्टम है, वो क्या करेगा? पहले मान लीजिये कि वार्षिक परीक्षा है और इस दौरान एक अध्यापक को चार उपन्यास पढ़ाने हैं, तो वो बहुत अच्छे-से पढ़ाता था, विद्यार्थियों से उसपर बातचीत करता था, प्रश्न लिखवाता था और विद्यार्थी लिखते थे।
अब तो सब बस भाग रहे हैं। प्राध्यापक भी भाग रहे हैं और विद्यार्थी भी। प्राध्यापकों की भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव भी एक कारण है। पंजाब, राजस्थान, बिहार जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से होने के कारण प्राध्यापकों के हिंदी बोलने मेंअंतर आ सकता है, लेकिन लिखने में जो वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं, उन्हें सहन नहीं किया जा सकता। इसके लिए अभ्यास ही उपाय है। प्राध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों को अभ्यास करना होगा। भाषा के प्रति हमें रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी।
सवाल – हिन्दी को लेकर आज सामान्य अवधारणा यह बन गई है कि यह विषय पढ़कर क्या करोगे? कुछ ऐसा पढ़ो जिसमें रोजगार हो। हिन्दी और रोजगार के अवसर पर आपका क्या मत है?
रमा जी – हिंदी में रोजगार की कोई कमी नहीं है, बल्कि रोजगार ज्यादा हैं और काम करने वाले अच्छे लोग कम हैं। मैं खुद हिंदी से रही हूँ, लेकिन हिंदी से होने के बावजूद मैंने मीडिया में काम किया, दो साल तक बैंक में नौकरी की, स्कूल में नौकरी की। मीडिया में तो रेडियो, टेलीविजन, समाचार-पत्र में बहुत लोग चाहिए, लेकिन हिंदी में ठीक काम करने वाले उतने लोग नहीं मिल रहे। मतलब कि रोजगार की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन रोजगार के लिए जहां भी आप जा रहे हैं, वहाँ काम चाहिए। अब जब आप वर्तनी की गलतियाँ करेंगे, पीएचडी होते हुए भी भाषा पर पकड़ नहीं होगी, आप एक न्यूज नहीं तैयार कर सकेंगे, सही-सही दस पंक्तियाँ नहीं लिख पाएंगे, तो आपको रोजगार कौन देगा? इसलिए मैं नहीं मानती कि हिंदी में रोजगार नहीं हैं। रोजगार हैं, लेकिन रोजगार लेने वालों को अपने आप को उसके लायक बनाना होगा।
सवाल – आज विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रमों में लोकप्रिय साहित्य को स्थान क्यों नहीं मिल पा रहा है?हिन्दी में प्रेमचंद लोकप्रिय भी रहे और अकादमिक स्थान भी मिला। धीरे-धीरे ऐसी प्रवृत्ति लगभग मृतप्राय हो गई और आज तो साफ तौर पर दो अलग साहित्य की दुनिया देखी जा सकती है। यह संतुलन क्यों नहीं बन पाया जो प्रेमचंद जैसे लोगों ने हिन्दी साहित्य को लेकर किया?
रमा जी – प्रेमचंद के समय में भी बहुत संघर्ष था। ये तो आज हमें लगता है कि प्रेमचंद, प्रसाद कितने लोकप्रिय हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस समय में संघर्ष नहीं था। क्या आज तेजेंद्र शर्मा जी की कहानियाँ नहीं पढ़ीं जातीं? खूब पढ़ी जाती हैं। क्या आज उनकी कहानियाँ पाठ्यक्रमों में नहीं हैं? खूब हैं। कहने का मतलब है कि आज भी लेखक पढ़े जा रहे हैं। लेकिन लोकप्रिय साहित्य में हमें हमेशा एक गंभीरता को बनाए रखना चाहिए।
दो तरह का साहित्य होता है। एक होता है कि लेखक बस लिखता है। वो उसमें अपनी संवेदनाएं, अपने अनुभव डाल देता है। दूसरी स्थिति में लेखक बाजार को सामने रखकर लिखता है, बेचने के लिए लिखता है। आज के समय में बाजारवाद सब पर हावी हो गया है, साहित्य पर भी। लेकिन वास्तव में लेखक को यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं लिख रहा हूँ तो पाठक उसको पढ़ेगा कि नहीं, उसको बस ये चिंता होनी चाहिए कि मैं अच्छा लिखूं और लिखता चला जाऊं और अगर मैं अच्छा लिखूंगा तो पाठकवर्ग अपने आप तैयार होगा।
आज भी ‘गोदान’ पाठ्यक्रमों में है न! जयशंकर प्रसाद की ध्रुवस्वामिनी, चन्द्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसी रचनाएं, जिनको हम बहुत मुश्किल मानते हैं, आज भी पाठ्यक्रमों में हैं न! अच्छा लेखन हमेशा रहता ही है। संघर्ष भी हमेशा रहा है, लेकिन उस संघर्ष में भी भाषा की गरिमा और स्तर के साथ कोई समझौता न करते हुए लेखक को पूरी गंभीरता के साथ लिखना चाहिए।
लेखक को दुरूह भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस समाज में वो रह रहा है, उसे केवल उसी समाज की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि उससे आगे भी देखना चाहिए। लेखक वही है, जो अपने समय-समाज से आगे की सोचता है। जो लेखक अपने आप को सीमाओं में नहीं बांधता, किसी ख़ास विचारधारा में नहीं बांधता और मुक्त होकर काम करता है, असल में वही लोकप्रिय होता है और वही अकादमिक जगत में प्रवेश करता है।
सवाल – विश्वविद्यालयों में हिन्दी ही नहीं अनेक मानविकी शाखा के विषयों पर लाल रंग या वाम विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा क्यों हुआ और ऐसे में क्या हम एक विद्यार्थी को वृहद कैनवास दे पाएंगे कि वह अपने मस्तिष्क का विस्तार कर पाये?अगर नहीं तो इसका क्या विकल्प है?
रमा जी – ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन लगभग सभी जगह है। इसका कारण ये है कि विश्वविद्यालय अब राजनीति के गढ़ बनते जा रहे हैं। एक विचारधारा को लगता है कि मेरे ही लोगों को पढ़ा जाना चाहिए। जबकि साहित्य को किसी विचारधारा में बांधना नहीं चाहिए और विद्यार्थियों को एक खुला मैदान देना चाहिए ताकि उसकी अपनी समझ विकसित हो और फिर वो जिस विचारधारा की तरफ मुड़ना चाहे, मुड़े। इसलिए हमें खुली दृष्टि को लाना पड़ेगा। पहले जब विश्वविद्यालयों में राजनीति नहीं होती थी, तो उनका स्तर अच्छा था। हमारे पाठ्यक्रम अच्छे बनते थे। विद्यार्थी अच्छे निकलते थे, उनकी समझ अलग तरह की बनती थी, लेकिन अब ये स्थिति होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
सवाल – साहित्यिक विमर्शों ने साहित्य का अंततः नुकसान किया है या उसे फायदा पहुंचाया है?
रमा जी – मैं ये नहीं मानती कि नुकसान किया है। मैं बहुत सकारात्मक सोच रखती हूँ। कम से कम विमर्श के बहाने ही सही, लोग पढ़ते तो हैं। चाहें दलित विमर्श हो, स्त्री-विमर्श हो या बाहर जाकर बेहतर लिख रहे और हिंदी के लिए काम कर रहे लोगों पर केन्द्रित प्रवासी विमर्श की ही बात हो, ऐसे विमर्शों से कोई नुकसान नहीं हुआ। हमें सब चीजें खुली छोड़नी चाहिए। विमर्श आ रहे हैं, आएं। किसी विमर्श का साहित्य सामने आ रहा है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जरूरत इतनी ही है कि हमारी सोच सकारात्मक और काम ठोस हो। हमें काम से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर हम सबको एक सकारात्मक सोच के साथ हिंदी साहित्य का विकास करना है।
अनुराग – अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रमा जी – अरे धन्यवाद की क्या बात है, मुझे लगता है कि जबतक आप जैसे विद्यार्थी हैं, पाठक हैं, पुरवाई जैसी पत्रिकाएँ हैं, तेजेंद्र शर्मा जी जैसे अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य को देने का बीड़ा उठाए लेखक हैं, तबतक हिंदी का भविष्य सुरक्षित है। धन्यवाद।



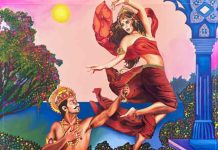
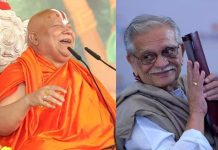
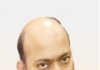


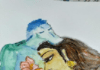
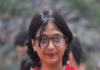

बेहतरीन संवाद !
बिल्कुल सच्ची बात कही मैम ने
काम खूब है ! पर काम आना भी तो चाहिए !
हिंदी के प्रति आशा जगाता सार्थक संवाद बधाई
बधाई
एक सार्थक और सच्चा संवाद बधाई